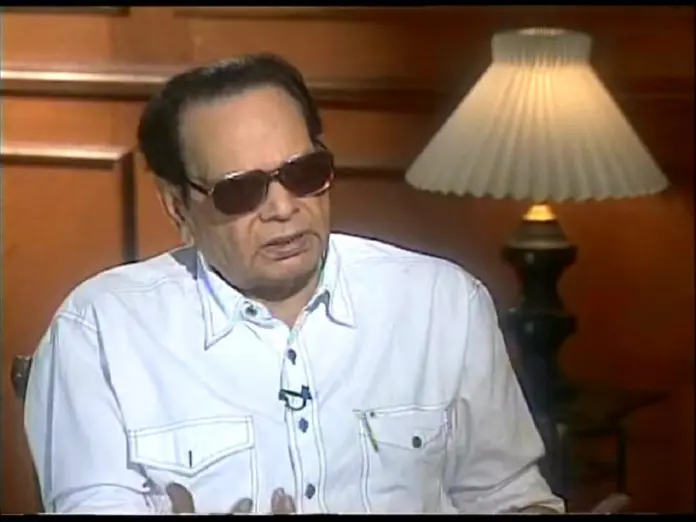कविता – हंस के महिला-लेखन विशेषांक, बहसें, बातचीत और कहानियाँ कहती हैं कि इस आन्दोलन में आपकी एक सक्रिय भूमिका रही, इस तरह के आयोजनों और विशेषांकों का भूमिकाओं की स्त्री-चेतना के सन्दर्भ में विशेष महत्त्व है। क्या इनके द्वारा किसी स्त्री के जीवन की दिशा को भी बदला जा सका है?
राजेन्द्र यादव- हिन्दी के गुरुकुली-साहित्य में आधी दुनिया को लेकर एक खास तरह की चुप्पी, उदासीनता और वर्जित तरह की मानसिकता न तो मुझे लोकतान्त्रिक लगती है, न मानवीय। स्त्री की स्थिति, नियति और संघर्ष की बात करना आज इतना अनैतिक और लगभग अश्लील माना जाता है कि उसके लिए सम्पादक के चरित्र को भी खींच लिया जाता है। यह पुरुष अहंकार और दम्भ है, जहाँ हंस के एक अंक में पच्चीस रचनाकारों के बीच दो स्त्रियों के नाम भी आ गये कि हाय-तौबा मचने लगती है। इस आडम्बरी समाज में जो हर जगह और हर कहीं नारी से आक्रान्त है, लेखन को लेकर तथाकथित शुद्धतावादी विचार जुगुप्सा पैदा करता है, ऐसा लगता है जैसे मैं स्त्री की नहीं, किसी बहुत घिनौनी लत की बात कर रहा हूँ, स्त्री विशेषांकों और हंस में स्त्री समस्याओं को केन्द्र में लाने के पीछे उसे अपने समाज में बराबरी की हिस्सेदारी देने का लोकतान्त्रिक प्रयास था। 33 प्रतिशत हक तो अब सरकार भी मानने लगी है, हंस को तो मैं 5 प्रतिशत या 10 प्रतिशत भी नहीं दे पाता हूँ। मैं उन लोगों की मानसिकता को क्या कहूँ जो स्त्री के किसी भी संघर्ष और अभिव्यक्ति को सेक्स के साथ जोड़ देते हैं। हालाँकि सेक्स भी उसकी मुक्ति का एक हिस्सा है।
जो कुछ भी हंस स्त्री के विषय में दे रहा है, वह निश्चय ही स्त्री चेतना को जाग्रत करने वाला है ताकि वे समाज की अधिक सार्थक और स्वतन्त्र इकाई के रूप में अपने आप को पहचान सकें।
क. – हंस को पढ़ने वाली स्त्रियों का प्रतिशत हमारे समाज में मुश्किल से दो से ज़्यादा भी नहीं होगा, और ये वही स्त्रियाँ हैं जो पढ़ी-लिखी हैं, चेतना सम्पन्न हैं,जागरूक हैं। अपढ़ या कम पढ़ी-लिखी स्त्रियों तक न हंस पहुँच सकता है, न उनकी समझ-सीमा में आता है, फिर स्त्री की जागरूकता में हंस कैसे मददगार है या होगा?
रा. या. – सही है कि हंस को पढ़ना, पढ़ सकना सारी स्त्रियों के लिए सम्भव नहीं, पर जो पढ़ और सोच सकती हैं उनके भीतर तो यह बोध जगाना ज़रूरी है कि वे आसपास की महिलाओं को उनकी भाषा में सामाजिक जागरूकता प्रदान करें। ज्ञान एक संक्रामक बीमारी है, वह आसपास के लोगों को अप्रभावित नहीं छोड़ता।
क. – कहा जाता है कि आपके तथाकथित स्त्री-विमर्श और व्यावहारिक जीवन के बीच विचारों की एक लम्बी खाई है, इस खाई का कारण…? आपने इसे पाटने की कोई कोशिश की है? जिस अन्तर्विरोध की चर्चा आप विचार लेखन के स्तर पर निर्मल और मटियानी में देखते-करते हैं, कहीं उसके शिकार खुद भी तो नहीं…?
रा. या. – यह सही है कि व्यक्ति का जीवन बहुत से सामाजिक दबावों और तनावों के बीच होता है, मगर सबसे पहले उसकी चेतना, मानसिक और बौद्धिक स्तर पर घटित होती है। मनुष्य का सोच उसके शरीर के मुकाबले अधिक स्वतन्त्र है, आज हम जहाँ हैं, वैसा होने के सपने सदियों पहले कुछ लोगों ने देखे थे। चाँद पर जाने का सपना कितनी सदियों में जाकर पूरा हुआ है? स्त्री-विमर्श को लेकर जो कुछ मैं सोचता हूँ, व्यवहार में ठीक यही नहीं कर पाता हूँ, मगर व्यक्तित्व के इस अन्तर्विरोध को लेकर मैं बहुत सन्तुष्ट नहीं हूँ और मैं उसे पाटने की कोशिश भी करता हूँ। निर्मल और शैलेश मटियानी जैसे लोग इस अन्तर्विरोध को जैसे का तैसा कायम रखना चाहते हैं और इसे कहीं से भी गलत नहीं मानते। जबकि मैं इसे अपने व्यक्तित्व की कमी समझकर बार-बार अपने विचारों को संशोधित-परिवर्धित करने की मानसिक प्रतिक्रिया से गुज़ारता रहा हूँ। यह सिर्फ बाहरी स्त्री-विमर्श नहीं, बल्कि अपने-आपको पुनःसंयोजित करने का प्रशिक्षण भी है…
क. – ‘होना-सोना एक खूबसूरत दुश्मन के साथ’ के लिए जितना ज़्यादा बवाल मचा, मुझे लगता है उसकी ज़रूरत नहीं थी। शर्मिन्दगी की बात यह है कि उसका सबसे ज्यादा विरोध लेखक समुदाय और उसमें भी ज़्यादा स्त्री समुदाय के द्वारा हुआ। बचाव-पक्ष में आपका यह चिल्लाते रहना कि यह लेख पुरुष समुदाय की उस वृत्ति का खुलासा है जो वह प्रत्यक्ष रूप या परोक्ष में सोचता बोलता है, कि यह लेख महिलाओं के प्रति गहरे सम्मान और संवेदना के साथ लिखा गया है भी कुछ खास काम नहीं कर सका। क्या यह लेख अपने भीतर के उस अंतर्विरोध को पाटने की कोशिश नहीं, जिसका खुलासा आपने अभी किया है कि यह अपने आप से लड़ी गयी, अपने मनोवृत्तियों से लड़ी गयी लड़ाई है?
रा. या. – तुमने ठीक पकड़ा ‘होना-सोना’ लिखने और उस जैसी भाषा में लिखने के लिए मुझे सबसे पहली लड़ाई खुद से ही लड़नी थी; अपने अन्तर्विरोधों को भी खोलना पकड़ना था क्यों कि आखिरकार मैं भी तो उसी पुरुष-समुदाय का हिस्सा था। वैसे मैंने जोमें औरत’ में बहुत पहले लिख चुका हूँ। फर्क सिर्फ भाषा या शैली का है जिसके द्वारा मैंने बताने की कोशिश की है कि पुरुष की आन्तरिक बनावट उसकी सामन्ती मानसिकता निर्लज्ज मर्दानी भाषा में किसी प्रकार प्रकट होती है। मैंने इस सन्दर्भ में अनेक बार कहा है और आज फिर कह रहा हूँ कि वहाँ सिर्फ वही है जो पुरुष मानसिकता दिन-रात अपने आचार-व्यवहार में करती या बोलती है। शायद पुरुष का यह वो कुरूप चेहरा है जिसे वह शीशे में देखने से डरता है; यदि तुलसीदास के मन में सीता के प्रति अटूट सम्मान न होता तो वे रावण द्वारा सीता को कहे गये दुर्वचनों को उतनी ईमानदारी से नहीं लिख सकते थे। यह लेख भी स्त्री-जाति के प्रति उसी गहरे सम्मान के साथ लिखा गया है।
मेरे लिए यह हैरानी की बात ही थी कि स्त्रियों को इस लेख से आपत्ति थी या इसे पढ़कर वे शर्म महसूस कर रही थीं। मैं चुनौती देता हूँ कि कोई स्त्री यह कहे कि वह इस भाषा को सुनती या समझती नहीं है? आँधी के डर से रेत में मुँह छुपा लेने वाले शुतुरमुर्ग की तरह पुरुष के विचारों और गालियों की अनदेखी कर जाना कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं, इतना साहस भी न जुटा पाना कि चुप रह जाने की बजाय वे बुलन्द आवाज़ में प्रतिरोध करें या जवाब दें। मुझे ऐसे आडम्बरी स्त्री-पुरुष दोनों से घृणा है जो देखे और जाने हुए को जुबान पर लाने में नैतिकता की दुहाई देने लगते हैं। स्त्री को लक्ष्य करके जिस सबको बोलने में पुरुष को कोई शर्म नहीं है उसे सिर्फ दुहराने में स्त्रियों की नानी मरती है।

क.- इसके पीछे कौन-सा कारण है कि पढ़ी-लिखी और नौकरीपेशा स्त्रियाँ भी घरेलू उत्पीड़न का शिकार उसी मात्रा में होती हैं, जिसमें अनपढ़ या कम पढ़ी-लिखी स्त्रियाँ? शिक्षा और स्वावलम्बन ने यदि स्त्रियों के चरित्र में ज़रूरी बदलाव नहीं किए तो फिर ‘नारी स्वातन्त्र्य’ के मोर्चे पर इनकी क्या भूमिका रह गयी?
रा.या.- स्त्रियों की चली आती मानसिकता है सुख और सुरक्षा के लिए समझौता, पुरुष से भय और अपनी कमजोरियों को स्वीकारने का पराजयबोध। पुरुष उनके इसी असुरक्षाबोध का फायदा उठाकर मनमानी करता है, अगर वह घर से निकाल दे तो हम कहाँ जाएँगी, हमारे चरित्र पर क्या-क्या लांछन लगेंगे, हम कहाँ मुँह दिखाएँगी, यह भय स्त्री को पुरुष के हर अत्याचार को सहने का तर्क देता है। हालाँकि आर्थिक रूप से स्वतन्त्र महिलाएँ भी इस गुलामी से स्वतन्त्र नहीं हैं, आदमी बच्चों का वास्ता देकर उसकी सामाजिक असुरक्षा का खाका खींचकर और शारीरिक कमज़ोरियों का बखान करके जैसे चाहता है उन्हें वैसे ही नचाता है। अगर कोई गुलाम अपने पर होने वाले अत्याचारों का प्रतिरोध नहीं करता तो वह निश्चय ही मालिक का सहयोगी है। वह औरत के भीतर इस संस्कार को ठोंक-ठोंककर बैठा देना चाहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम उसी की हकदार हो, तुम्हारी भलाई उसी में निहित है।इसमें अधिकांश कमज़ोरी स्त्री की ही है कि वह पति और संरक्षक के रूप में एक डोमिनेटिंग (दबंग) पुरुष की कामना करती है, जब जानवर खुद ही अपना सिर जुए के नीचे डालने को बेचैन हो तब हम और आप क्या कर सकते हैं… नहीं, शायद तभी यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कुछ करें…
क. – ऐसा अचानक क्या हुआ कि आज की महिलाओं ने स्त्री-स्वतन्त्रता के आन्दोलन के नाम पर पुरुषवादी मनोवृत्तियों के विरोध की बजाय पुरुष-विरोधी माहौल को तैयार करना शुरू कर दिया, वे वृत्तियों को गलियाने या, उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश के बजाय पूरे पुरुष सम्प्रदाय को गलियाना ही अपना परम-धर्म समझने लगीं। आन्दोलन का यह स्वरूप आपकी नज़र में कहाँ तक जायज़ है?
रा. या. – कभी-कभी जब हम व्यक्तिवादी संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदलते हैं यानी पुरुष और पुरुष मानसिकता को अलग करते हैं तो उसके पीछे एक चालाकी काम करती है। यह ऐसा ही है जैसे हमें हत्यारों पर नहीं हत्यारों की मानसिकता पर बात ही करनी चाहिए, इससे हत्यारा मुक्त हो जाता है और सारी बातचीत अमूर्त मानसिकता पर होने लगती है। मानसिकताएँ या प्रवृत्तियाँ किन्हीं माध्यमों से प्रकट होती हैं और हमारा साबिका उन्हीं से पड़ता है। सामन्तवादी पुरुष का विरोध करना और मानसिकता से लड़ना एक ही बात है। इसलिए जब तुम कहती हो कि पुरुष से नहीं, उसकी मानसिकता से लड़ा जाए तो कन्फ्यूज़न उत्पन्न करती हो। क्या मानसिकता व्यक्ति से अलग कहीं बाहर रखी हुई चीज़ है और क्या यह पुरुष के पूरे सोच और आचार-व्यवहार से प्रकट नहीं होती? अगर होती हैं तो विरोध उसी का करना होगा, उस पूरे पुरुष का। सही सन्तुलन तो यह होगा कि हम सिर्फ व्यक्ति या सिर्फ मनोवृत्ति का विरोध न करें बल्कि दोनों मुद्दों को एक साथ लेकर चलें। गफलत तभी पैदा होती है जब हम पूरे सच को समझे बिना सिर्फ व्यक्ति का विरोध करते हैं। स्त्री-मुक्ति का संघर्ष सामन्तवादी मानसिकता वाली पुरुष-जाति से है।
क. – कुछ महिला रचनाकारों को अपने लेखन के आगे स्त्री-लेखन का ठप्पा पसन्द नहीं, वे सिर्फ लेखक कहलाना ज़्यादा पसन्द करती हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है…
रा. या. – मैंने जब कृष्णा सोबती से यह सवाल पूछा कि वे पहले महिला हैं या लेखिका तो अपने स्वभाव के अनुसार उन्होंने वही गोलमोल जवाब पकड़ा दिया जो वे शुरू से करती आ रही हैं। उन्हें स्त्री कहलाने में शर्म है। कृष्णा सोबती और मृदुला गर्ग जैसी महिलाएँ जब महिला ठप्पे का विरोध करती हैं तो मुझे अंग्रेजी राज्य के समय के उन ईसाइयों की स्मृति हो आती है जो अपने को भारतीय कहलाने का विरोध करते थे और आग्रह करते थे कि उन्हें भी अंग्रेज़ ही कहा जाए। यह हीनता की भावना है और सत्तावानों के साथ अपने को शामिल किए जाने की आकांक्षा भी, मुहावरे में कहूँ तो यह पाँचवें सवार की कुण्ठा है, जिसे सुन-देखकर बस दो बातों का ख्याल आता है-एक लड़की जो लड़कों की तरह पली या पाली गयी है इस बात का उग्र विरोध करती है कि उसे लड़की समझा जाए। लेकिन प्रकृति जब उसे यह बता देती है कि वह सिर्फ लड़की है तो उसे इस नियति से समझौता करने में काफी द्वन्द्व से गुजरना होता है। किशोर अवस्था में भी कुछ ऐसा ही होता है, एक किशोर हमेशा बचपन और युवा होने के द्वन्द्व में बँटा रहता है। युवा वह होता नहीं और बच्चा कहलाना उसके आत्म-सम्मान के विरुद्ध होता है। मुझे लगता है कि यह महिलाएँ लेखन को एक ‘मोनोलेथिक’ वस्तु समझती हैं और अभी किशोर-मानसिक अवस्था से ऊपर नहीं उठ पाई हैं, वरना पश्चिम में जहाँ लेखन वयस्क हो चुका है किसी लेखक को न अपने ‘ब्लैक लेखक’ कहलाने में कोई शर्म या झिझक है न महिला लेखिका। भारतीय स्त्री-लेखन के लिए मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि स्त्री होना उनकी नियति है और लेखक होना उनका चुनाव, जो प्रक्रिया बहुत बाद में उनके जीवन से जुड़ी है, इन बातों को उन्हें समझने-स्वीकारने का साहस होना चाहिए।
क. – विमर्श का सही स्वरूप क्या होना चाहिए, वर्तमान समय में उसकी सही दिशा क्या है?
रा.या. – सही स्वरूप क्या हो यह कहना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है क्योंकि कुछ आन्दोलन जो बहुत नये होते हैं अपने विकास के साथ ही अपना स्वरूप ग्रहण करते हैं। मैं समझता हूँ कि स्त्री-विमर्श का सही स्वरूप तभी बनेगा जब स्त्री बिना किसी दबाव लिहाज के अपने बारे में अपना निर्णय स्वयं ले सकेगी। अपने साथ उसे पुरुष को भी मुक्त करना होगा। अभी तो स्थिति यह है कि पहले उसे मर्द अपनी सम्पत्ति की तरह इस्तेमाल करता था और अब मुक्ति का भ्रम देकर बाज़ार उसकी नुमाइश कर रहा है। मगर उसका संघर्ष सिर्फ बाज़ार ही नहीं है, उसका संघर्ष अपने जैसे दूसरे मुक्ति-संघर्षों के साथ जुड़कर ही प्रभावी बन सकता है। उन्हें यह समझना ज़रूरी है कि दलितों और दूसरे हाशियाकृत लोगों के साथ मिलकर ही वे अपना भविष्य तय कर सकती हैं। मुक्ति अकेले की नहीं होती, वह अपने जैसों को साथ लेकर होती है। समाज निरपेक्ष अकेले की मुक्ति अन्ततः आत्महत्या या धर्म के रास्ते पर ले जाती है। बहुत अधिक व्यक्ति-स्वातन्त्र्य की ऐसी हिमायती महिलाओं को भी मैंने या तो धर्म की शरण में पनाह लेते देखा है या मृत्यु की, बात दोनों एक ही हैं…
क. – फिर भी आपको कमी कहाँ लगती है?
रा.या.- देखो, जब दलित या स्त्री जब सवर्ण या मर्द जैसी सत्ता पाने की आकांक्षा रखते हैं तो वे सत्ता के उन सारे गुणों को आत्मसात कर लेते हैं-यानी अपने से कमज़ोरों के लिए वे सत्तावानों जैसे ही हृदयहीन हो जाते हैं। इसलिए मेरी समझ में ज़रूरत उन जैसा बनने की नहीं, उनके बावजूद अपना जैसा बनने की है।
क. – नयी कहानी के दौर में आप लोगों ने अनुभूति की प्रामाणिकता पर ज़ोर दिया था, आज दलित लेखक भी यही कह रहे हैं, आपके इस विचार से क्या आपकी प्रतीक्षा, सिंहवाहिनी, ढोल जैसी कहानियाँ और सारा आकाश, अनदेखे अनजान पुल जैसे उपन्यास खारिज नहीं हो जाते? एक ही व्यक्ति अपने आपको कितने पात्रों में ढालेगा? क्या प्रतिनिधि की आवश्यकता तभी तक होती है जब तक कि बागडोर स्वयं भोक्ता के हाथों में नहीं आ जाए?
रा. या. – अनुभूति की प्रामाणिकता का अर्थ है- जो कुछ मेरे साथ घटित हुआ या जो मैंने अनुभव किया, या वे निजी अनुभव जो दूसरों के लिए भी उतने ही प्रामाणिक हों, वे विलक्षण अनुभव, वे अनुभूतियाँ जिनमें सम्प्रेषित होने के गुण हों, मेरे प्रेम की अनुभूति अगर बहुत गहरी और ईमानदार हो तो तुम्हें भी उतनी ही अपनी लगेगी या तुम्हारी संवेदना को भी उसी तरह आन्दोलित करेगी। आखिर बड़े कवियों की निहायत निजी अनुभूतियाँ कैसे हमारी अपनी हो जाती हैं।
जहाँ तक दलित लेखन का प्रश्न है तो वह लेखन मूलतः सामाजिक अपमानबोध का लेखन है, दरिद्रता, गरीबी, अशिक्षा के अलावा जो बातें उन्हें और उनके साहित्य को हमसे अलग करती हैं वह हैं अपमानबोध, अकेले होने की पीड़ा… अनुभव का सम्प्रेषण या साधारणीकरण एक ऐसे वर्ग की अपेक्षा करता है जिसके अनुभव लगभग समान हैं। दलित अनुभव अपने जैसे पीड़ित लोगों के बीच तो सम्प्रेषणीय है पर हमारे मन में सहानुभूति की जगह करुणा ही जगाता है, कुछ ऐसे भाव कि, ‘बेचारों को क्या-क्या नहीं भुगतना पड़ता है’, यह सम्प्रेषण को सहज नहीं रहने देता। वह व्यक्ति की बजाय सामाजिक, साधारणीकरण माँगता है।
क. – रचना में भोक्ता की उपस्थिति अगर इतनी ही ज़रूरी है और अपना ही खाया-पीया वमन करना है तो रचना परकाया-प्रवेश कहाँ रह जाती है? कई ऐसे भी लेखक हैं जो पूरे शोध के साथ किसी एक नये क्षेत्र या विषय को अपनी रचना में उठाते हैं और बहुत हद तक उसका प्रामाणिक और सामाजिक सन्दर्भों में भी चित्रण कर पाते हैं, तो क्या उनके लिखे को भी इस आधार पर खारिज कर देना चाहिए वे स्वयं उस रचना में शामिल नहीं…
रा. या. – हम जो कुछ भी खाते-पीते हैं, उसके उत्पादक हम स्वयं नहीं हैं, उसमें न जाने कितने श्रमों का योगदान है। जिसे मैं निजी अनुभूति कहता हूँ वह मेरे व्यक्तित्व में छनने और घुलने के बाद अन्ततः सामाजिकता के आईने से ही देखी-परखी जाती है, उसकी परिणति सामाजिकता में ही होती है। इसे आज की भाषा में ‘पर्सनल इज पॉलिटिकल’ कहा जाता है- ‘जो निजी है वही सार्वजनिक भी है।’ यहाँ बात वमन की नहीं, पचाने की है और उसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी दिखाई देता है यानी रचना के।
क. – यानी कि आप यह मानते हैं कि रचयिता का सीधे भोक्ता होना जरूरी नहीं। फिर तो आप यह भी मानते होंगे कि कोई जरूरी नहीं कि यदि ममता कालिया अनदेखे अनजाने पुल’ को या प्रकाश दीक्षित ‘सारा आकाश’ को लिखते तो हो सकता है कि वो ज़्यादा अच्छी या प्रामाणिक होती, खरी होती…
रा. या. – मैंने भले ही हीन भाव को लड़की की कुण्ठा से रिलेट किया है, पर यह कुण्ठा मेरी भी हो सकती है, किसी की भी, मूल प्रश्न वहाँ कुण्ठा का है और उससे उबरने का। ‘सारा आकाश’ के सारे अनुभव मेरे भी हैं, इसी परिवेश से उपजे हुए हैं, मैं भी इसी परिवेश से जुड़ा रहा हूँ… सारा आकाश के समय तक मेरी शादी नहीं हुई थी, इसलिए बाहरी डिटेल्स भले ही प्रकाश के हों, समस्याएँ मेरी ही थीं, मेरे समय की, समाज की। इसलिए मैं सचमुच नहीं मानता कि वे प्रामाणिक अनुभव नहीं हैं और चूँकि वे प्रामाणिक हैं इसीलिए अपने समय और समाज के भी हैं।
क. – निर्भय होकर लिखने में जो सबसे बड़ा भय होता है-वह यह कि हमारी तटस्थता या निस्पृहता से हमारा कोई अंतरंग आहत न हो, जबकि आपकी अधिकतर कहानियाँ या उपन्यास किसी-न-किसी खास चेहरे की तरफ उँगली उठाते हैं। सम्बन्धों के टूटने का भय क्या आपको कभी नहीं सताता या कमज़ोर करता? सिर्फ लेखन की खातिर क्या अपने आस-पास के लोगों और समाज से इतनी निर्ममता उचित है?
रा. या. – कोई क्या कहेगा, क्या सोचेगा का जितना भी लिहाज़ हम करेंगे दुनिया की उन्नति उतनी ही बाधित होगी न जाने कितनी सचाइयाँ और यातनाएँ अनकही रह जाएँगी, जब-जब आप सत्य कहेंगे, किसी-न-किसी की भावनाएँ आहत होंगी ही। अगर मान लो मैं कहता हूँ कि मैं ईश्वर को नहीं मानता तो सारे ईश्वर-प्रेमियों को ठेस लगेगी। जब निजी और सामाजिक सत्य या मोटे रूप से यथास्थिति के खिलाफ दिया गया वक्तव्य सामने आयेगा तो किसी-न-किसी को आहत होना ही है। यह हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हम किस हद तक किसकी अप्रसन्नता बर्दाश्त कर सकते हैं। सही है कि हम कबीर के युग में नहीं हैं कि कहा जा सके ‘जो घर फूँके आपनौ, चलै हमारे साथ…’ लेकिन अगर सबकुछ जनरंजन या मनभावन ही कहते रहें तो हम कभी कुछ नया न सोच पाएँगे, न कर पाएँगे। “मत कहो आकाश में कुहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है” दुष्यन्त ने कहा था।
क. – कोई ऐसा वाकया जिसमें इस कारण आपके आपसी सम्बन्ध भी प्रभावित हुए हों…?
रा. या. – बहुत-सी प्रिय या अप्रिय घटनाएँ सामने आयीं। कई बार कइयों ने अपने को किसी-न-किसी चरित्र से आइडेंटिफाई किया। ‘खेल खिलौने’ कहानी को लेकर जिस घटना का मैंने पहले कई बार ज़िक्र किया है वह भी इसी श्रेणी की है और नवीनतम ‘हनुमान प्रसंग’ भी…
क. – ‘खेल खिलौने’ कहानी से सम्बन्धित वह घटना कौन-सी थी, मुझे इसके बारे में याद नहीं।
रा. या. – ‘जिस लड़की का इस कहानी में चित्रण है उसका वास्तविक प्रेमी मेरे घर आया। पहले तो डराता-धमकाता रहा… इसके बाद बैठकर रोने लगा कि आपने मुझे इतना हृदयहीन क्यों चित्रित किया है? मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि यह तुम नहीं कोई और है…
क. – ये प्रभाव तो नकारात्मक थे, कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया, जहाँ सामनेवाला अपने को पहचानकर खुश हुआ हो, या उसकी ज़िन्दगी में कोई धनात्मक परिवर्तन आया हो…?
‘कुलटा’ कहानी का जो पति है वह बच्चा पैदा नहीं कर सकता था। जैसाकि मैंने ‘मुड़-मुड़कर…’ में लिखा भी है, एक महिला ने मुझे पूरे एक पेज का पत्र लिखा कि मेरे पति भी कुछ इसी तरह के हैं और मैं आपसे एक बच्चा चाहती हूँ, यह पत्र मेरे लिए एक बड़ा धक्का था… ‘अनदेखे अनजान पुल’ को पढ़कर तो कई लड़कियों ने लिखा कि वे अपनी मनोग्रन्थियों से उबर सकीं… जिस सुनीति लड़की का मैंने जिक्र किया है वह बीमार थी और भुवाली में तपेदिक से लड़ रही थी।
नहीं चरित्रों से ज्यादा पाठकों के अच्छे पत्र आये, उन्होंने मेरे लेखन की सराहना की… तुम शायद इसको अच्छी तरह समझती हो कि मेरे जितने भी पात्र हैं, जीवित-जाग्रत व्यक्ति हैं। अधिकांश रचनाओं के साथ तो यही हुआ कि जहाँ तक लोगों ने पढ़ा और उन्हें स्वीकार हुआ वे मेरी प्रशंसा करते रहे पर जैसे ही पात्र उन्हें अपने से थोड़ा हटा हुआ लगा तो विरोधी हो गये। सभी जानते हैं कि जब हम रचना करते हैं तो जो मुख्य करैक्टर होता है, वह तो होता ही है, लेकिन चरित्र अपनी योजना में ढालने के दौरान वैसे ही कई और चरित्र भी उसमें घुल-मिल गये होते हैं। लिखना बहुत हद तक सपना देखने की तरह होता है जिसमें चेहरा तो किसी का होता है और आँखें दूसरे की। नाक तीसरे की। जगह कोई होती है, घर कोई और सदस्य किसी और परिवार के।
इसी सन्दर्भ में एक घटना… मेरा एक नौकर था, बहुत ही स्नेही और लगाव रखने वाला, खुलकर और साफ-साफ बोलने वाला। जब वह चला गया तो मैंने उस पर एक कहानी लिखी। रेडियो पर कभी उस कहानी को पढ़ा भी, उसने न जाने कैसे सुन लिया और आकर मुझसे बड़ी बेचैनी से पूछने लगा कि साहब मैं ऐसा हूँ या, मेरी आदतें इतनी बुरी हैं… मेरी अधिकतर कहानियों के साथ ऐसा ही है, पहले तो लोग खुद को पहचानकर खुश होते हैं… फिर थोड़ी देर बाद बेचैन… उन्हें यह लगने लगता है कि वे ऐसे नहीं हैं कि उनका मजाक उड़ाया गया और अपमान किया गया है।
प्र. – अपने सम्पादकीय, लेखों और साक्षात्कारों में आपने बार-बार निर्मल जी से लेखन को ‘स्थगित लेखन’ कहा है, वरन् उन्हें ही नहीं आपने अपनी पीढ़ी के कई लेखकों के बारे में ऐसे बयान दिए हैं कि उनके लेखन में नया कुछ भी नहीं है और वो लिखने की विधा को साध लेने पर किए गये भाषागत और शिल्पगत अभ्यास भर हैं। फिर भी वह क्या कारण है कि उनकी नयी किताबें चाहें वो ‘अन्तिम अरण्य’ हो ‘कितने पाकिस्तान’ हो या ‘समय सरगम’ धुआँधार बिकती हैं? क्या आज का पाठक इतना बोदा या मूर्ख है कि ये बातें उसे समझ में नहीं आतीं?
रा. या. – देखो, लेखक के लिए पाठक खाद-पानी की तरह जरूरी है, मगर लेखक जंब पाठक की अपेक्षाओं का बन्दी हो जाता है, तब उसका विकास बन्द हो जाता है। मैं मानता हूँ कि एक ‘जेनुईन’ लेखक को अलोकप्रिय होने का जोखिम उठाकर भी पाठकों द्वारा बने-बनाए फ्रेम को तोड़ते रहना चाहिए। जहाँ तक पाठकों की संख्या की बात है तो यह स्थिति सिर्फ निर्मल की ही नहीं है, ‘गुनाहों के देवता’ के पाठक उनसे पचास गुना ज़्यादा हैं और मेरे भी कम नहीं हैं। लेखकीय विकास और पाठकीय लोकप्रियता न एक होते हैं न समानान्तर दिशा में जाते हैं।
जहाँ तक निर्मल के लेखन का प्रश्न है तो मुझे लगता है कि उनकी प्रारम्भिक कहानियों के पात्र जिस एकाकीपन और संवादहीनता की स्थिति में कैद थे आज तक वहीं कैद हैं और उसी संवादहीनता की स्थिति को वे आज तक अलग-अलग नामों से दुहरा रहे हैं। उनके पास न सपना है, न भविष्य, सिर्फ अतीत है और निर्मल का यही अतीत वैचारिक लेखन के रूप में आता है। वे वहीं रुके और उसकी आरती उतार रहे हैं। भारतीय अतीत कितना महान मोहक और अद्वितीय था इसी को वे अपनी रहस्यवादी और सांध्य-भाषा में दुहराते रहते हैं। अपनी इस अतीतग्रस्तता में निर्मल सारे आधुनिक लेखकों के हवाले और नये वैचारिक मुहावरों के बावजूद पुराणवाचक साधु-सन्तों की याद दिलाते हैं, जिनकी एकमात्र चिन्ता ‘मोक्ष’ और आज के शब्दों में ‘मुक्ति’ है। निर्मल के पात्रों की तार्किक परिणति मृत्यु ही हो सकती है। “मौत से पहले आदमी इनसे निजात पाए क्यूँ।”

क. – आपने अपने एक इण्टरव्यू में कहा है कि मोहन राकेश ने अपने घनिष्ठ लोगों से धीरे-धीरे अपने को काट लिया था, अपनी डायरी में उसने जिन 10 लोगों को ‘टुच्चा’ कहकर याद किया (जिसमें एक नाम आपका भी था…) वे कभी उसके सबसे निकटस्थ थे। आप इस मनोग्रन्थि का कारण क्या समझते हैं? उनकी लेखकीय महत्वाकांक्षा या सुपीरियरिटी ‘कॉम्पलेक्स’?
रा. या. – इस कटाव का कारण था उसका जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास कि वह सही है दूसरे गलत। या यह कि वह दुश्मनों से घिरा ऐसा शहीद है जो किसी महान ‘कॉज’ के लिए अपने और अपने साथवालों का बलिदान करता है। उसके अपने जब अलग होते हैं, तो वह यही ओट लेता है कि वह बलिदानी है, वहाँ खुद अपने को जाँचने का कोई प्रयास नहीं है… शायद हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति के साथ यही होता है।
क. – क्या आपके सन्दर्भ में भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे वे नाम या रिश्ते कभी आपके निकटस्थ और आत्मीय वे उनसे आपकी दूरियाँ बनती गयीं। अर्चना जी ने आपके ऊपर केन्द्रित अपने संस्मरण ‘तोते की जान’ में लिखा है कि जैसे ही आपको यह महसूस होता है कि कोई रिश्ता या व्यक्ति आपकी कमज़ोरी बन रहा है आप उसे झटककर दूर खड़े हो जाते हैं; आपने इस मुद्दे पर खुद को कभी टटोला है?
रा. या. – खुद अर्चना मेरे साथ 35 साल से जुड़ी रही है। मगर क्या इस दृष्टि से मैं अपने को अलग मानता हूँ… मैं समझता हूँ कि इसके पीछे मेरी किशोर अवस्था की कुण्ठाएँ हैं, एक्सीडेण्ट की वजह से जो शारीरिक कमी आई उसको लेकर मेरे मन में एक डर घर कर गया कि मुझे दूसरों पर निर्भर रहना होगा। आश्रित रहने का अर्थ अपनी स्वतन्त्रता का परित्याग था, यहीं से एक संकल्प मेरे मन में आकार लेने लगा कि मुझे हर तरह के दबावों, कमजोरियों और उन निर्बलताओं से बचना होगा, जो मुझे निर्भर बनाती हैं या मेरी स्वतन्त्रता का हरण करती हैं। बाद में यह स्वतन्त्रता ‘लेखकीय स्वतंत्रता’ में बदल गयी और इसके लिए मैंने ऐसी नौकरियों को, पुरस्कारों-सम्मानों और इस तरह की बाहरी सहायताओं को अस्वीकार करना शुरू कर दिया, जो कहीं से भी लेखकीय स्वतन्त्रता को प्रभावित कर सकती थीं। हो सकता है, बल्कि मेरा यह सोचना उस सीमा तक गया कि इसमें वे सम्बन्ध भी आ गये जो इतने अधिक अन्तरंग थे कि मुझे लगा वे मुझे बाँध रहे हैं, और मेरी स्वतन्त्रता को प्रभावित कर रहे हैं। उस अर्थ में हो सकता है कि अर्चना का विश्लेषण सही हो कि मैं भाग खड़ा होता हूँ… यह ‘दूसरे को धोखा देने से ज्यादा अपने को बचाने की कटु आवृत्ति है…’
क. – मन्नू जी ने अपने बिलकुल एक ताजा साक्षात्कार में (शायद ‘राष्ट्रीय सहारा’ में) आपके लिए लिखा है ‘जब उन्हें सम्बन्ध तोड़ना ही था तो बनाया क्यों?’ आपने भी अभी स्वीकारा कि मेरे मन में हमेशा से अपनी अपूर्णता को लेकर एक कुण्ठा थी, कि मुझे दूसरों पर आश्रित नहीं होना है-जो यह सिद्ध करता है कि आप जानते थे कि शादी या किसी ऐसे रिश्ते की परिणति अन्ततः क्या होनी है?… ‘साहिर’ ने लिखा है-‘वो अफसाना जिसे तकमील तक ले जाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा…’ पर वह क्या वजह रही कि आपका रिश्ता उस खूबसूरत मोड़ पर थम नहीं सका… आरोपों-प्रत्यारोपों का यह सिलसिला अच्छी मित्रता की गवाही तो नहीं ही देता…
रा. या. – रिश्ते की परिणति क्या है, मुझे यह पता नहीं था… फिर भी मन्नू और मैं दोस्त तो अच्छे हैं ही… वह दोस्ती का सम्बन्ध ही हो सकता है जहाँ हम खुलकर एक-दूसरे की खामियों-खूबियों को गिना सकते हैं… पति-पत्नी का जो बँधा-बँधाया सम्बन्ध है… उसका निर्वाह मेरे लिए मुश्किल था। हालाँकि वह सम्बन्ध भी दोस्ती की ही परिणति था। 44 साल लगातार हम यही अनुभव करते रहे कि हम अच्छे दोस्त हो सकते हैं, अच्छे पति-पत्नी नहीं। आज जो सम्बन्ध तुम देख रही हो वो मैत्री के ही हैं…इस पर मेरे और दूसरों के द्वारा इतना कुछ बोला और लिखा जा चुका है कि मैं अब चुप रहना ही पसन्द करता हूँ… कोई भी स्वतन्त्र सम्बन्ध जब उस फ्रेम को स्वीकार करता है जो सैकड़ों सालों से चला आ रहा है और आज लगभग स्वायत्त हो गया है, अपनी शर्तों और सीमाओं के साथ प्रभावी होता है। विवाह एक ऐसी ही संस्था है। बचपन के घनिष्ठ दोस्त जब एक ही संस्था में नौकर हो जाते हैं तो उनके बीच सम्बन्ध वही नहीं रहते तुमने ‘नमकहराम’ फिल्म तो देखी होगी…
क. – क़ई एक ठोस कारण अलगाव का आप नहीं दे पा रहे हैं… ‘हो सकता है’ की शब्दावली से परे मैं आपसे कुछ स्पष्ट जानना चाहती हूँ… वैसे यदि आप चाहें तो हम इस सवाल को यहीं छोड़कर आगे बढ़ें…
रा. या. – अर्चना वाली बात ही सही लगती है, मनुष्य की स्वतन्त्रता को कुचलने वाले जो तन्त्र हैं उसमें धर्म, नैतिकता और सत्ता की प्रमुखता है, मैं शायद इन्हीं स्तरों पर इनसे मुक्ति चाहता था। मैंने बार-बार इन सवालों को समझने-पुनर्व्याख्यायित करने की कोशिश की है… किसी भी तरह के सम्बन्ध जब रूढ़ और यथास्थितिवादी हो जाते हैं तो मुझे बेचैनी होती है। शायद यही द्वन्द्व कहीं मेरे और मन्नू के बीच भी रहा है… चाहो तो बँधी-बँधाई शब्दावली में यह भी कह सकती हो कि मैं पति की जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं था। जब साथ रहने के दौरान एक-दूसरे की अनुपस्थिति ज्यादा सुखकर लगने लगे तो समझना चाहिए कि सम्बन्धों का यह स्वरूप ज़्यादा नहीं चलेगा… यह दोनों की रचनात्मकता के लिए घातक है। तकलीफ मुझे यह है कि मेरे मुकाबले मन्नू की रचनात्मकता इससे ज्यादा प्रभावित हुई।
क. – अलग रहने का निर्णय पहले किस तरफ से हुआ…
रा. या. – बेकार प्रश्न है यह… अब पहल किसने की, भूख किसे लगी, इससे क्या बनता-बिगड़ता है… सच्चाई यह है कि भूख लगी थी और दोनों को लगी थी…
प्र – आपने जब अलग रहना शुरू किया तो कहा था कि ‘बस यह एक प्रयोग है, मैं और मन्नू लिखने-पढ़ने के लिए हमेशा ऐसा करते रहे हैं, मन्नू ने ‘आपका बण्टी’ हॉस्टल में रहकर लिखा-कहानियाँ लिखने के लिए अनेक बार बाहर या बाद में उज्जैन भी रही; मैं भी अक्सर लिखने के लिए बाहर जाता रहा हूँ…’ आप क्यों इस निर्णय को सरेआम आने नहीं देना चाह रहे थे?
रा. या. – नहीं, तब हमने इसे प्रयोग की ही तरह लिया था… पर इस बार वह कुछ ज्यादा लम्बा खिंच गया अब इस विषय पर आगे एक भी प्रश्न नहीं…
क. – आपके लेखन ने आपके दुश्मनों और दोस्तों दोनों की संख्या में बेशुमार वृद्धि की। आपकी नज़र में वह कौन-सा कारण है कि पढ़ने के बाद आपके लेखन से निस्पृह नहीं रहा जा सकता?
रा. या. – मैं अपने लेखन को उस ‘कैटेलिस्टिक एजेंट’ की तरह मानता हूँ, जिसके डालने से दूध और पानी अलग-अलग हो जाते हैं… शायद मेरा लेखन पाठकों के ध्रुवीकरण में मदद करता है, वे चुन सकते हैं कि उन्हें परिवर्तनकामी समाजधर्मी लेखन का पक्षधर होना है या कलात्मक विशिष्टताओं के व्यक्तिनिष्ठ लेखन के साथ। मैं मानता हूँ कि हम जिस हलचल भरे हंगामाखेज़ समय और धार्मिक कट्टरताओं के आतंक में जी रहे हैं वहाँ लेखक जैसा संवेदनशील प्राणी असंपृक्त और तटस्थ रह ही नहीं सकता, उसे वैचारिक धरातल पर अपने देश और काल से जूझना होगा… सामाजिक विकास की हलचलों से जूझते हम तीसरी दुनिया के लेखक हैं। हमारी समस्याएँ अमेरिका या यूरोप से बिलकुल अलग हैं। लेखक की सार्वभौमिकता वैसा ही बड़ा झूठ है, जैसा मानव-मात्र के सार्वभौमिक होने का भ्रम। निराकार और अमूर्त संसार में मानव-मात्र एक हो सकता है लेकिन जैसे ही हम उसे मनुष्य का शरीर देते हैं, वह देश में भी बँधा होता है और काल में भी। यूरोप और अमेरिका का व्यक्ति वही नहीं है जो पलामू या बिहार का है।
क. – आपने नाही-नाही करते हुए भी आखिर आत्म-कथा लिख ही डाली… गोकि वह पूरी तरह से व्यवस्थित और क्रमवार आत्मकथा भी नहीं… अलग-अलग समय और आयोजनों पर लिखे गये लेखों और संस्मरणों का एक साथ किया गया संयोजन मात्र है… प्रश्न यह कि आत्मकथा के लिए आपका वह जो एक व्यर्थताबोध वाला भाव था उसके बदलने की कोई खास वजह… आखिर मुड़-मुड़कर पीछे देखने का कुछ तो खास कारण होगा?
रा. या. – जो व्यवस्थित आत्मकथाएँ होती हैं क्या तुमने उन्हें कभी ध्यान से पढ़ा है? वस्तुतः हर आत्मकथा में संवेदनशील, निर्णायक और स्पन्दनशील हिस्से बीच-बीच में ही आते हैं, शेष आत्मकथा किसी व्यक्ति के जीवन के एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु तक पहुँचने की यात्रा होती है। ये स्पन्दनशील क्षण, स्मृतियाँ या स्थिति ही किसी लेखक की सारी मानसिकता, ऊर्जा या विचार का निर्माण करती हैं। मैंने ‘मुड़-मुड़कर देखता हूँ’ में सिर्फ दो ही काम किए हैं, एक तो अपने-आप को अपने से तोड़कर एक दूरी का निर्माण किया है ताकि ‘उस अपने’ को मैं एक नितान्त दूसरे आदमी की निगाह से देख सकूँ। दूसरे, मैंने अपने आप को एक कहानी के चरित्र के रूप में देखा है और उसी तरह फालतू विवरणों को काटा-छाँटा है। दूसरे शब्दों में उन संवेदनशील क्षणों को चुन लिया है, जो व्यक्ति का निर्माण करते हैं। इसलिए चाहो तो उन्हें आत्म-कथांश कह लो, चाहे वह दृश्य-दीप्ति, जिनका जिक्र अज्ञेय ने ‘शेखर : एक जीवनी’ की भूमिका में किया है; हर आत्मकथा यूँ भी एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक छलाँग लगाने की कथा है, वे अन्तःसूत्र भी वहाँ होते हैं जो बीच के जाल को महीन धागे से बुनते हैं। मैंने वह जाल नहीं बुना…
जहाँ तक व्यर्थताबोध की बात है, उसे मैंने ईमानदारी से स्वीकार किया है और अपने से ये सवाल करता रहा हूँ कि मेरे सारे प्रेम, सारी निष्ठा के बावजूद मैं अन्त तक अपने सहयात्रियों को जोड़कर नहीं रख सका। मुझमें कोई कमी रह गयी… मगर यहाँ देखने की बात यह है कि न मैं संन्यासी बना, न मैंने आत्महत्या की, न मैं अतीत की जुगाली करने में जुटा। इस व्यर्थताबोध ने मुझे एक भविष्योन्मुखी ऊर्जा ही प्रदान की है। मैं अपने लेखन और विचार के क्षेत्र में आज भी सक्रिय हूँ, न मुझे अनुभवों ने कुचला है, न पलायन या पराजय मेरी प्रवृत्ति बनी, “न दैन्यं न च पलायनम्, अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे।”
प्र. सवाल ‘हंस’ को लेकर। ‘हंस’ की कहानियों में एक खास तरह की मांसलता और ऐन्द्रिकता अपनी जगह बनाती दिखती है, क्या देह-चर्चा के बिना कोई भी कहानी अच्छी नहीं बन सकती…? क्या सम्पादन भी एक व्यवसाय है और ऐसी कहानियों का चयन आपके व्यक्तित्व का व्यावसायिक पक्ष?
रा. या. – इससे बड़ी बेवकूफाना बात कोई नहीं होता सकती कि ‘हंस’ में रचना या सामग्री पाठकों को लुभाने के लिए या व्यावसायिक दृष्टिकोण से दी जाती है। ‘हंस’ जैसी पत्रिका में यदि कोई तथाकथित अश्लील कहानी छपती है तो उससे किस हद तक व्यावसायिक लाभ हो सकता है, यह तुम भी जानती हो? मामला व्यवसाय का उतना नहीं जितना दृष्टिकोण का है। मैं यह सोच नहीं पाता कि जब मैं राजनीतिक, धार्मिक संस्कृतिवाद से समझौता नहीं कर पाता, तो इन झूठी नैतिक मान्यताओं के आगे क्यों सिर झुकाऊँ?
अस्वीकार के क्षेत्र क्या चुन-चुनकर तय करने होंगे? क्या यह ऐसा चुनाव है जिसे दूसरे तय करेंगे?
मैंने शुरू से ही ‘हंस’ को भाषा, कथ्य और विचार के क्षेत्र में उन प्रश्नों का मंच बनाया है, जिन्हें हमेशा कुचला और अनदेखा किया गया-कभी जाति, कभी भाषा, कभी कथ्य या फिर वर्ण-व्यवस्था के नाम पर। जो लोग ‘हंस’ को ध्यान से पढ़ते हैं, उन्हें पता लग जाना चाहिए कि शिष्टता, नैतिकता, सुरुचि कहकर जो धार्मिक किस्म का औपनिवेशिक और विक्टोरियन सौन्दर्यबोध हमारे ऊपर लाद दिया गया है, ‘हंस’ उस सबके खिलाफ एक विद्रोह की आवाज है।
वर्ण-व्यवस्था सिर्फ जातिवाद में ही नहीं है, सम्प्रदायवाद से लेकर सौन्दर्यबोध और भाषा के ‘एक्स्क्लूसिविज्म’ में भी है, जहाँ 80 प्रतिशत लोगों की भाषा और स्मृतियाँ अश्लील कहकर प्रवेश निषेध की तख्तियाँ लगा दी जाती हैं। वो चाहे काशीनाथ सिंह के अस्सी के निवासियों की बोलचाल की भाषा हो, चाहे मैत्रेयी पुष्पा की देहधर्मी कहानियाँ उपन्यास।
मुझे ‘अशोक वाजपेयी’ और नामवर जैसों का ‘आडम्बरी आभिजात्य’ और उच्चतर कलात्मक मूल्यों के नाम पर अमूर्तनों का चित्रांकन बहुत ज्यादा गले नहीं उतरता, इसलिए ‘हंस’ की तथाकथित अश्लीलता को मैं बिछड़े और पिछड़े लोगों की पुनर्वापसी का नाम देना चाहता हूँ, उनसे संवाद करना चाहता हूँ जिन्हें हमने कभी बात करने लायक नहीं समझा। बोलने तो दिया ही नहीं, क्योंकि उनकी भाषा हमें फूहड़ और अश्लील लगती है। फिर जो लेखक ‘हंस’ में लिखते हैं वे सब समर्थ और व्यक्तित्ववान है, क्या मैं उन्हें अपने हिसाब से लिखने को मजबूर कर सकता हैं? ऐसा कहना उनका अपमान करना है।

प्र – आपको नहीं लगता कि इस बहस-बातचीत-लेख या सम्पादकीय में आप जरूरत-बेजरूरत कुछ नामों को घसीट लाते हैं, जबकि बिना उन नामों के उदाहरण दिये भी बात उतनी ही स्पष्ट होती हैं या आप उसे ऐसे भी कह सकते हैं।
रा. या. – जिन नामों को बार-बार लेने का आरोप तुम मुझ पर लगा रही हो, उन व्यक्तियों से मेरी कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं है, वे मेरे सभ्य-शिष्ट मित्र लोग हैं। पर जहाँ भी मैं उनके नाम का प्रयोग करता हूँ प्रवृत्ति के रूप में ही हैं। आज के सन्दर्भ में किसी नाम का कोई अर्थ नहीं रह गया है, न ‘गाँधी’, न ‘तुलसी’ न अन्य कोई-ये सारे नाम प्रवृत्तियों और विचारधाराओं के सुविधाजनक नाम हैं…
क. – ‘इण्डिया टुडे’ के नये अंक में आपकी दो कहानियाँ (लघु-कथाएँ) आनेवाली हैं, उनका लेखन-स्रोत क्या है, क्या उनके पहले भी ‘हासिल’ जैसी कोई लम्बी-चौड़ी भूमिका है? ‘हासिल’ के पहले भी मेरी समझ से उस भूमिका की कोई आवश्यकता नहीं थी… यह कुछ वैसा नहीं जैसे कि अपराधी यह कहता है- ‘मैं अपराधी नहीं।’ पागल चीख-चीखकर पागल होने से इन्कार करता है… आपका यह सफाई देना भी कि यह कहानी आपके जीवन से सम्बन्धित नहीं, कहीं आपके…
रा. या. – नहीं, इनके आगे-पीछे कोई भूमिका नहीं है। कहानी अनुभव की प्रामाणिकता माँगती है…जब भी मुझे फुर्सत मिलती है मैं अपने अनुभवकोश के उसी हिस्से को ज्यादा रचनात्मक पाता हूँ जो निजी सम्बन्धों के साथ जुड़े हैं, अतः इण्डिया टुडे वाली कहानियों के केन्द्र में भी मेरा पिछला जीवन या परिचय ही है… और ‘हासिल’ कहानी की भूमिका को अगर मेरे ‘होना-सोना…’ वाले लेख की भूमिका के साथ मिलाकर पढ़ोगी तो चीजें ज्यादा साफ होंगी। मुझे शायद यह डर भी रहा होगा कि इन दोनों रचनाओं को सही सन्दर्भ में और स्वस्थ दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, इसलिए मुझे भूमिका के कौशल का सहारा लेना पड़ा। हालाँकि इस डर ने रचना पर कोई अंकुश नहीं लगाया, रचनाएँ जैसी थीं वैसी ही गयीं। अगर मुझे दूर की कौड़ी ही लानी हो तो मैं कहूँगा-‘हासिल’ नामवरजी के व्यंग्यार्थ पर ही लिखी गयी कहानी है। वे नये रचनाकारों से जिस तरह फ्लर्ट (लटर-पटर) करते हैं, और बाद में नये की ऊर्जा-दृष्टि और शक्ति के सामने पराजित होकर असफलता-बोध तक पहुँचते हैं, उस रोमांस को मैंने लेखक और लड़की यानी ‘सपना सन्दीप’ के रूप में दिया है।
क. – क्या आपको यह लगता है कि आपकी दोनों आनेवाली कहानियाँ आपकी पहले आ चुकी कहानियों के आगे बड़ी रेखा साबित होंगी?… क्या इसी डर से, आप कई कहानियों को (पहले लिखी) प्रकाशित करवाने से बचते रहे हैं…
रा. या. – मैं लिखने और छपने के बाद अपनी हर रचना को भूल जाता हूं। दुबारा तो शयद ही पढता हूं। लिखता डूबकर हूं फिर उससे पूरी तरह मुक्त हो जाता हूं। पुराना न मेरे लिए ब धक है, न साधक। इतने दिन तक साथ काम करके तुमने यह कभी नहीं देखा होगा कि मैंने शायद ही कभी अपनी किसी रचना पर अपनी तरफ से बात की हो।
‘इण्डिया टुडे’ के नये अंक में आपकी दो कहानियाँ (लघु-कथाएँ) आनेवाली हैं, उनका लेखन-स्रोत क्या है, क्या उनके पहले भी ‘हासिल’ जैसी कोई लम्बी-चौड़ी भूमिका है? ‘हासिल’ के पहले भी मेरी समझ से उस भूमिका की कोई आवश्यकता नहीं थी… यह कुछ वैसा नहीं जैसे कि अपराधी यह कहता है- ‘मैं अपराधी नहीं। पागल चीख-चीखकर पागल होने से इन्कार करता है… आपका यह सफाई देना भी कि यह कहानी आपके जीवन से सम्बन्धित नहीं, कहीं आपके…
नहीं, इनके आगे-पीछे कोई भूमिका नहीं है। कहानी अनुभव की प्रामाणिकता माँगती है… जब भी मुझे फुर्सत मिलती है मैं अपने अनुभवकोश के उसी हिस्से को ज्यादा रचनात्मक पाता हूँ जो निजी सम्बन्धों के साथ जुड़े हैं, अतः इण्डिया टुडे वाली कहानियों के केन्द्र में भी मेरा पिछला जीवन या परिचय ही है… और ‘हासिल’ कहानी की भूमिका को अगर मेरे ‘होना-सोना…’ वाले लेख की भूमिका के साथ मिलाकर पढ़ोगी तो चीजें ज्यादा साफ होंगी। मुझे शायद यह डर भी रहा होगा कि इन दोनों रचनाओं को सही सन्दर्भ में और स्वस्थ दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, इसलिए मुझे भूमिका के कौशल का सहारा लेना पड़ा। हालाँकि इस डर ने रचना पर कोई अंकुश नहीं लगाया, रचनाएँ जैसी थीं वैसी ही गयीं। अगर मुझे दूर की कौड़ी ही लानी हो तो मैं कहूँगा- ‘हासिल’ नामवरजी के व्यंग्यार्थ पर ही लिखी गयी कहानी है। वे नये रचनाकारों से जिस तरह फ्लर्ट (लटर-पटर) करते हैं, और बाद में नये की ऊर्जा-दृष्टि और शक्ति के सामने पराजित होकर असफलता-बोध तक पहुँचते हैं, उस रोमांस को मैंने लेखक और लड़की यानी ‘सपना सन्दीप’ के रूप में दिया है।
क. – आपका अचानक ही रचनात्मक लेखन से वैचारिक लेखन के क्षेत्र में चले आना, आपके साहित्यिक पाठकों के लिए निराशाजनक रहा। जबकि कुछ के लिए यह आपके व्यक्तित्व का ज्यादा प्रखर हिस्सा है… आपकी नज़र में यह सब क्या है?
रा. या. – पहली बात तो यह कि कोई लेखक क्या लिखे, यह चुनाव सिर्फ उसका और उसी का है, इसमें पाठकों और लेखकों की प्रत्याशाएँ सोच-सोचकर खुद को क्यों बाधित करूँ? यहाँ भी मुझे लगा कि मैं वैचारिक लेखन में ज्यादा सम्पूर्णता और प्रभाव के साथ अपने-आपको व्यक्त कर सकता हूँ, इसलिए आज मेरी प्राथमिकताएँ वही हैं। कहानी और उपन्यास एक ठहराव माँगते हैं जिसे ग़ालिब ने ‘फुर्सत के रात-दिन’ कहा है। उसमें कविताएँ तो लिखी जा सकती हैं, कहानियाँ नहीं। आज भी अच्छी कहानियाँ और उपन्यास वे ही लोग लिख रहे हैं जो महानगर की आपाधापी से अपने आपको काटे हुए हैं, अपनी रचनात्मक मानसिकता में जो अपने पात्रों के साथ ज्यादा वक्त तक रह सकने की स्थिति में हैं। इस भेद को गुजरात के हत्याकाण्ड के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। इस वध-उत्सव पर राजेश जोशी, मंगलेश डबराल, देवी प्रसाद मिश्र जैसे जमे हुए कवियों ने अद्भुत कविताएँ लिखी हैं, वे वहाँ के समाचारों और सूचनाओं से आन्दोलित संवेदना की कविताएँ हैं, मगर शायद कहानी एक भी नहीं लिखी गयी, क्योंकि कहानी में उन स्थितियों-पात्रों को निकट से देखना-जानना होता, जो बिना वहाँ गये सम्भव नहीं। यहाँ तक कि भुगतनेवाले वर्ग अर्थात् मुसलमानों की तरफ से हिन्दी में सिर्फ असगर वजाहत ने ही कहानियाँ लिखीं। यह भी सम्भव है कि कहानी लिखने या रचनात्मक लेखन से वैचारिक लेखन की ओर मुड़ने का एक कारण समयाभाव और जुड़ाव का न हो पाना भी हो…
क. – अपनी बातचीत और विचारधारा में ‘पर्सनल इज पॉलिटिकल’ का नारा देने के बावजूद आप निरन्तर लिखी जाने वाली अपनी डायरियों को नितान्त अपनी निजी सम्पत्ति के रूप में देखते हैं, और उन्हें अपने जीवनकाल में ही नष्ट कर देने और जला देने की बात करते हैं। जबकि कितने ही लेखकों की डायरियाँ आज प्रकाशित होकर उनके जीवन का एक अनदेखा पक्ष हमें दिखाती हैं। आपके मन में इनको प्रकाशित करवाने की कोई योजना क्यों नहीं है? आपका कटा-छँटा और सँवरा हुआ रूप ही पाठकों के सामने जाए यह क्या जरूरी है? जबकि आप दूसरों के ऐसे तराशे सच का विरोध करते हैं?
रा. या. – लेखक और व्यक्ति में अन्तर करना चाहिए, मैं अपनी जिन डायरियों को नष्ट करने की बात करता हूँ, वे एक व्यक्ति के निजी अनुभव हैं, लेखक के अनुभवों का इन्दराज नहीं। दूसरे मैं मानता हूँ कि ‘प्राइवेट’ और ‘पर्सनल’ में अन्तर है। प्राइवेट वह है जो हम दूसरों को न दिखाना चाहेंगे, न उसमें दूसरों का हस्तक्षेप बर्दाश्त करेंगे। बाथरूम मेरा प्राइवेट मामला है, ड्राइंगरूम मेरा पर्सनल, उसमें दूसरे भी आ सकते हैं, मेरे कपड़े मेरे निजी होने के बावजूद एक विशेष समाज का हिस्सा भी हैं, उस पर सभी को टिप्पणी करने का हक बनता है… जिन छपी हुई डायरियों की तुम बात कर रही हो, वे शायद हमेशा छपने-छपाने के ध्येय से ही लिखी गयी थीं। लेखक उन्हें लिखते वक्त पाठकों की रुचि-अरुचि को ध्यान में रखकर सचेत था और लेखक के मन में यह विश्वास भी था कि वह साहित्य को कुछ बहुमूल्य दे रहा है… मेरे भीतर यह विश्वास नहीं… मेरी डायरियाँ सिर्फ मेरे लिए हैं… पुराने को याद करने के लिए या उस दुनिया को पुनः जगाकर अपनी रचनात्मकता के लिए कोई सूत्र तलाशने के लिए। इन्हीं सब कारणों से डायरी के प्रकाशन की कोई इच्छा मुझमें नहीं है।
इधर तो दसियों वर्षों से मैंने डायरियाँ लिखना ही बन्द कर दिया है। अगर दुष्ट-बुद्धि का सहारा लूँ तो कहूँगा कि इघर कथनी और करनी का अन्तर शायद मिट गया है। कथनी और करनी में एक हिस्सा वह होता है जो निजी होता है और कर्म के रूप में बदल नहीं पाता। इसे पब्लिक और पर्सनल भी कह सकते हैं। इस अन्तर्विरोध की चेतना जिसमें जितनी तीव्र है, वह उतना ही संवेदनशील है। डायरियाँ उसी निजी संवेदनशीलता की प्रविष्टियाँ होती हैं-यानी जो कुछ हम महसूस तो करते हैं, मगर दूसरों के सामने कह नहीं पाते। हो सकता है, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत इतना महत्त्वपूर्ण नहीं है कि उसे ‘ऐतिहासिक दस्तावेज़’ के नाम पर सुरक्षित रखा जाए। यह भी हो सकता है कि कथनी और करनी की दूरी कम हो गयी हो-या मुझे ही लगता हो कि कम हो गयी है। हालाँकि किसी भी समय में व्यक्तिगत और सामाजिक की दूरी नहीं रहेगी यह सोचना मूर्खता है। खानाबदोश लोगों के पास अपना ऐसा कोई निजी कमरा कहाँ होता है जहाँ दूसरों को बुलाकर हुलस-हुलस कर दिखाएँ। जहाँ किसी को ढंग से बैठाने की जगह ही न हो वहाँ बाहर ही मिलना सुविधाजनक होता है।