पुल पार करने से
पुल पार होता है
नदी पार नहीं होती
नदी पार नहीं होती नदी में धँसे बिना
नदी में धँसे बिना
पुल का अर्थ भी समझ में नहीं आता
नदी में धँसे बिना
पुल पार करने से
पुल पार नहीं होता
सिर्फ़ लोहा-लंगड़ पार होता है
कुछ भी नहीं होता पार
नदी में धँसे बिना
न पुल पार होता है
न नदी पार होती है।
वरिष्ठ कवि नरेश सक्सेना की ऊपर उद्धृत कविता पर कुछ महीने पूर्व कवियों और कविता समीक्षक विद्वानों की आभासी दुनिया में कुछ विवाद हुए थे। विवाद का कारण क्या था, मुझे ठीक-ठीक याद नहीं, न हीं इस आलेख का यह उद्देश्य ही है। यहाँ इस कविता को उद्धृत करने का संदर्भ इतना भर है कि स्मृतियों में दर्ज कथादेश (अक्टूबर 2023) में प्रकाशित सीमा आजाद की कहानी ‘मॉर्निंग वॉक’ को लगभग दो वर्षों बाद पुनः पुनः पढ़ते हुए इस कविता की याद लगातार आती रही। किसी रचना को पढ़ते हुए किसी दूसरी रचना की याद हो आना यूं तो सामान्य सी बात है। पर यह सामान्य सी बात तब खास हो जाती है, जब इस क्रम में पाठकों के लिए दोनों ही रचनाओं के निहितार्थों को समझने की कई पारस्परिक अर्गलाएं स्वतः ही खुलने लगती हैं।
सीमा आजाद की इस कहानी में सुबह की सैर के दौरान मीना और श्याम सुंदर नामक पैंसठ वर्षीय एकाकी स्त्री-पुरुष मिला करते हैं। मॉर्निंग वॉक के दौरान हुई उनकी बातचीत के बहाने स्त्री-पुरुष जीवन के अंतरालों के बीच जिस तरह एक पुल का निर्माण होता है, वही यहाँ एक संवेदनशील कहानी की तरह मूर्त हुआ है। शुरुआत में इस कहानी को पढ़ते हुए हंस (जून 2014) में प्रकाशित वरिष्ठ कथाकार और स्त्रीवादी ऐक्टिविस्ट सुधा अरोड़ा की यादगार कहानी ‘उधड़ा हुआ सवेटर’ की स्मृति हो आती है। उस कहानी में भी किसी पार्क में इसी उम्र के एक स्त्री पुरुष सुबह की सैर के दौरान मिला करते हैं। उनके बीच संवाद और आत्मीयता वहाँ भी है। लेकिन कुछ ही आगे बढ़ने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि लगभग एक जैसी शुरुआत और कथा स्थितियों की किंचित समानताओं के बावजूद यह एक सर्वथा अलग कहानी है। ‘उधड़ा हुआ स्वेटर’ के स्त्री पुरुष जहाँ एक दूसरे के माध्यम से, अपने जीवन में उग आई रिक्तियों की पूर्ति के संवेदनापरक अनुभूतियों को जीने लगते हैं, वहीं ‘मॉर्निंग वॉक’ की मीना और श्यामसुंदर ‘पारस्परिकता सह स्वतंत्रता’ की जरूरत को समझते-समझाते, लैंगिक आग्रहों और अंतरालों की स्वतःस्फूर्त पिघलन के वाहक और गवाह बन जाते हैं।
आजीवन अनाम रह जाने की शास्वत स्त्री पीड़ा के बोध के साथ शुरू हुई इस कहानी में आप जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं, भारतीय स्त्रियों के वे तमाम दुख, जिन्हें सहज ही उनके जीवन का हिस्सा मान कर स्त्रियों का ‘महिमामंडन’ किया जाता रहा है, विडंबना के धागों की रील की तरह खुलने लगते हैं। श्याम सुंदर और मीना जी के संवाद का एक टुकड़ा देखिए-
“पत्नी थी तो घर में दिन भर आवाज ही आवाज रहती थी, कभी पड़ोसी महिला की, कभी सब्जी वाले की, कभी काम वाले की, कभी उसकी और…मेरी भी…मैं उसे किसी न किसी बात पर टोकता रहता था।”
श्याम सुंदर जी मीना जी की ओर देखकर फिर हँसे। लेकिन मीना जी के लिए ये हँसी की बात नहीं थी। ये देखकर उन्होंने बात पूरी की-
“अब एकदम सन्नाटा रहता है।”
मीना जी अचानक बोल पड़ीं-
“मुझे तो पहले वाली टोका-टोकी से अब का सन्नाटा अच्छा लगता है।”
अपने कहे पर श्याम सुंदर की असहजता को भाँपते हुए मीना आगे कहती है –
“एक उम्र के बाद इंसान के लिए सुकून जरूरी होता है, चाहे वह कोई भी हो… पूरा जीवन सबके पीछे दीदते-दौड़ते थकान हो गई थी, जरा भी सुकून नहीं था।”
गौरतलब है कि लगभग प्रतिपक्षियों की तरह संवाद करने के बाद मॉर्निंग वॉक से लौटते हुए दोनों ही मानसिक रूप से बेचैन हैं। मीना जी के ‘सुकून’ की बात श्याम सुंदर को गहरे परेशान कर देती है-
“क्या औरतें पति की मौत के बाद अकेलापन नहीं महसूस करतीं? क्या उनकी पत्नी भी सुकून की खोज में थी? जो मेरे मरने पर उसे मिलता? ”
ऐसा सोचते हुए श्याम सुंदर मन ही मन यह फैसला कर लेता है कि कल से वह मीना से बात नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ-
“आगे बढ़ते हुए मीना जी की इच्छा हुई कि काश कि वे पहले मर गयी होतीं और उनके पति को भी उनके बगैर ऐसे ही सन्नाटा लगता तो कितना अच्छा रहता, तब मेरी कीमत समझ में आती…”
श्याम सुंदर ने जहाँ पत्नी के जीते जी उसकी उपेक्षा की वहीं मीना अपने पति द्वारा उपेक्षित रही। इसलिए प्रत्यक्ष संवाद हो कि उसके बाद की मानसिक प्रतिक्रिया, मीना और श्याम सुंदर का प्रतिपक्षियों की तरह परस्पर सम्मुख होना स्वाभाविक है। कहानी में यदि यदि इतना भर भर ही होता तो यह स्त्री विमर्श की सतही समझ की कहानी भर होकर रह जाती। पर यह कहानी उस मुकाम पर नहीं ठहरती, बल्कि ऐसे ही छोटे-छोटे प्रसंगों (यथा- पूरे परिवार केलिए भोजन तैयार करनेवाली स्त्री का स्वयं के लिए खाना न बनाना, सोने जागने जैसी छोटी-छोटी बात पर भी सास-ननद की चौकसनिगाही आदि) पर उपजी स्वाभाविक प्रतिगामी प्रतिक्रियाओं और उसके बहाने स्मृतियों के आलोक में उसके व्यवहार की समीक्षाओं के साथ श्याम सुंदर के भीतर अफसोस और अपराधबोध का भाव उत्पन्न करते हुए एक-एक कदम आगे बढ़ती है। पहली बार ‘सुकून’ के बारे में स्त्री का पक्ष सुनने के बाद, अतीत की किसी दोपहर समय से पहले ही दफ्तर से वापस आने पर झुंझलाहट के बावजूद पत्नी के सेवा भाव को याद करते हुए श्याम सुंदर सोचता है-
“आज श्याम सुंदर जी ने इस घटना को नए तरीके से देखा। उनके जाने के बाद सारा काम निपटाकर पत्नी थोड़ी देर को नींद लेती होगी, उसी समय मैं पहुँच गया, इसलिए उसे झुंझलाहट हुई होगी, इस तरीके से सोचते हुए आज उनके दिमाग में आया कि मुझे उसकी नींद देखकर कह देना चाहिए था कि ‘जाओ सो जाओ’ मैं पानी-चाय सब ले लूँगा, आखिर शादी से पहले आकर सारा काम खुद करता ही तो था न। लेकिन नींद…अचानक उनके दिमाग में मीना जी का बोला गया शब्द ‘सुकून’ याद आ गया, हाँ, ‘सुकून’। उसके थोड़ी देर के ‘सुकून’ में खलल तो नहीं पड़ता। ऐसे न जाने कितनी बार मैंने उसके छोटे-छोटे सुकून को छीना है।
उन्हें लगा काश वे इस घटना को दोहरा पाते, तो इसे ठीक कर लेते। वे तड़प उठे।”
किसी स्त्री के आब्ज़र्वैशन पर, अपनी स्मृतियों के माध्यम से किसी पुरुष द्वारा अपने व्यक्तित्व का यह सेल्फ ऑडिट इस कहानी को स्त्री विमर्श पर केंद्रित कहानियों से अलग ला खड़ा करता है। इस क्रम में ‘सुकून’ और ‘सन्नाटा’ जैसे शब्दों का जो लैंगिक अर्थ प्रकट होता है, वह भी इस कहानी के हासिलों में से एक है।

कहने की जरूरत नहीं कि अपने कथ्य पर सतत केंद्रित यह कहानी अपनी निर्मिति में एक खास तरह के सायासपान से लैस है, जो इसके गढ़े होने का अनुमोदन भी करता दिखता है। बहुत संभव है यथार्थ के आग्रही कुछ पाठकों और समीक्षकों को यह सायासपन कुछ हद तक अविश्वसनीय भी लगे। कुछ लोग मीना के तटस्थताबोध में संवेदना की पारंपरिक नमी का अभाव भी देख सकते हैं। लेकिन मेरा आग्रह है कि इस कहानी को यथार्थ के बजाय स्वप्न की तरह देखा, पढ़ा और समझा जाना चाहिए। हमारा समाज अभी इस हद तक स्त्री संवेदी नहीं हुआ है, पर यह कहानी संवाद, स्मृति और आत्मसमीक्षा के त्रिकोणीय शिल्प में एक स्त्री संवेदी समाज का जो स्वप्न प्रस्तावित करती है, उसके लिए यह सायासपन और तटस्थता दोनों ही जरूरी है। इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि मीना ने जीते जी अपने पति से कोई शिकायत नहीं की। इसे पितृसत्तात्मक मूल्यों के साथ अनुकूलन कहें या जीवन जगत की अनकही विवशता, वह जीवन भर अपनी खीज, अकुलाहट और गुस्से को चुपचाप पीती रही। उसका सारा प्रतिरोध पति की मृत्यु के बाद प्रकट होता है। उसी तरह श्याम सुंदर को अपनी पत्नी के जीते जी उसके प्रति वह संवेदना कभी नहीं जागी, जिसका अहसास उसकी अनुपस्थिति में मीना के तंजिया संवाद सुनने के बाद उसे होता है। मतलब यह कि ‘ऑडिट’ और ‘इमोशनल इनवॉलमेंट’ एक साथ नहीं संभव है। ऑडिट की चुनौतियाँ तब और गहरी और बड़ी हो जाती हैं जब ‘ऑडिटर’ और ‘ऑडिटी’ दोनों एक ही व्यक्ति हो। इस तरह देखें तो श्याम सुंदर के बहाने प्रत्ययक्षतः पुरुष मनोवृत्तियों की ऑडिट की तरह दिखती यह कहानी अपनी आंतरिक संरचना में मीना के बहाने स्त्री मन की स्वीकृति के साहस और समीक्षा की भी कहानी है, जिसके बिना ‘सुकून’ और ‘सन्नाटा’ जैसे शब्दों की यह लैंगिक अभिव्यंजना संभव नहीं हो सकती थी।
एकतरफा सम्बोधन को ही सम्प्रेषण मान लेने की ठसक न सिर्फ सम्प्रेषणहीनता या सम्प्रेषण अंतराल को जन्म देती है, बल्कि इससे हमारा व्यक्तित्व एक खास तरह के सामाजिक, पारिवारिक और आत्मिक अपरिचय तथा आत्ममुग्धता का शिकार भी हो जाता है। श्याम सुंदर अपनी पत्नी के संदर्भ में मीना जी के कथन ‘बड़ी अच्छी थी…उनका चेहरा देखकर अच्छा लगता था, हमेशा मुस्कुराती रहती थीं’ के आलोक में पत्नी की तस्वीरें निकालकर देखता है-
“आज इन तस्वीरों को देखते हुए उन्हें लगा कि उनके बच्चे उनसे मिले गोरे रंग के कारण नहीं, माँ से मिले चेहरे के कारण सुंदर दिखते हैं।”
पत्नी के जीते जी सिर्फ उसके साँवले रंग को देखनेवाले श्याम सुंदर के मन में उठने वाली इस टीस में ‘बच्चे मेरे रंग पर गए हैं, तुम्हारे पर नहीं’ की आत्ममुग्धता का अफसोस और पत्नी की कायिक उपस्थिति से भी उसके जीवन पर्यंत अपरिचय का उद्घाटन दोनों ही शामिल है।
पितृसत्ता ने स्त्री-पुरुष के बीच घर और बाहर के कार्यक्षेत्र की एक मजबूत विभाजक रेखा खींच रखी है। यही कारण है कि स्त्रियाँ भावनाओं के मामले में जितनी आत्मनिर्भर होती हैं, घर के बाहर के कामों के मामले में उतनी ही पर-निर्भर। बाजार से सब्जी लाने या टेलर के पास जाने का काम हो या फिर हाउस हेल्प की गैरहाजिरी में भोजन तैयार करना, जीवनसाथी की मृत्य के बाद कार्य विभाजन का यह पितृसत्ताक फार्मूला किसी त्रासदी की तरह सतह पर फैल जाता है। तंज या शिकायत के शिल्प में मीना जी जो कुछ श्याम सुंदर से कहती हैं, उसमें कार्य विभाजन की उस प्रविधि का प्रतिरोध और अस्वीकार तो है ही, उसके आलोक में श्याम सुंदर का हलवा बनाना सीखना और मीन का खुद बैंक जाकर पासबुक अपडेट करवाना, उस विभाजन के परिमार्जन की तरफ बढ़ा कदम है। इस तरह स्त्री सरोकारों की यह कथा स्त्री पक्ष के उद्घाटन के कारण नहीं, पुरुष पक्ष की आत्मसमीक्षा के कारण ज्यादा महत्त्वपूर्ण बन पड़ी है।
इस आलेख की शुरुआत मैंने नदी और पुल के संदर्भ से की थी। नदी और पुल का एक रूपक इस कहानी में भी आद्योपांत उपस्थित है, जिसके गहरे निहितार्थों पर चर्चा किए बिना यह टिप्पणी अधूरी होगी। जैसा कि यह स्पष्ट ही है कि कहानी के दोनों चरित्रों की मुलाकात मॉर्निंग वॉक के दौरान होती है। इस क्रम में वे अमूमन कर्जन पुल शुरू होने के पहले बनी एक सीमेंटेड बेंच के पास मिलते और सुस्ताते हैं। कहानी में इस बात का एकाधिक बार उल्लेख है कि मीना जहाँ सैर के दौरान उस पुल के पार जाया करती है, वहीं श्याम सुंदर आधे पुल से ही वापस आ जाते हैं। कहानी के अंतिम दृश्य में जब एक सुबह टहलते हुए वे दोनों क्रमशः हलवा बनाने और पासबुक प्रिन्ट कराने की बात साझा कर रहे होते है, उस दिन पहली बार श्याम सुंदर मीना के साथ बात करते हुए पुल पार कर जाते हैं। उल्लेखनीय है कि जबतक स्त्री-पुरुष के बीच लैंगिक आधार पर कार्य विभाजन की रेखा धुंधली नहीं हुई थी, मीना अकेले ही पुल पार करती रही, लेकिन जैसे ही इस रेखा के मिटाने का प्रयास हुआ, दोनों ही साथ-साथ पुल पार कर गए। पुल जबतक पार न किए जाएं, उनकी भूमिका विभाजक की होती है। पुल संयोजक की तरह तभी पहचाने जाते हैं, जब उन्हें पार किया जाय। विभाजन की नीयत और नियति का प्रतिकार किए बिना कोई पुल भला कैसे पार किया जा सकता है? इस संदर्भ में साथ-साथ पुल पार करते हुए श्याम सुंदर और मीना के बीच हुई बातचीत को गौर से सुना जाना चाहिए –
“अगर शादी से पहले मेरी किसी लड़की से दोस्ती हुई होती तो मेरी शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी होती… माने मैं भी अपनी पत्नी को थोड़ा सुख दे पाता।
मीना जी हँसने लगीं और हँसते-हँसते कहा-
“मेरी शादी के पहले अगर मुझे ये पता चल गया होता कि कुछ आदमी समझदार भी होते हैं, तो मैं शादी ठोंक-पीट कर करती।”
‘हलवा बनाने’ और ‘पासबुक प्रिन्ट कराने’ की पृष्ठभूमि में श्याम सुंदर और मीना के उपर्युक्त संवाद एक खूबसूरत दुनिया के स्वप्न की सम्मोहक प्रस्तावना हैं। यद्यपि ‘मॉर्निंग वॉक’ में सबेरा यानी शुरुआत की व्यंजना निहित है। बावजूद इसके सोचता हूँ, इस कहानी का शीर्षक ‘मॉर्निंग वॉक’ के बजाय ‘पुल’ होता तो कैसा रहता? और यह कहते हुए बचपन में पढ़ी महीप सिंह की प्रसिद्ध कहानी का शीर्षक भी मन-मस्तिष्क में कहीं कौंध रहा है- ‘पानी और पुल’। वह कहानी भारत-पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठ भूमि में लिखी गई थी। सीमा आजाद इस कहानी में जिस विभाजन की बात करती हैं, वह भी कम भयावह नहीं है। अच्छा है कि सीमा इस कहानी में उस विभाजन को पाटने के लिए एक पुल भी प्रस्तावित करती हैं। इस कहानी की आत्मा विभजान में नहीं, उसी पुल में बसती है।


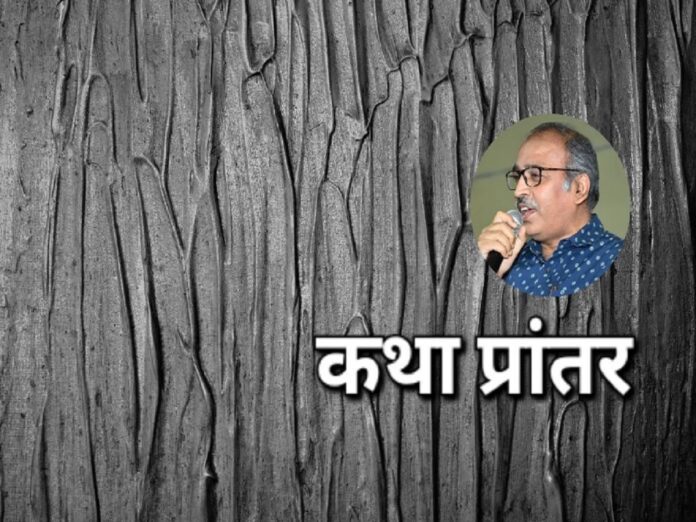
कहानी की समीक्षा की खूबी कि समाज के अंधेरों मे रोशनदार की तरह खुलती है कहानी.परत दर परत खोलते हुए कहानी के मर्म तक पहुंचती समीक्षा.
आदरणीय श्री राकेश बिहारी जी,
नमस्कार,
सीमा आज़ाद की कहानी “मॉर्निंग वॉक” पर लिखी आपकी आलोचना पढ़ी, बहुत अच्छी लगी। कहानी तो मैंने नहीं पढ़ी है, पर समीक्षा पढ़कर इसे पढ़ने की इच्छा जग गई।
आलोचक का काम रचना और पाठक के बीच पुल बनाना है और इसमें आप पूरी तरह से सफल रहे हैं। आपने समालोचन ब्लॉग पर भी कई कहानियों की आलोचना लिखी है। मैंने उनमें से अधिकांश लेख पढ़ रखा है। वे भी बहुत अच्छी हैं। आपके लेखों को पढ़कर कहानी पढ़ने की इच्छा जग जाती है। इन लेखों को पढ़कर कहानी पर आलोचना कैसे लिखी जाए, यह सिखा जा सकता है।
इतनी अच्छी आलोचना लिखने के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। आप ऐसे ही लिखते रहे।।आपको साधुवाद।
——— प्रमोद कुमार बर्णवाल
बहुत शुक्रिया!
बहुत खूब! लेकिन ऑडिट और emotional involvement साथ होता है. न कर पाना emotional limitation है. ये उम्दा दिखाया है कथाकार ने. पत्नी इसलिए याद आ रही क्योंकि वह उसके अनुसार चला करती थी. लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या स्त्री के इस पक्ष को लेकर पहले कहानियां नहीं लिखी गई हैं? मुझे लगता है कि मैं ने पढ़ी है
राकेश जी की विश्लेषण पद्धति द्वाद्वात्मक है जिसके तहत वे रचना को दोनों सिरों से स्पर्श करने में सक्षम होते हैं.
कहानी का शीर्षक पुल ज़्यादा समीचीन प्रतीत होता haim
आभार!
बहुत अच्छी समीक्षा. एक-दूसरे के संदर्भ में अपने-अपने अभाव देखने की बजाय अपने-अपने व्यवहार को जांचने और स्पाउज़ की प्रतिक्रियात्मक आकांक्षा को समझने की परिपक्वता का जो कोण आपने कहानी की ताकत के रूप में उभारा है, दरअसल वही कहानी के संवेदनात्मक मर्म की शिनाख्त है। यहीं आलोचक पाठ-प्रक्रिया में महज पाठक नहीं रहता, सह-सर्जक बन जाता है।