बी. सरोजा देवी और राजेंद्र कुमार अभिनीत पुरानी वाली ससुराल फिल्म का एक गीत, कहें तो गीत भी नहीं एक कव्वाली है- ‘इक सवाल मैं करूं, इक सवाल तुम करो, हर सवाल का जबाब, इक सवाल हो!’ कव्वालियों की एक पुरखलूस परंपरा रही है, हमारी फिल्मी दुनिया में पर सवालों के प्रत्युत्तर में भी कोई एक कोई सवाल ही हो, यह कमाल सिर्फ साहिर लुधियानवी ही रच सकते थे। इसी गीत की कुछ पंक्तियां है-
सवाल- ‘ प्यार की बेला, साथ सजन का, फिर क्यूं मन घबड़ाये?
नैहर से घर जाती गोरी, क्यूं नैना छलकायें?
जबाब – है मालूम कि जाना होगा, दुनिया एक सराय,
फिर क्यूं जाते वक्त मुसाफ़िर, रोये और रुलाये?’
मैंने भी हर बार अपने मन से यही कहा है- है मालूम कि जाना होगा, दुनिया एक सराय, फिर क्यूं जाते वक्त मुसाफ़िर, रोते और रुलाये? पर मन है कि फिर भी नहीं मानता, बिसूरता है और बिसूरता ही जाता है। इसे कोई ज्ञान, कोई दर्शन नहीं बहला सकता। यानी जगह बदलना, या फिर किसी जगह को पीछे छोड़ देना, मेरे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। लाग-लगाव के सारे सिरे मन से उलझे उलझे जाते हैं, मोह की ये डोर चाहे होती भले रेशमी हो पर बांधती है मन को बड़े कस-बल के साथ। हर पड़ाव, हर छूटी जगह, दिल में किसी स्थान, शहर याकि पड़ाव से कहीं ज्यादा; किसी नासूर की तरह जगह घेरे रहती है।
बहुतों के साथ ऐसा ही होता होगा और बहुतों के साथ नहीं भी, कि बहुत सारे लोग जिंदगी की लय में बहना और उसके साथ कदमताल करते चलना जानते हैं। पर मेरे लिए ऐसा ही है। छोड़ देना या छूट जाना, जिंदगी का चाहे एक महत् हिस्सा हो; पर मेरे लिए सबसे मुश्किल है, यह काम। फिर छूटी चीजें अटकी रहती हैं, कसकती रहती हैं बहुत भीतर तक। एक मरोड़ की तरह उठती हैं यादों की कोई हूल।
जानती हूं कि जो कुछ छूट गया सो फिर छूट ही गया। इसे फिर अब जीवन में लौटकर नहीं आना। और ठीक इस तरह तो बिलकुल नहीं आना। ‘फिर आयेंगे’ या ‘फिर आना होगा न!’ की तसल्ली मुझे कोई तसल्ली नहीं बख्शती तो बस इसी वजह से।
इलाहाबाद जब शिफ्ट हुई तब पहले से तय था कि यह रहना टेम्पररी है, इस जगह से दिल तो बिलकुल नहीं लगाना। इसे बंजारों के एक पड़ाव की तरह बरतना होगा और हंसते-हंसते छोड़कर निकल जाना। हालांकि पिछले पड़ाव यानी कांटी (मुजफ्पफरपुर) में अटका हुआ मन, अब भी उसके लिए किसी बिसूरते हुते बच्चे जैसा था। तो लगता तो यही था, यह कुछ मुश्किल नहीं होगा। जब पहले से पता हो…
लेकिन सिविल लाइंस, हाट-बाजार, कटरा, साहित्यिक गोष्ठियां; संगम और वहां की सुबह-शामों ने दिल में घर कर लिया और कब कर लिया यह जान ही न पाई। और जब जाना तो देर हो चुकी थी बहुत..
जिंदगी में कुछ भी तो ठीक वैसा नहीं होता जैसा कि हम सोचते या फिर तय करके रखते हैं। मनाही करो तो दिल और जल्दी स्वीकार लेता है, अपना लेता है, अपना बना लेता है।
अब जाना था और फिर-फिर नहीं लौटकर आना था। उस तरह और उस जगह तो कदापि नहीं। फिर भी मन अपने जिद की पतंग जोर से पकड़े अड़ा था कि इसे यूं तो नहीं ही छोड़ना, आजाद भी नहीं होने देना। एक बार छोड़ दिया या छूट गया तो बस…
चंद घंटों से भी कम की उस यात्रा में इतना रोई, इतना रोई, जितना शायद पहले कभी रोई होऊंगी। किसी भी नयी जगह जब हम जाते हैं तो थोड़ा सा उस पुरानी जगह को साथ ले जाते हैं। इससे थोड़ी कसक कम हो जाती है, थोड़ी सी वह जगह बनी रहती है, सदा-सर्वदा हमारे बीच। ‘रंजे-सफ़र की कोई निशानी तो पास हो, थोड़ी सी ख़ाके-कूच-ए-दिलबर ही ले चलें।’ छोड़ दिये जाने और छूट जाने को नियत उस घर में जो सबसे महत्वपूर्ण थे, वो थे गमले और पेड़ पौधे। सामान बांध चुकने के बाद जब ट्रांसपोर्ट वाले ने पेड़ पौधों के लिए हाथ खड़े कर दिये, तब ‘वे’ भी उनके साथ सर्व-सम्मति से शामिल थे। यह साजिश लगी थी मुझे, घोर साजिश… अल्पमत की इस सरकार को आखिरकार गिर ही जाना था, पर मेरा मन इस बात को मानने को बिलकुल तैयार नहीं था कि दो-दो गाड़ियों में इन पौधों के लिए जगह नहीं थी। जो पौधे दो महीने अकेले कांटी में बिताने के बावजूद, इलाहाबाद तक की लम्बी दूरी तय कर पायें, वो 55 किमी. की यह छोटी सी दूरी…
यह भी पहली बार हुआ कि मेरे पॉटरी वाले सारे वाजेज, अलग-अलग आकार वाले गमले और तिपाइयां-चौपाइयां सब रस्ते में टूट फूट लीं। मैं लाख कोसती रही मुंये ट्रांसपोर्ट वालों को, पर अब क्या होना था?
इलाहाबाद को मुझसे छूटना था और पूरी तरह से छूटना था।
गोकि इलाहाबाद अब भी अक्सर जाती हूं और बार- बार जाती हूं। पर उस घर की तरफ जाते रस्तों को देखकर इक हूक जरूर उठती है। बतर्जे इस शेर- ‘उस शहर को यूं देख के क्यूं हूक उठे है, उस शहर में तो कोई भी अपना नहीं रहता।’ मैं भी यह जानते हुये भी कि उस गली में तो कोई भी अपना नहीं रहता, जो भी साथ या आसपास हुआ उससे यह जरूर कहती हूं-‘हमलोग पहले यहीं तो रहते थे, अभी… महीने पहले तो बस जाना हुआ…
कई बार ऐसे में खुद को दिलासा देती हूं। चीजें ही तो थीं…उनका सोचो जिनको…
ऐसे में इस कल्पना मात्र से ही सिहरन होती है कि कैसा महसूस होता होगा जब किसी दैवी या मानवीय अथवा अमानवीय आपदा के कारण उस ज़मीन के टुकड़े से सारे नाते-रिश्ते तोड़ने पड़ते होंगे, एक अनिश्चित अवधि के लिए, या शायद सदा-सर्वदा के लिए, जो हमारी जिंदगी रहे हों कभी? उस दर्द, टूट, कसक को वही जान सकता है, जिसे उससे गुज़रना पड़ा हो। यह पीड़ा कुछ ऐसी ही है, जैसे किसी दूध पीते बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया जाए! छीन ली जाये उससे उसकी दूध-पिलाई भी।
किसी विदेशी कवयित्री की कविता का भावार्थ है- ‘ट्रेन सरहद से होकर गुज़र रही है, राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के दरम्याँ चलती गाड़ी में एक शिशु जन्मता है। माँ को खुशी है उसे दर्द से मुक्ति मिलती है। एक नये नागरिक का जन्म होता है। लेकिन कवयित्री की जिज्ञासा है कि दो देशों के बीच काँटेदार बाड़ को पार करती हुई मुल्कों की चेक पोस्टों की निगाहों के बीच भागती ट्रेन में जनमें शिशु की नागरिकता आखिर क्या होगी?
देश और नागरिकता बहुत मायने रखते हैं, जीवन में। कोई भी व्यक्ति, जहाँ, वह अपने परिवार और समाज के साथ रहता है, उसके लिए वह मात्र ज़मीन का टुकड़ा भर नहीं होता है, वह उसकी पहचान का हिस्सा होता है। उस टुकड़े का जुड़ाव उसके सम्पूर्ण अस्तित्व के साथ होता है। ज़मीन के उस टुकड़े को हम गाँव, मुहल्ला, कस्बा या और कोई भी कोई नाम दे सकते हैं। और यही टुकड़ा इलाके, ज़िले, प्रान्त या देश के स्तर पर उसकी बृहत्तर पहचान भी तय करता है।
इस पहचान को भी हम विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग नाम देते हैं, भाषा के आधार पर, प्रांत के स्तर पर… जैसे अवधिया, भोजपुरिया, तमिल, गुजराती, पाकिस्तानी, चीनी, अमरीकी, रूसी या और कुछ। ज़मीन के उसी टुकड़े से उसका एशियाई, अफ्रीकी या योरोपियन होना भी तय होता है।
ज़मीन का वह टुकड़ा क्षेत्रीय पहचान भर नहीं है। मानव सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न तत्त्व भी उसी ज़मीन के टुकड़े की सोंधी मिट्टी में पनपते हैं। जैसे- रीति-रिवाज़, खान-पान, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कलाएँ, भवन निर्माण, शैली, वेश-भूषा, तीज-त्यौहार, इत्यादि। जमीन का वह टुकड़ा न केवल हमें बसाता है, बल्कि वह स्वयं भी हमारे अन्दर पहुँच कर बस जाता है, किसी विशाल वट वृक्ष के फैलाव और गहराई के साथ।
यूं कहें तो वर्तमान समय में विश्व की आधी आबादी बेघर है और अपनी ज़मीन छोड़कर दूसरे राज्य या मुल्क में जहाँ लोगों की भाषा, धर्म या संस्कृति अलग है, विस्थापितों का सा जीवन जी रही है। बेघरी का आलम यूं हुआ पड़ा है कि लोगों को रोजी-रोटी के निमित्त अपना मुल्क छोड़कर दीगर मुल्कों में बसना पड़ता है और वहाँ की विपदाओं को सहना पड़ता है। यह एक दूसरे स्तर का विस्थापन है।
शरणार्थी होने और बस जाने के दरम्यान हर युग में एक लम्बा फासला हुआ करता है, और यह फासला कभी भी आसानी से नहीं कटता। कोई नहीं जानता कि गर एक बार उजड़े तो फिर कब और कहाँ शरण मिलेगी? वही जमीन और वो आस्मां कभी मिलेगा भी कि नहीं…शायद इसीलिए बचपन या फिर जवानी के दिनों में अपनी जगह से अथाह नफरत करनेवालों को भी उम्र के एक पड़ाव पर उसके लिए उदास होते, बोझिल होते हुते देखा है। नॉस्टेलजिया शायद इसे ही कहते हैं।
इस तरह कई जगहें, कई शहर, कई लोग ऐसे होते हैं, जिनके पास से जाकर भी हम कहीं नहीं जाते। अंठियाये हुये पड़े रहते हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द-गिर्द, उन्हीं के आसपास… अपने हिस्से के उन जगहों, शहरों और इंसानों को हम समेटे रहते हैं अपने भीतर। अच्छी तरह सहेजे हुये भी…
हर इंसान के दिल में कोई ऐसी जगह या कुछ ऐसी जगहें होती जरूर हैं। किसी की दिल्ली, किसी का कानपुर, किसी का बनारस, किसी का इलाहाबाद… किसी का सीवान, तो किसी का छत्तीसगढ़। किसी का नार्वे, तो किसी का इंग्लैंड …किसी का कुछ तो किसी का कोई… जिस तरह प्रिय होने का कोई तर्कशास्त्र नहीं होता, अप्रिय होने का भी नहीं होता है।
कई बार पुरानी जगहों पर चाहकर और योजनाएं बनाकर भी जाने का वक्त नहीं होता। ऐसे लम्हों में मन बार-बार अज्ञेय के यायावर की तरह दिलासा देता है- ‘दिया मन को दिलासा, पुनः: आऊंगा/ भले ही दिन, बरस, अनगिन, युगों के बाद…’ पर न वे युग लौटते हैं, न वे दिन… जगहें भी जैसे अपनी धूरी से खिसककर कोई और हुई जाती हैं, और… और… और…
मैं अपनी कहूं तो मेरे लिए वो जगहें हैं- मेरा गांव चैनपुर, गोरखपुर, फिर मुजफ्फरपुर, और फिर दिल्ली… ये जगहें ठीक वही हैं, जिनका जिक्र सुन बांछे खिल जाती हैं, आंखें या तो चमक उठती हैं, या झिलमिल हुई जाती हैं।
कुछ भी वहां न बचा रहने और पट्टीदारों के द्वारा हड़प लिये जाने के बावजूद और रोज-ब-रोज उसे सपने में देखने के बाद एक बार चैनपुर गयी। उस वीरानी सी वीरानी को देखकर बिलकुल वह घर याद नहीं आया, न उसके होने का कोई एहतराम ही। बस सपने में रोज-ब-रोज और बार-बार उसका रसा-बसा रूप जरूर आना बंद हो गया। एक बार गोरखपुर गयी तो तो उसमें पुराने शहर का नक्श तलाशती रही। जबकि वो कहीं नहीं मिला और मैं निराश हो उठी। दिल्ली जाकर अभी भी बांछे खिलती हैं, पर कई बार यह भी लगता है, अच्छा ही है कि नहीं जा सकी यहां के अपने पुराने ठीयों पर, उसके आसपास। वर्ना उन पुरानी जगहों को खस्ताहाल या दूसरे हाल में देख मेरे मन के भीतर का वह हिस्सा भी मर जाता। वो सुंदर स्मृतियां नष्ट हो जातीं। उन्हें नष्ट होना ही होता…जोकि मैं बिलकुल नहीं चाहती। रश्मि भारद्वाज की एक कविता का अंश है-
उस जगह कोई नहीं पहचानता मुझे
बैठी हुई हूँ
उस जगह।
उस जगह को याद करती हुई
अब मेरी आँख भरती तक नहीं
साँस भारी हो चलती है मगर
जहाँ होती हूँ वहाँ कम होती हूँ
जहाँ होती हूँ वहाँ नहीं, जाने कहाँ- कहाँ होती हूँ
मैं खोजती हूँ एक जाना-पहचाना चेहरा…
साथ चलता कोई दुलार कर देखता नहीं मुझे,
रिक्शा वाला भी बैठते संग बता देता है
कि ‘दस रुपया लगेगा!’
तो कह देती हूँ “ठीक है भइया, ठीक है!”
“अब इस जगह से ले तो चलो…!”
जो ठीक इसी मनःस्थिति को बयान करती है और उदास कर जाती है…
वैसे शरणार्थी कौन नहीं है और कहाँ नहीं हैं? किससे अपना घर नहीं छूटा। पर औरतों से बड़ा शरणार्थी कौन होगा?
आज भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण,.बर्बरता और कट्टरता के कारण और सबसे बढ़कर युद्धों के कारण न जाने कितने लोग बेघर होते हैं। अभी भी हो रहे। कितनों को अपनी सरजमीं छोड़नी पड़ी। हमारी सभ्यता का इतिहास अनवरत युद्धों का इतिहास है। रक्तरंजित। त्रासद। युद्ध एक विभीषिका है और विभीषिका की परिणाति है – बेघर और बेदर होना। शरणार्थी होना।
जबकि यह दिल दुआ करता है और लगातार करता है- विस्थापन किसी के हिस्से न हो, बिछड़ने का दर्द किसी के पास न आये। किसी को किसी भी मजबूरी या बेचारगी में नहीं छोड़नी पड़े अपनी सरजमीं, अपना मिट्टी-पानी।
एक असंभव की प्रार्थना में मेरे हाथ बार-बार उठते हैं। और मेरा ही मन कहता है- ‘आमीन!’

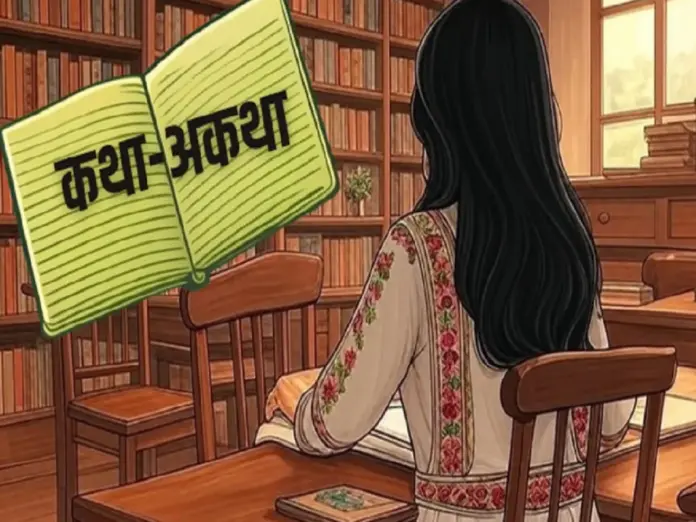
मेरी स्मृतियों में नानी का बहुत अच्छा घर है और मैं बिल्कुल वहाँ जाना नहीं चाहती…जानती हूँ वो घर अब बिल्कुल भी वैसा नहीं होगा…अगर गई तो वो मधुर यादें बिखर जायेंगी।
एक पंक्ति जो दिल को छू गई-“औरतों से बड़ा शरणार्थी कौन होगा”
औरत हूँ, अच्छी तरह समझ सकती हूँ।
शुक्रिया नमिता!