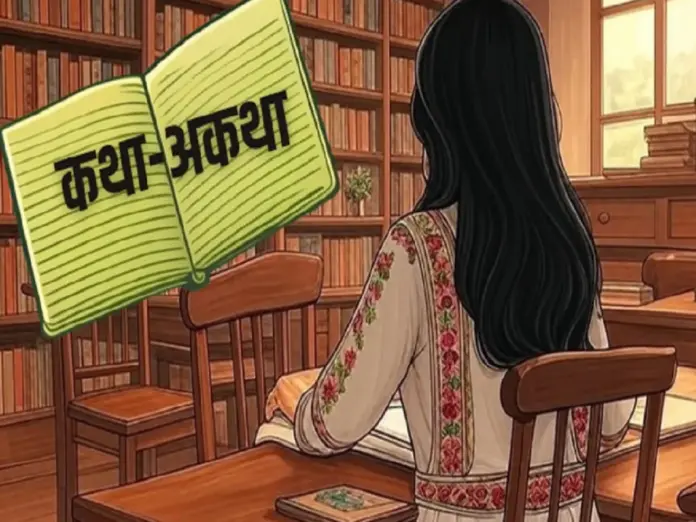विनोद कुमार शुक्ल को मिली तीस लाख की रॉयल्टी ने एक बार फिर हंगामा बरपा रखा है। उनकी रॉयल्टी और श्री शुक्ल इस बार दूसरी दफा चर्चा के केंद्र में हैं। हालांकि मानदेय का मामला एक चिरकालीन और पुरातन मामला है, तबसे जबसे लेखन और प्रकाशन का सह-अस्तित्व शुरू हुआ। लेकिन हाल फिलहाल यह मामला तब प्रकाश में आया, जब 2022 में लेखक और अभिनेता मानव कौल ने सोशल मीडिया पर विनोद कुमार शुक्ल के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट की थी। तस्वीर के साथ उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इतने बड़े लेखक जिनकी दर्जनों किताबें न सिर्फ प्रकाशित हैं बल्कि बेहद लोकप्रिय भी हैं, उन पुस्तकों की रॉयल्टी के तौर पर उन्हें महज कुछ हजार रुपये मिलते हैं।
मानव कौल ने यह भी लिखा था कि – “पिछले एक साल में वाणी प्रकाशन से छपी तीन किताबों का इन्हें 6000 रुपये मात्र मिला है और राजकमल से पूरे साल का 8000 रुपये मात्र। मतलब देश का सबसे बड़ा लेखक साल के 14000 रुपये मात्र ही कमा रहा है। लेखक ने वाणी प्रकाशन को यह लिखित में दिया है कि वे उनकी किताब न छापें…”
वाणी से उनकी तीन किताबें प्रकाशित हैं — ‘दीवार में एक खिड़की रहती थी’, ‘अतिरिक्त नहीं’ aur ‘कविता चयन’। दो किताबों के ईबुक संस्करण भी आये हैं। मई 1996 से लेकर अगस्त 2021, यानी पच्चीस वर्षों में उन्हें वाणी से कुल एक लाख पैंतीस हजार, अर्थात सालाना करीब पाँच हजारकी राशि मिली। जबकि उनकी एक किताब को साहित्य अकादमी सम्मान भी मिला है और अब पेन नोवोकोब भी। यूं भी बेहिसाब हिंदी लेखकों-पाठकों के घरों में यह किताब दिख जायेगी।
नौकर की कमीज के अँग्रेजी अनुवाद के कथित रूप से न बिकने के कारण पल्प कर दिये जाने जैसा पत्र भी विनोद जी के पास आया था, तब रायपुर के अखबारों में इसकी खबर भी छपी थी। पता नहीं किताब बिकी थी भी या नहीं या यह भी रॉयल्टी बचाने की एक योजना भर थी।
लेकिन सबसे त्रासद यह कि वे छह वर्षों तक प्रकाशक को यह लगातार लिखते रहे कि ‘मेरी किताब न छापें’, ‘मेरी अनुमति के बगैर नया संस्करण न छापें क्योंकि प्रूफ की कई गलतियाँ हैं’, ‘मेरा अनुबंध समाप्त कर दें’ — लेकिन कोई सुनवाई नहीं न होनी थी, न हुई ।
इन बुजुर्ग लेखक की पीड़ा को समझने के लिए सितम्बर 2019 के इस खत को पढ़ें- “मैंने आपको स्पीड-पोस्ट तथा ईमेल भेजा था कि बिना मेरी अनुमति के नया संस्करण नहीं निकालें। इस संबंध में मैंने जब तब फोन से भी अनुरोध किया था, लेकिन आपने फिर नया संस्करण निकाल दिया। इसके पूर्व भी जितने संस्करण निकले हैं, उसकी पूर्व-सूचना मुझे कभी नहीं दी गयी। मैं इससे दुखी हूँ।” उनका यह भी कहना था कि प्रकाशकों के साथ ईबुक का अनुबंध नहीं हुआ, लेकिन फिर भी प्रकाशकों ने ईबुक छाप दी। हालांकि प्रकाशक ने यह कहा कि उन्हें ई बुक की रॉयल्टी भी भेजी जाति रही। उन्हें अगर प्रकाशक से कोई शिकायत थी तो मिल बैठकर बात करना चाहिए था, न कि इस तरह सारे-आम इस मुद्दे कों उछाला जाना था।
विनोद कुमार शुक्ल के इस साक्षात्कार के बाद हिन्दी साहित्य के पटल पर यह मामला काफी गर्माया। लेखकों ने ज़्यादातर उनके पक्ष और कुछेक ने विपक्ष में भी बहस शुरू कर दी। लेखकीय रॉयल्टी प्रकरण में विनोद कुमार शुक्ल जी के साथ लगभग समस्त साहित्य जगत एक साथ खड़ा है, ये शुभ संकेत था। मैं भी उनके अर्थात प्रत्येक लेखक और उसके परिश्रम और पारिश्रमिक के अधिकार के पक्ष में साथ हूँ। सोचिए कि प्रेमचंद ने भी खुद को ‘कलम का मजदूर’ कहा, बेगार तो कभी नहीं कहा।
विकुशु के इस साक्षात्कार और तमाम नए-पुराने लेखकों के एकजुट और एकमत होकर लिखने का ही परिणाम था कि प्रकाशकों में थोड़ी सी खलबली मची। जहां से नहीं आती थी या फिर कम आती थी, वहाँ से भी लेखकों को रॉयल्टी और रॉयल्टी स्टेटमेंट आने लगे। चाहे यह राशि बहुत तुच्छ या नगण्य रही हो, पर मामला कुछ हद तक आगे तो बढ़ा ही था।और फिर तीन साल बाद उसीदीवार में खिड़की रही थी’ के लिए उन्हें रॉयल्टी बतौर एक बड़ी धनराशि मिली।
रॉयल्टी को लेकर बहुत विवाद और मुकदमें भी हुए। अगर सभी बड़े लेखकों की रॉयल्टी को लेकर इतिहास लिखा जाये तो पता चलेगा कि उनका कितना शोषण हुआ या किया गया, कितना नहीं।
पता नहीं किस तरह, पर, अमृतलाल नागर, फणीश्वरनाथ रेणु और काका हाथरसी जैसे लेखक-कवि लेखन की रॉयल्टी से ही अपना जीवन गुजार गए। यहाँ तक कि ‘नयी कहानी’ के लेखकों की स्थिति भी इस मामले में अच्छी रही, इनमें से कई ऐसे थे जिन्होंने कोई नौकरी या फिर नियमित नौकरी नहीं की। वे अपनी किताबों और रचनाओं की अग्रिम राशि लेकर तब किताब लिखते और देते रहे। मानदेय के पैसों से खींच-खांच उनका घर भी चलता रहा और इसी के माध्यम से वे लिखने और सैर-सपाटे के लिए पहाड़ों पर भी जाते रहे। हालांकि इसमें से कुछ ऐसे भी लोग थे, जो एक किताब या एक कहानी के लिए कई प्रकाशकों और संपादकों से अग्रिम राशि लेते थे और फिर एक ही रचना के शीर्षक बदलकर या फिर थोड़ी फेर-बादल के साथ उन सबको सौंप देते रहे। यह कोई प्रशंसनीय कार्य भले न रहा हो, या फिर ये अपने लेखक और लेखन से भले ही एक तरह की की जानेवाली बेईमानी हो, पर यह तो तय है कि उस समय तक लेखकों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं तो अच्छी जरूर थी।
विमल कुमार ने रॉयल्टी विवाद के संदर्भ में 1918 में एक पोस्ट लिखकर यह बताया कि उग्र जी को अपनी रचना ‘शराबी’, ‘बधुवा की बेटी’ और’ चार बेचारे’ को पुस्तक के रूप में छपवाने पर इन किताबों की 40 हज़ार रॉयल्टी मिली थी।‘ अगर यह सच है तो हिंदी में सबसे अधिक रॉयल्टी पाने वाले लेखक उग्र ही है। क्या इतनी रॉयल्टी उस ज़माने में प्रेमचंद को भी मिली होगी? शिवपूजन सहाय ने लिखा है कि प्रेमचंद को 1925 में प्रकाशित रंगभूमि पर 1800 रुपए की रॉयल्टी उस जमाने में भी मिली थी। 1918 में सेवासदन कोलकत्ता की ‘ हिंदी पुस्तक एजेंसी’ से छपा था। लेकिन शिवरानी देवी ने अपनी संस्मरणात्मक पुस्तक ‘प्रेमचंद घर में’ में यह लिखा है कि अगर प्रकाशक प्रेमचंद को ईमानदारी से रॉयल्टी देते तो उन्हें आर्थिक संकट नही झेलना पड़ता। सच क्या है अब ये कौन बता सकता है? लेखक जब इस दुनिया में हो ही नहीं। लेकिन यह भी सच है कि मैथिली शरण गुप्त का साकेत उस जमाने मे गोदान से अधिक बिका। यही नहीं, मैथिली शरण गुप्त ने भी अपना प्रकाशन खोला था। ठीक उसी समय में शिवपूजन सहाय की देहाती दुनिया भी आई, पर राजा राधिका रमण ने शिवपूजन जी के 20 हज़ार रुपये की रॉयल्टी उन्हें दी ही नहीं। यह एक लेखक नहीं बल्कि एक प्रकाशक कर रहा था, अपने समकालीन के साथ।
उस ज़माने के बड़े प्रकाशक थे नवल किशोर प्रेस, गंगा पुस्तक माला, खड्ग विलास प्रेस, ज्ञानमंडल, पुस्तक भंडार, भारती भंडार। लेकिन लेखको को प्रकाशकों के शोषण से बचने के लिए तब भी अपना प्रकाशन खोलना पड़ा। प्रेमचंद ने भी प्रकाशन खोला। यशपाल ने विप्लव, जैनेन्द्र ने पूर्वोदय, अश्क जी ने नीलाभ प्रकाशन दिनकर ने उदयाचल प्रकाशन सुमित्रा जी ने युग मंदिर, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह ने अशोक प्रेस। यहाँ तक कि राजेन्द्र यादव ने भी अक्षर प्रकाशन खोला और जिसके घाटे से तंग आकर उन्होंने उसे एक बड़े प्रकाशक को बेच दिया। इससे एक बात तो तय होती है कि लेखकों के वश में लेखन के साथ-साथ प्रकाशन भी चलाना एक दुरूह और दुर्वह कार्य रहा। एक-एक करके इसमें से अधिकतर प्रकाशन बंद हुये। या फिर जो बचे रहे वो लेखक की अपनी किताबों तक ही सीमित होकर रह गये या फिर उनकी ज़िंदगी तक। अश्क का नीलाभ प्रकाशन इसका अपवाद जरूर रहा पर इसमें अश्क जी और कौशल्या जी के हाड़तोड़ मेहनत का बहुत बड़ा हाथ था। उनके पश्चात नीलाभ के रहते हुये और उसके बाद भी यह प्रकाशन उपेक्षित और नाममात्र का होकर रह गया। यहाँ तक कि प्रकाशक बनते ही लेखकों का रवैया अपने समकालीन लेखों के लिए बदल जाता। वे मित्रों का भी शोषण करते रहे, जिसका उदाहरण शिवपूजन सहाय और राजा राधिका रमन के बीच का मानदेय प्रकरण था। राजेन्द्र यादव से जब भी अक्षर प्रकाशन को लेकर बात हुई, वे हमेशा प्रकाशकों के साथ खड़े दिखे, उनके विचार से जब किताबें नहीं बिकती तो लेखक भला क्या करे? यहाँ कई बार उनसे मेरी राय एकदम मुख्तलिफ रही।
वर्तमान में अकेले गौरीनाथ और उनकी अंतिका है जो वर्षों से इस क्षेत्र में डटे हुये हैं। गौरीनाथ कहानीकार हैं और पहले हंस पत्रिका में काम करते थे। पर गौरीनाथ भी इसे चलाते रहने को अपनी विवशता मानते हैं- ‘मेरा अनुभव बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन एक बार शुरू करके बंद कैसे करें।’ हालांकि सोचनेवाला तथ्य यह भी है कि प्रकाशन अगर इतना घाटे का सौदा है तो नौकरी छोड़ देने के बाद इतने बरसों से उनकी रोजी-रोटी कैसे चल रही? उनका परिवार कैसे चल रहा? हालांकि वो एकमत होकर प्रकाशकों का पक्ष नहीं लेते। कहते हैं- ” ऐसा भी नहीं है कि प्रकाशक बेईमानी नहीं कर रहे हैं। करते हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि इसमें सिर्फ लेखकों का ही शोषण हो रहा है। प्रकाशकों को बेईमानी इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि सिस्टम की बेईमानी का उन्हें शिकार होना पड़ता है। पुस्तकों की बिक्री का हाल बहुत अच्छा नहीं है, खासकर हिंदी में।”
गौरीनाथ यह भी कहते हैं कि ‘यदि लेखक जागरूक रहे तो वो खुद भी अपनी पुस्तकों की बिक्री और रॉयल्टी की स्थिति के बारे जानकारी ले सकता है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन एक्ट के तहत इसीलिए बनवाया गया था ताकि लेखकों का शोषण न हो सके। नेहरू ने निराला के प्रकाशकों से विवाद होने के कारण इसे बनवाया था। यहाँ सरकारी योजनाओं के तहत खरीद की जाती है, उसका हिसाब रखा जा सकता है। एक्ट के तहत अगर प्रकाशक दोषी पाया जाता है तो तीन साल के लिए उसे प्रतिबंधित किया जा सकता है।
समझदारी, पारदर्शिता और लेखों की हिस्सेदारी को लेकर नॉटनल और नीलाभ श्रीवास्तव बहुत प्रतिबद्ध हैं। वे कई बरसों से पूरी प्रतिबद्धता से इस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी यह ईमानदारी देखते हुये जहां खुशी होती है, वहाँ एक भय भी कि इस नीति और रीति के साथ नॉटनल कितना दूर जाएगा या जा पाएगा? नीलाभ कहते हैं कि ‘वैसे तो एमबीए में बिजनेस एथिक्स का कोर्स होता है जो लगभग हर जगह कंपलसरी है। लेकिन भारत में आम धारणा यही है कि बिजनेस का मतलब झूठ, छल। मैं इस धारणा को झूठ साबित करना चाहता हूँ।‘ लेकिन चूँकि ईबुक में किताबें सस्ती होती हैं तो रॉयल्टी भी ज़्यादा नहीं आ सकती। वो कुछ सौ या हज़ार में सिमटकर रह जाएगी। नॉटनल पर किताबें सस्ती ज़रूर होती हैं लेकिन पाठकों की संख्या ज़्यादा हो जाए तो अमाउंट बढ़ने लगता है, बढ़ सकता है।
यह एक बहुत बड़ा यथार्थ है कि आज हिन्दी में प्रकाशकों की संख्या बहुत ही कम है। बड़े प्रकाशक तो उनमें भी चुनिन्दा। प्रकाशक चतुर होते हैं, बिकने वाले लेखकों को रॉयल्टी और एडवांस में रॉयल्टी देते हैं, यह भी एक मिथ है। यह मैं अपने अनुभव से भी कह रही। ज्ञानपीठ के पास भले ही किताबें बेचने का कोई व्यवहारिक तरीका न रहा हो, पर मेरे अनुभव में वो मानदेय को लेकर काफी पारदर्शी रहा। लगातार कई वर्षों तक वित्तीय साल के अंत तक मुझे मानदेय और रॉयल्टी स्टेसमेंट लगातार मिलते रहे। मेरी सर्वाधिक किताबें भी इसी प्रकाशन संस्थान से थीं। यही नहीं एक पैसे न देने के लिए ख्यात प्रकाशक से भी बाकायदा अग्रिम रॉयल्टी मिलने का भी अनुभव है। बावजूद इसके कुछ अनुभव बुरे भी रहे, जहां न कभी कोई अग्रीमेंट किया गया, न रॉयल्टी की एक पायी भी कभी मेरे हिस्से आई। एक समझदार लेखक की तरह मैंने ऐसे प्रकाशनों से आगे अपना कोई संबंध नहीं रखा। यही नहीं मैंने स्वतंत्र पत्रकारिता करते हुये भी अपना लेखन और जीवन दोनों उसकी पारिश्रमिक से बिताया है। तब मेरे पास एक डायरी हुआ करती थी, जिसमें रचना की तिथि, प्रकाशन की तिथि, कहाँ प्रकाशित हुआ, और मानदेय कितना आया और कब आया इसकी एक सूची बनी हुई थी। जिसे मानदेय मिलने के बाद राशि भरकर टिक कर देती थी। मुझे अधिकतम रचनाओं के लिए पारिश्रमिक मिले थे, यह तक कि साहित्यिक पत्रिकाओं से भी, जिनसे मैं बस अपने लेखक को बचाए रखने के लिए कहानियाँ-कवितायें बगैर किसी मानदेय की अपेक्षा और आकांक्षा के भेजती रही। आज जब बोले भारत के लिए साहित्य-सम्पादन देखते हुये नए-पुराने लेखकों का बतौर मानदेय एक छोटी सी धनराशि पाने के बाद उनका कृतज्ञता-भाव देखती हूँ, या फिर यह संदेश देखती हूँ कि ‘यह बहुत दिनों बाद उन्हें कहीं से मिला पारिश्रमिक है, कि आजकल तो लेखकों को मानदेय दिये जाने की परम्परा ही नहीं रही। या यह कि बरसों से लगातार लिखते रहने के बावजूद यह कहीं से आया उनका पहला पारिश्रमिक है, तो खुशी के साथ -साथ एक गहरा क्षोभ मन में गहराने लगता है। रोऊँ की हंसूँ, वाकई मुझे यह समझ में नहीं आता। इतनी बुरी स्थिति आखिर आई तो कैसे? क्या इसमें लेखकों का कोई हाथ नहीं? आपने इसे आने ही क्यूँ दिया? छपने की यह बेगार भूख को आप क्यों और कैसे प्रश्रय देते रहे?
सोचूँ तो इसके भीतर लेखकों का भी उतना दोष नहीं, उनके भीतर यह बात जैसे गांठ की तरह बांध दी गयी हो कि सिर्फ लेखन करके गुजारा नहीं किया जा सकता। आप पहले एक अदद स्थायी नौकरी ढूंढिए, फिर अपना शौक पूरा करने के लिए लिखते-उखते रहिए। ऐसे ही लेखक बगैर पारिश्रमिक के अपनी रचना संपादकों प्रकाशकों को नहीं देते। छापने और किताब आने पर सोशल मीडिया पर उनकी भूरी-भूरी प्रशंसा और आभार व्यक्त करनेवाले पोस्ट भी लिखते हैं। कई बार रचनाएँ संपादकों को अनुग्रहित करके भी छपती या छपवाई जाती हैं, प्रकाशकों कों पैसे देकर किताब निकलवाई जाती है। सोचने की बात यह है कि एक पूरी समयखाऊ और कई बार उबाऊ नौकरी के बाद कोई लेखक लिखेगा तो क्या लिखेगा? यदि प्रकाशक उन्हें उचित मानदेय देता, तो नौकरी की मजबूरी उनके हिस्से कदापि नहीं आती। और प्रकाशकों को भी यह शिकायत नहीं होती कि किताबें तो बिकती ही नहीं, हम रॉयल्टी दें तो आखिर दें कहाँ से। इसमें दोनों ही बराबर के दोषी हैं और यह एक एक अन्योन्याश्रित मामला जैसा है। जब आचार्य चतुरसेन ने वैशाली की नगरवधू लिखा (1948-49) तो अपनी पिछले चालीस सालों की साहित्य साधना को खारिज करते हुए इसे अपनी पहली रचना घोषित किया था। मैला आँचल के पहले रेणु ने बहुत कुछ लिखा और उसे अज्ञात रहने दिया था, आप बताइये कि आप यह क्या कर रहे हैं? लेखकों के भीतर जागरूकता सबसे अहम और जरूरी है। नहीं तो अपनी कालजयी रचनाओं में क्रांति के बिगुल बजाने वाले साहित्यकार प्रकाशकों से अपने अधिकार नहीं माँग पाते। यशैषणा अथवा अमरत्व की भावना उन्हें प्रकाशकों खासकर बड़े प्रकाशकों के आगे मुंह खोलने नहीं देती।
लोगों, खासकर लेखकों का यह आरोप भी कि सारे प्रकाशक बहुत अमीर हैं, यह भी एक इकहरी बात है। सोचने की बात यह भी है कि प्रकाशक अपनी रोजी-रोटी चलाने के लिए ही प्रकाशन संस्थान खोलता है। प्रकाशन उसके लिए समाज सेवा नहीं, बल्कि एक धंधा है, जाहिर है कि वो इसमें हमेशा मुनाफा चाहेगा। बेशक वह मुनाफा लेखकों के हक की कीमत पर नहीं होना चाहिए। मानदेय केवल लेखों को मान देना भर न हो, बल्कि उनके अंश की तरह उसे बरता जाये। इस मामले में मुझे पारिश्रमिक से भी कहीं ज्यादा अविनाश मिश्र का दिया टर्म ‘लेखकांश’ इसीलिए ज्यादा उचित लगता है।
सच तो यह है कि यह बात गम्भीर है और इसे संजीदगी से लिया जाना चाहिए। लेखक व प्रकाशक के बीच खुल कर कुछ मुद्दों पर बात होनी चाहिए और शिकायतों को दूर किया जाना चाहिए। मगर यह कोशिश सामूहिक रूप से अक्सर नहीं होती है। 2022 की बात अगर छोड़ दें तो लेखक बस अलग-अलग अपना इज़हार और गुहार करते दीखते हैं। इस क्रम में लेखक व प्रकाशक के बीच उठे मसले को बिना गहराई से समझे हुए जो शोर पैदा हुआ है, उससे ग़लतफ़हमियां दूर तो क्या ही होंगी, और बढ़ती सी दिखती हैं। इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि कॉपीराइट नियमों में आज संशोधन की बहुत जरूरत है ताकि लेखकों को उचित रॉयल्टी मिल सके। लेखक संगठनों की भूमिका भी इस संदर्भ में महत्त्वपूर्ण हो सकती है। लेखकों को चाहिए कि वे एकजुट होकर यह लड़ाई लड़ें, उनमें आपसी सहमति और सन्मति हो। वे विनोद कुमार शुक्ल की रॉयल्टी से जले-भुने नहीं, न उनकी तरह मोटी रॉयल्टी पाने की झूठी उम्मीद में किसी खेल का हिस्सा ही बनें।