श्याम बेनेगल की फ़िल्में यथार्थ और स्वप्न के संतुलन की फ़िल्में हैं। उनमें अपने समकालीन निर्देशकों की तरह एकरेखीय राजनीतिक पक्ष नहीं दिखता। उनमें घटनाओं और चरित्रों के आसपास की नाटकीयता का असर दिखाई देता है। दरअसल श्याम बेनेगल ‘इमोशन’ के बारीक रेशों की पड़ताल में माहिर हैं। चरित्रों का द्वंद्व और घटनाक्रम का चरम उनके सिनेमा में लक्षित होता है। विज्ञापन फ़िल्मों के निर्माण के रास्ते उनका फ़िल्मों में आना इतना तो ताकीद करता ही है कि उनकी फ़िल्में विचार के स्तर पर कुछ नया और अनोखा ज़रूर ही कहेंगी। और यह उनकी हर फ़िल्म के लिए लागू होता है। फिर भी बेनेगल का आग्रह कथानक के द्वंद्व पर अधिक दिखाई देता है। उनकी फ़िल्में खुलने के लिए अपना ‘स्पेस’ चाहती हैं। साथ ही किरदारों के मनोभावों और मनोविज्ञान को बेहतरीन ढंग से पकड़ती हैं। मगर बेनेगल प्रतिरोध के फ़िल्मकार नहीं। वे बदलाव के पैरोकार हैं। वे अपने सिनेमा में स्वप्न देखते हैं। अपने समय से भिड़ते भी है और उसकी आलोचना भी करते हैं। किरदारों के मन को पढ़ते हैं। उनके सिनेमा में एक समूची समाज व्यवस्था है। वहाँ दर्जनों चरित्र हैं। हर चरित्र की भीतरी जद्दोजहद है। उसका स्व है। उनके यहाँ वर्ग भेद पर निशाना तो है, महिलाओं की अस्मिता पर भी तीखे सवाल हैं और उनके हक़ की लड़ाई भी। वे बहुत सारे घटनाक्रमों की पड़ताल में माहिर हैं। उनके सिनेमा का कैनवास बड़ा है जहाँ हर वक़्त कुछ न कुछ घट रहा है।
श्याम बेनेगल को कला या समानान्तर हिन्दी सिनेमा के शुरुआती निर्देशकों में ही माना जाता है। इसलिए भी उनका काम अलग से रेखांकित हो जाता है क्योंकि सत्तर के दशक में समानान्तर सिनेमा आंदोलन की दिशा को निर्धारित करने वाली आरंभिक तीन फ़िल्में मृणाल सेन की ‘भुवन शोम’, मणि कौल की ‘उसकी रोटी’ और बासु चटर्जी की ‘सारा आकाश’ ने तीन भिन्न रास्ते निर्देशकों को दिये। तीनों फ़िल्मों में अपनी तरह का कोई साम्य नहीं। केवल मर्ज़ी से फ़िल्म माध्यम को ‘एक्सप्लोर’ करने का नज़रिया है। एक अन्य तरह से देखें तो तत्कालीन दर्शक वर्ग के लिए कोई मसाला या मनोरंजन इन फ़िल्मों ने उपलब्ध नहीं कराया और ना ही उसकी परवाह की। ऐसे में बेनेगल की फ़िल्मों को देख कर यह अंदाज़ लगाया जा सकता है कि शायद उन्होंने ‘फ़ॉर्म’ के रूप में रंगमंच और कथा-साहित्य की नाटकीयता या ‘ड्रामेटिक्स’ को अपनाया। रंगमंच कलाकार को वो करने की संभावना अथवा छूट प्रदान करता है, जो वो नहीं कर सकता। वहाँ केवल प्रयास है, इसलिए वह प्रयोग है। कर के देखते हैं – का भाव वहाँ प्रमुख है। सिनेमा की तकनीक की तरह वहाँ ‘परफ़ेक्शन’ पर ज़ोर नहीं। इसी भाव से बेनेगल अपने सिनेमा को रचते हैं। यहाँ मेरा ख़याल यह भी है कि हम अक्सर दर्शकों को दोष देते हैं, वे अच्छी फ़िल्मों को नहीं देखते या अच्छे-बुरे की समझ नहीं। मगर यह सवाल भी आना चाहिए कि दर्शकों को फ़िल्म या कला माध्यम से जोड़ने की ट्रेनिंग हमारे ‘सिस्टम’ में है भी या नहीं? साहित्य और रेडियो को छोड़ दिया जाये तो कला माध्यमों में ऐसा कोई नहीं जिसे जनता ने अपनाया हो। ऐसे में दर्शकों से सिनेमा के जानकार होने या हर तरह के सिनेमा को ‘डी-कोड’ कर लेने की अपेक्षा करना ग़लत है।
श्याम बेनेगल ने हिन्दुस्तानी जनता की इसी नब्ज़ को बखूबी पकड़ा। और अवाम में बिखरी पड़ी नाटकीयता और उसके जुड़ाव के आधार पर उन्होंने अपना सिनेमा रचा। इसके साथ ही एक ख़ास तरह की भाषा, कहानी, विचार और असर या इसके मिले-जुले को समझने वाला दर्शक वर्ग भी उन्होंने तैयार किया। सिनेमा या किसी भी को कला को देखने-समझने के लिए ‘इंटरप्रिटेशन’ ज़रूरी है। इस अवधारणा के साथ अब श्याम बेनेगल का सिनेमा बेहतर ढंग से खुल सकता है। साथ ही समझने, महसूस करने और सोचने के लिए भरपूर संभावनाएँ भी दे सकता है।

बेनेगल का सिनेमा क्या है, वह खोजना कठिन नहीं। मगर क्यों वह ऐसा रहा, उसके कुछ सूत्र उनके जीवन में खोजे जा सकते हैं। सबसे पहला तो यह कि उनका अवचेतन क्या बुन रहा? ज़ाहिर तौर पर वे गुरुदत्त से अपनी रिश्तेदारी के कारण भी सिनेमा के संपर्क आए ही । बेनेगल के पिता फोटोग्राफर थे। और फोटोग्राफी का शौक उन्हें पिता से विरासत में मिला था। बचपन में वे घर के पास के सिनेमाघर में फिल्में देखने जाया करते जिसमें अधिकतर हॉलीवुड या विश्व सिनेमा की फिल्में होती। पिता घर-परिवार के लोगों की तस्वीरें खींचते या 16mm के अपने कैमरे से फ़िल्में बनाकर पारिवारिक मिलन समारोहों में दिखाते। श्याम बेनेगल के अवचेतन पर इसका प्रभाव पड़ा ही और 12 वर्ष की उम्र में उन्होने उसी कैमरे से एक फ़िल्म बनाई ‘छुट्टियों में मौज मजा’। और तभी तय कर लिया कि वह फ़िल्मकार बनेंगे। उनकी फ़िल्मों के मूल्य भी उनके पिता की देन थे। घर में दस भाई-बहन थे और प्रगतिशील विचारों के पिता ने ताकीद की थी मैट्रिक के बाद वे केवल लड़कियों की पढ़ाई पर ख़र्च करेंगे और बेटों को अपनी पढ़ाई का ख़र्च खुद उठाना होगा। लेकिन श्याम बेनेगल की असली प्रेरणा सत्यजीत राय और उनकी फिल्म ‘पाथेर पांचाली’ थे, जिसके प्रभाव को उन्होंने अपने कई साक्षात्कारों में स्वीकार किया है। यहाँ तक कि फ़िल्मकार बतौर उनकी एक डॉक्यूमेंट्री सत्यजीत राय पर है जिसे राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था।
बेनेगल हैदराबाद से बंबई आए थे और सिनेमा बनाने की जद्दोजहद के बीच विभिन्न एडवरटाइज़िंग एजेंसियों में कॉपीराइटर की नौकरी करने लगे थे। राय भी विज्ञापन के पेशे से सिनेमा में आए थे। बेनेगल के अवचेतन में राय से प्रेरणा के साथ ही एक तरह का तुलनात्मक असर भी संभवत: रहा ही होगा। विज्ञापन का एक और महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप समाज (या किसी वस्तु के लिए उसके खास उपभोक्ता) से सीधे तौर पर जुड़ना होता है। 1960-70 के उस वक़्त के बंबई में ‘एडवरटाइज़िंग’ पेशे के कई बड़े नाम मसलन अलीक पद्मसी, गारसन द कुन्हा, सिलवेस्टर द कुन्हा, अरुण कोलहटकर, केरसी कात्रक आदि रंगमंच, साहित्य से जुड़े हुए थे। दक्षिण बंबई के कुलीन, संभ्रांत, अँग्रेजीदा वातावरण में कलाओं की ख़ुराक का अपना रुतबा था। तमाम प्रगतिशील रचनाकार कलाओं के हर माध्यम से जुड़े थे। फिर विज्ञापन लिखने-बनाने का माध्यम फ़िल्म भी था ही। ज़ाहिर तौर पर बेनेगल जैसे पढे-लिखे, सोचने-समझने वाले व्यक्ति के मन में भी चेतन-अवचेतन रूप से इन सभी सरोकारों का मिला-जुला सिनेमा पनप ही रहा होगा। यहाँ उनके सिनेमा बनाने ने अलग तरह से करवट ली। बेनेगल के पूर्ववर्ती फ़िल्मकारों ख़्वाजा अहमद अब्बास, चेतन आनंद, गुरुदत्त, बिमल रॉय, सत्यजीत राय, ऋत्विक घटक, मृणाल सेन, या समकालीन मणि कौल, कुमार शाहनी, बासु चटर्जी आदि का काम उनके सामने था ही। इन सबमें ‘फ़ॉर्म’ के साथ ‘एक्सपेरिमेंट’ केवल मणि कौल और कुमार शाहनी ने किया। राय और घटक की फ़िल्में भी कुछ हद तक ‘एक्सपेरिमेंट’ करती हैं लेकिन अंतत: उनकी दृष्टि का फ़लक कथात्मक बंगाली ज़बान और समाज से होते हुए वैश्विक पहुँच तक होता है।
बंबई की फ़िल्म इंडस्ट्री में तब का हिन्दी सिनेमा ‘सामाजिक मेलो-ड्रामा’ श्रेणी में आता था और तमाम फ़िल्मकार अपनी फ़िल्मों को उसके आर्थिक समीकरणों से जोड़ कर देखते थे। इनमें से केवल मृणाल सेन ही बांग्ला-हिन्दी के बीच आवा-जाही रखते हुए यथार्थवादी, सामाजिक-राजनीतिक फ़िल्में बना रहे थे। बेनेगल ने भी यही रास्ता अपनाया और इन सरोकारों के कारण एक हद तक बेनेगल की फ़िल्में उनके समानांतर रखी जा सा सकती हैं। बेनेगल की अपनी सोच में गाँव-देहात का यथार्थ एडवरटाइज़िंग की दुनिया की चार-दीवारी के भारत की सोच से बिलकुल अलग और ज़मीनी था। संभवत: इसीलिए अहिंदी भाषी होने के बावजूद हिन्दी का मध्यमवर्गीय समाज आगे चलकर उनकी कहानियों का हिस्सा बना। व्यवस्था के प्रति रोष तो उस दौर के बुद्धिजीवियों में था ही मगर वह सामाजिक ढाँचों मसलन – धर्म, जाति, भेदभाव, शिक्षा, बेरोजगारी, पितृसत्ता, महिलाओं की स्थिति आदि की जकड़न भरा समय भी था। बेनेगल ने इसी असंगति पर प्रहार किया। लेकिन उनका तरीका अपने पूर्ववर्तियों से कुछ अलग था और उन्होने इस सामाजिक हस्तक्षेप को कुछ अलग तरह से अपने सिनेमा में ‘अचीव’ किया जिसमें उनका बंबई के सिनेमाई माहौल में होना और अपने चुने हुए विषयों के दर्शकों से संवाद की इच्छा होना को भी शामिल किया जा सकता है। हालाँकि इस तुलनात्मक अध्ययन के बाद भी बेनेगल के सिनेमा की तीव्रता और असर कुछ कम ही है बजाए बाक़ी फ़िल्मकारों के। तब भी बेनेगल के सिनेमा को कमतर नहीं आँका जा सकता।
सिनेमा बनाने के स्वप्न में आर्थिक संसाधन बेहद ज़रूरी हैं। दृष्टि सम्पन्न फ़िल्मकारों/कलाकारों के लिए सार्थक सिनेमा की शुरुआत में सबसे बड़ी अड़चन निर्माता ढूँढने की ही होती है, जो आज भी जारी है। यह भी एक तरह का संघर्ष ही है, लेकिन यह बेनेगल के हिस्से कम ही आया। वे भाग्यशाली रहे कि ‘एडवरटाइज़िंग’ के दिनों के साथी ललित बिजलानी और फ्रेनी वरियावा द्वारा स्थापित ब्लेज़ फ़िल्म्स ने ‘अंकुर’, ‘निशांत’, ‘भूमिका’, ‘मंडी’ और ‘त्रिकाल’ जैसी फ़िल्में बतौर निर्माता प्रस्तुत की। स्वतंत्र (इंडी) फ़िल्मकार के रूप में बेनेगल इस तरह यहाँ अलग रास्ता तय करते नज़र आते हैं। आगे चलकर भी उन्हें शशि कपूर बतौर निर्माता मिले जिन्होंने उन्हें ‘जूनून’ और ‘कलयुग’ बनाने का मौक़ा दिया। बेनेगल ने हमेशा ही अपने संसाधनों की परख जारी रखी। और इसके लिए सरकारी संस्थानों की योजनाओं आधारित शॉर्ट फ़िल्म्स और विज्ञापन फ़िल्में, डॉक्युमेंट्री फ़िल्म्स बनाने की कवायद जारी रखी। भारतीय रेल के लिए दूरदर्शन पर ‘यात्रा’ धारावाहिक बनाया। और इसी रास्ते दूरदर्शन के लिए ‘भारत एक खोज’ जैसा अद्भुत और ऐतिहासिक काम वे कर गए। यहाँ एक और बात उल्लेखनीय है कि बदलते समय के साथ उन्होंने विभिन्न माध्यमों में आवा-जाही बनाए रखी। उनके समकालीन या पूर्ववर्ती या आने वाले बहुत कम फ़िल्मकारों के पास लघु फ़िल्में, डॉक्युमेंट्री, फ़ीचर फ़िल्म, टेलीविज़न या अन्य तमाम माध्यमों का उत्कृष्ट काम होगा। इस मामले में बेनेगल उनसे आगे रहे।
यह तो हुई संसाधनों की बात। दूसरी बात बेनेगल की निर्देशकीय या नेतृत्व क्षमता है। बेनेगल के आसपास हमेशा उच्च दर्जे के कलाकारों का जमावड़ा रहा। उनका यह आग्रह अभिनेताओं को लेकर है और उनकी हर फ़िल्म में उस समय के सशक्त रंगमंचीय अभिनेताओं की फ़ौज है। इस खोज में वे शबाना आज़मी, स्मिता पाटिल, गिरीश कारनाड, अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, मोहन आगाशे, कुलभूषण खरबन्दा, अनंत नाग, अमोल पालेकर, पंकज कपूर, रजित कपूर, के के रैना, अन्नू कपूर, रघुवीर यादव, नीना गुप्ता, पल्लवी जोशी, राजेश्वरी सचदेव तक तो पहुँचते ही हैं। ख़ास यह कि इन तमाम कलाकारों ने या तो पहली बार बेनेगल के साथ ही काम शुरू किया या बिलकुल अपने शुरुआती दौर में ही वे बेनेगल की फिल्मों में नज़र आए। इसके अलावा विजय तेंदुलकर और सत्यदेव दुबे जैसे दिग्गज अथवा वनराज भाटिया, गोविंद निहालानी भी उनकी टीम और ‘विज़न’ का ही हिस्सा थे।
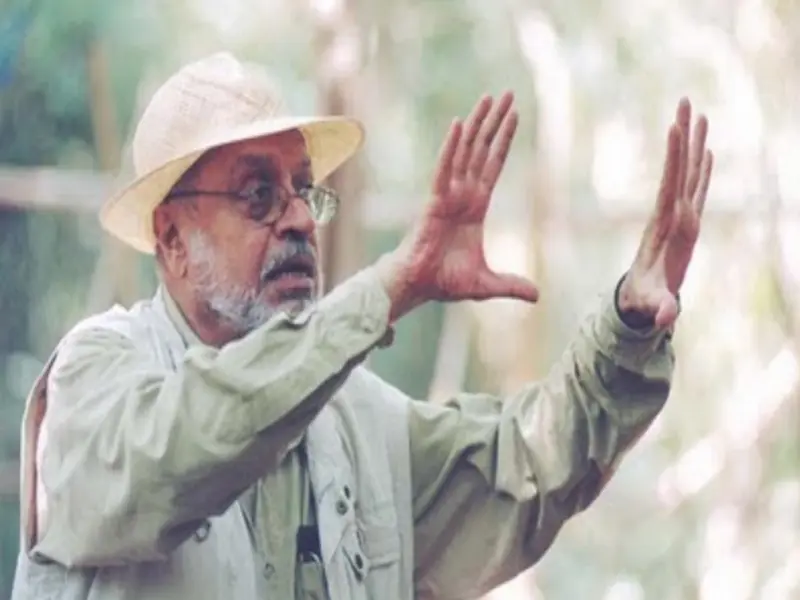
बेनेगल की सक्रियता हतप्रभ भी करती है। साल 1974 में अंकुर के बाद अगले 30 सालों तक लगभग हर साल उनकी कोई न कोई न फ़िल्म या डॉक्यूमेंट्री या धारावाहिक आता रहा। और लगभग सभी फ़िल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार या समकक्ष मान्यता मिली। यह दर्शाता है कि बेनेगल के फ़िल्मकार के पास कहने के लिए कितना कुछ है, करने के लिए उससे ज़्यादा है। उनकी चेतना में दृष्टि सम्पन्न फ़िल्मकार है जो अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य के प्रति प्रगतिशील सोच के साथ आगे बढ़ता रहा। बार-बार उनके साथ काम करने वाले कलाकारों (प्रमुख अभिनेताओं और समकालीन सहयोगियों से इतर) सुरेखा सीकरी, वीरेंद्र सक्सेना, इला अरुण, सोनी राजदान, शमा ज़ैदी, रवि झांकल, ललित तिवारी, इरफान, संजय लीला भंसाली, प्रह्लाद कक्कड़, अशोक मेहता, अशोक मिश्रा आदि पर नज़र जाती है जो दिखाता है कि बेनेगल की परख के क्या मायने हैं!
यह भी दिलचस्प है कि साल 1958 में हैदराबाद से बंबई आने के करीब 16 साल बाद बेनेगल का सिनेमा बनाने का सपना साकार हुआ। लेकिन इस दौरान गुज़रे समय में सैकड़ों विज्ञापन फ़िल्में बनाने का अनुभव बेनेगेल के हिस्से आया, जिसे उन्होंने ख़ुद को तैयार करने के अभ्यास के रूप में ही लिया। ‘अंकुर’ की कहानी भी उन्होंने सालों पहले ‘शॉर्ट स्टोरी’ की तरह लिखी थी जिसे माँजने-तराशने में उन्होंने इतने साल लिए। शबाना आज़मी के चरित्र के लिए उन्होंने दक्षिण भारतीय अभिनेत्री शारदा सहित वहीदा रहमान, अंजू महेंद्रु तक से ‘ना’ सुनी मगर सिनेमा जुनून की हद तक अपने को सुनने और उस पर जमे रहने की फ़ितरत बेनेगल की रही। ‘ब्लेज़’ के रूप में उनके अपने निर्माता तो थे ही, ‘मंथन’ के लिए गुजरात के दूध बेचने वाले पाँच लाख किसानों का दो-दो रुपया देकर निर्माता बनने की कहानी भी इसी ‘इंडी’ या स्वतंत्र सिनेमा की ऐतिहासिक घटना है। ‘मंथन’ की शुरुआत ही अँग्रेजी में लिखे इस वाक्य से होती है – 500,000 farmers of Gujrat present’। ‘अमूल’ के रूप में बनी सबसे अनोखी दूध प्रदाय और उत्पादन की व्यवस्था की यह कहानी एक मिसाल ही है। इस कहानी में वो सबकुछ है जो हमारे आसपास आज भी घटता नज़र आ सकता है। जाति आधारित भेद, राजनीति, प्रेम, धोखा, शोषण, न्याय-अन्याय के बीच की बहस, विरोध और एक बड़ा स्वप्न। पर इन सबके बावजूद व्यवस्था से टकराते हुए दर्शक दूध यूनियन के सपने तक पहुँच जाते हैं। ‘मंथन’ सच में समुद्र मंथन की तर्ज पर मथा हुआ ही कुछ था, जिसने शायद सब कुछ बदल डालने का असंभव सपना देखा था। बेनेगल अपने सिनेमा में ऐसे ही स्वप्न देखते रहे हैं। ‘मंडी’ भी ऐसी ही एक अलग दुनिया रचती है। जहां कोठे की स्त्रियाँ इंसान हैं। उन्हें स्त्रियॉं की तरह देखा गया है। इसके पहले कोठे की छवि नाचने-गाने वाली तवायफ़ों की ही होती थी। किरदार या चरित्र की तरह नहीं। इसके कई सालों बाद हिन्दी सिनेमा में ‘सत्या’ जैसी फ़िल्म आई थी जिसमें अपराधियों को इंसानों की तरह दिखाया गया था। ही ही-खी खी करती स्त्रियों और किरदारों के बीच ‘मंडी’ का स्याह ‘ह्यूमर’ भी अपने आप में ‘जाने भी दो यारों’ की तरह ‘ब्लैक कॉमेडी’ श्रेणी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। बेनेगल के तमाम प्रयोग इसी तरह फ़िल्म-दर-फ़िल्म चलते रहे और इसकी जड़ें समाज से जुड़ी रहीं। बाद के दशकों में ‘वेलकम टू सज्जनपुर’ और ‘वेल डन अब्बा’ तक यह जारी रहा। उनके यहाँ चरित्र स्वतंत्र तो हैं, उनमें विविधता भी है। वे बिलकुल देसी ज़बान ‘हाओ’, ‘नको’ ‘मेरे को’ ‘पुलिस पटेल’ ‘बाई’ जैसी ध्वनियों का इस्तेमाल करते। ‘मंडी’ में एक गीत रुक्मणी (शबाना आज़मी) गाती है, हैदराबादी लहज़े में-
मैं कित्ती बार बोल ना जी
उजला कपड़ा पेनो नक्को
काला कपड़ा पेनो नक्को
तू सदा सबस परी रहे,
गोदी हरी भरी रहे
चार दिन की चाँदनी है
दुख का तिड़का झेलो नक्को
यहाँ ‘मंडी’ ख़त्म होती है, और ठीक यहीं से ‘हरी भरी’ शुरू होती है। बेनेगल के सिनेमा में समय स्पष्ट रूप से रेखांकित होता है। वह दर्शक को बाँध लेने में विश्वास करते हैं, इसलिए उनकी लगभग सभी फ़िल्मों की शुरुआत में या तो ‘नैरेटर’ की आवाज़ सुनाई देती है या पार्श्वसंगीत जो परिवेश को बुनते हुए कथा तक ले जाता है। साथ ही यह एक ख़ास तरह का रूपक भी होता है, जो हथौड़े की तरह दर्शक के दिमाग पर लगता है। मसलन, ‘निशांत’ की शुरुआत पुजारी के स्नान मंत्रों से होती है, जिसमें न्याय, समानता, वीरता, ईमानदारी आदि का वर्णन है लेकिन एक घटना के साथ यही आदर्श तत्काल भंग हो जाते हैं। वहीं ‘त्रिकाल’ गोवा की सड़कों से गुजरते हुए खूबसूरत संगीत से शुरू होती है जिसका असर स्मृतियों में ले जाता है।

इन दिनों जब हम कहते-सुनते हैं कि आज का हिन्दी समाज एक अपढ़ समाज है, जिसे अपने अतीत, वैभव, संस्कृति, कला या परंपरा का ज्ञान नहीं या भान नहीं। तब बेनेगल जैसे निर्देशक कितने ज़रूरी हैं, यह समझ आता है। बेनेगल का फ़िल्मकार क्या बना रहा वह तो देखने की बात है ही। वह अपने समय में बनाने के लिए क्या चुन रहा, वह ज़्यादा बड़ी बात है। और फिर वह जब बहुत सारे में से चुन लेने के लिए स्पष्ट और स्वतंत्र है तो यहाँ इस कोण से देखना भी दिलचस्प है कि चुनने के लिए वह क्या ख़ारिज भी कर रहा? और फिर उनका चुनाव ‘भारत एक खोज’, ‘अमरावती की कथाएँ’, ‘कथा सागर’, ‘यात्रा’ जैसे बेहतरीन धारावाहिकों का होता है। तकनीकी रूप से भले ही ये धारावाहिक समृद्ध नहीं, मगर इस रूप में तो यह ज़रूरी है कि इनसे जुड़ने वाले नाम कौन हैं? रंगमंच और इतर कलाओं के लगभग तमाम ज़रूरी और बेहतर कलाकार बेनेगल की निर्देशकीय दृष्टि का हिस्सा रहे। वे तमाम कलाकार भारत की मिट्टी, परंपरा, संस्कृति, साहित्य, समाज, राजनीति की बात कह रहे। और फिर हिन्दी का वृहत समाज भले वह आधुनिक हो, शहरी हो या ग्रामीण – दूरदर्शन पर तब अपने इतिहास, धरोहर से रूबरू हो रहा था। एक पूरा का पूरा समाज अपने दायित्वबोध, परंपरा और विचार से समृद्ध हो रहा था। बेनेगल जैसे निर्देशक इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं कि उनका चुनाव एक पूरे समाज को शिक्षित करता रहा – हर तरह से। और इसमें हर उम्र का व्यक्ति शामिल है। मेरी पीढ़ी के लोग अपने बचपन में थे। लेकिन टेलीविज़न पर गंभीर विमर्श का हिस्सा हमारे अवचेतन को मिल रहा था। हम अपने बचपन में मोगली से भी परिचित हो रहे थे, समाचारों से भी, उनकी प्रस्तुति से भी और फिर इस तरह के धारावाहिकों से भी। ऋग्वेद के श्लोक हमारे बाल-मन पर आज भी अंकित हैं। स्क्रीन पर एक गुलाब का फूल और उसकी पत्तियाँ, ‘भारत एक खोज’ का शीर्षक और पार्श्व से वह समवेत आवाज़ें –
सृष्टि से पहले सत् नहीं था, असत् भी नहीं
अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था।
छिपा था क्या, कहाँ,
किसने ढका था।
उस पल तो अगम, अतल
जल भी कहाँ था।
अपने आस-पास की सामाजिकी, राजनीति और महिलाओं की स्थिति को चित्रित करते हुए बेनेगल ने समय-समाज को इतिहास की दृष्टि से देखने तक की दूरी तय की ‘भारत एक खोज’ के ज़रिये। यह कई मायनों में उनके सिनेमाई उत्तरार्ध और उत्कर्ष का बिन्दु भी है। यह देखना दिलचस्प है कि बेनेगल ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में सिनेमा बनाने की शुरुआत की। सन 1974 में पहली फिल्म ‘अंकुर’ के बनने तक वे 40 वर्ष के हो चुके थे। वर्ष 1988 में ‘भारत एक खोज’ के पहले तक यानि 14 वर्षों में उनके खाते में ‘निशांत’, ‘मंथन’, ‘भूमिका’, ‘जुनून’, ‘कलयुग’, ‘मंडी’, ‘त्रिकाल’, ‘सुसमन’ जैसी फ़िल्में दर्ज होती गईं। बेनेगल लगातार रचते चले जा रहे थे। ख़ास यह भी कि इस समय तक आते-आते हिन्दी का कारोबारी सिनेमा अपनी चमक खोता जा रहा था और 80 के दशक में वह अपने निम्नतम रचनात्मक स्तर पर था। बंगाल और कुछ हद तक दक्षिण का क्षेत्रीय सिनेमा थोड़ी-बहुत चमक ज़रूर बिखेर रहा था। अलावा ख़ुद के बेनेगल के आस-पास प्रेरणा के स्रोत लगभग नहीं के बराबर थे। लेकिन बेनेगल का जीनियस यही है वे अपने समय से आगे के चिंतक रहे। कम से कम अपने सिनेमा में। अपने छात्र जीवन से ही जवाहर लाल नेहरू और उनकी ‘डिस्कवरी ऑफ इंडिया’ का बेनेगल पर प्रभाव था। बेनेगल ने इसे ‘डॉक्यू-फ़िक्शन’ की तरह बनाया था। इस तरह से यह उनके यथार्थवादी फ़िल्मकार से आगे का काम था। मुझे यह धारावाहिक विश्व सिनेमा के बेहतरीन कामों में से एक लगता है। यह विचार के स्तर पर तो निश्चित रूप से गोडफ़्रे रेजियो की क्वासी त्रयी (कोयानिसक्वात्सी, पोवाक्वात्सी, नाकोयक्वात्सी) या रॉन फ़्रिक की ‘बराका’ और ‘सैमसारा’ जैसी अद्भुत फ़िल्मों के समकक्ष रखा जा सकता है। ‘भारत एक खोज’ फ़ॉर्म के रूप में भी मणि कौल या कुमार शाहनी के प्रयोगों की तरह सिनेमा माध्यम में प्रतिनिधि भारतीय सिनेमा की अवधारणा को पुष्ट करता है। रंगमंचीय तत्त्वों का आग्रह बेनेगल के सिनेमा में शुरुआत से रहा है। उन्होंने सूत्रधार की भारतीय नाट्य परंपरा का यहाँ भी प्रयोग किया है। बल्कि दो सूत्रधार- जवाहर लाल नेहरू की भूमिका में रोशन सेठ और वाचक बतौर ओम पुरी की आवाज़ों का इस्तेमाल। सिनेमा माध्यम में ‘नैरेशन’ को कमतर माना जाता है लेकिन बेनेगल ने पूरी तरह से भारतीय प्रस्तुतीकरण को साकार किया है। यह भी दिलचस्प है कि इसके बाद बी. आर. चोपड़ा निर्मित महाभारत में भी लेखक राही मासूम रज़ा ने ‘समय’ रूपी सूत्रधार के रूप में हरीश भिमानी के स्वर को प्रमुखता से प्रस्तुत किया था। बेनेगल सूत्रधार की अपनी पसंद को ख्यात साहित्यकार धर्मवीर भारती के उपन्यास ‘सूरज का सातवाँ घोड़ा’ पर इसी नाम से बनी फ़िल्म में भी ले जाते हैं। बहरहाल, ‘भारत एक खोज’ उनके फ़िल्मकार का चरम है। प्रामाणिक और गझिन इतिहास के इतने सूक्ष्म, रचनात्मक, प्रायोगिक और सरल फ़िल्मांकन की दूसरी मिसाल भारतीय सिने इतिहास में नहीं। उत्कृष्ट हिन्दुस्तानी ज़बान, फ़्लैशबैक, बेहतरीन फ़िल्मांकन, ख़ूबसूरत दृश्य विन्यास, और यादगार संगीत ‘भारत एक खोज’ के प्राण तत्त्व रहे। सम्पादन की दृष्टि से भी यह एक मुश्किल काम था, जहाँ दृश्यों और ‘नैरेशन’ की भरमार थी। उम्दा अभिनेता यहाँ भी थे। यह सब एक कृति में साधना निर्देशकीय कौशल और दक्षता के बगैर संभव नहीं।

आज शिक्षा से लेकर रहन-सहन, व्यापार आदि में नैतिकता की बहस और तरह-तरह के मनोविज्ञान की उठा-पटक, बहस के बीच अनायास ही ‘भारत एक खोज’ या ‘अमरावती की कथाएँ’ या ‘कथा सागर’ के बेहतरीन वैश्विक साहित्य की याद आती है। हिन्दी का समाज जो अब न शास्त्रीय संगीत सुनता है, न किताबें पढ़ता है न चित्रकला देखता-समझता है न ही अपने परंपरा बोध को लेकर सजग है – बेनेगल जैसे निर्देशक एक के बाद एक बेहतरीन नग़मे चुनकर हमारे सामने रखते रहे। क्या उन्हें केवल समानान्तर सिनेमा के निर्देशक के रूप में सीमित कर देना चाहिए?
इतने सबके बाद भी श्याम बेनेगल को विश्व सिनेमा में वह जगह नहीं मिलती जिसके वो हक़दार हैं। कुछेक को छोड़कर विश्व सिनेमा के महत्त्वपूर्ण फिल्म समारोहों में उनकी फिल्में जगह न पा सकीं। न ही दुनिया के फिल्म स्कूलों में उनका सिनेमा पाठ्यक्रम बतौर शामिल किया जाता है। अपने समकालीन या उस समय के सक्रिय फ़िल्मकारों मृणाल सेन, मणि कौल, कुमार शाहनी, अब्बास कियारोस्तामी, कृश्तोफ किस्लोव्स्की, आन्द्रेई तारकोव्स्की आदि के बरक्स बेनेगल का सिनेमाई दृष्टिकोण पिछड़ता नज़र आता है। नि:संदेह बेनेगल दर्शकों से संवाद में यक़ीन करते होंगे और कथानक के साथ ही नाटकीयता पर उनका आग्रह ज़्यादा है। यह एक तरह से जनभाषा में रचे साहित्य की तरह भी इशारा करता है जिसका मक़सद धरातल पर बदलाव लाना है। लेकिन कुछ जगहों पर उनके सिनेमा में शिथिलता भी है। जैसे ‘मंडी’ का अंत जो मेलो-ड्रामेटिक लगता है या ‘सूरज का सातवाँ घोडा’ में सातवीं दोपहर का कथन जब माणिक मुल्ला इस कहानी के शीर्षक पर बात करते हैं। तब संकेत के रूप में सफ़ेद घोड़ा ही दिखाया गया है। (मेरे ख़याल से निर्देशक को उस संकेत में कुछ और ढूँढना ज़रूर चाहिए था)। कला और यथार्थ के संतुलन के बरक्स निर्देशक का द्वंद्व इस तरह उनके यहाँ उजागर भी होता है। ‘त्रिकाल’ भी सरियलिज़्म के प्रभाव में मध्य में बहुत सारे फैलाव को दर्शाती है और फिर अस्पष्ट रूप से सिमट आती है अंत में। ‘निशांत’ के घटनाक्रम भी ऐसे हैं जहाँ दर्शक बतौर बहुत सारे सवाल रह जाते हैं कि ज़मींदार भाइयों के विरुद्ध क्रान्ति के आगाज़ से अंजाम का सफर बहुत जल्दी तय हो जाता है। या तो इन जगहों पर सतही-सा कुछ हो रहा या फिर ऐसा कुछ जिससे ‘कंविन्स’ होना थोड़ा मुश्किल है। और इसकी पुष्टि अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के उन तीखे सवालों से होती है जो समानान्तर सिनेमा की आलोचना करते हुए उन्होने पूछे थे। नसीर इस हद तक आलोचनात्मक रहे कि उन्होंने समानान्तर सिनेमा आंदोलन के फ़िल्मकारों (जिनमें श्याम बेनेगल भी आते हैं) के सरोकारों पर ही सवाल उठाए जो उन्होंने इन फ़िल्मों के जरिये दर्शाए थे। एकबारगी देखने पर यह लगता भी है कि व्यवस्था में बदलाव होने की जो फितरत इस सिनेमा में है, वह बहुत आसान हल है। हालाँकि ‘अंकुर’ में यह भरपाई हो जाती है। एक बच्चे का जमींदार के घर पर पत्थर मारना जैसे बदलाव की शुरुआत या प्रतिरोध का सशक्त हस्तक्षेप है। ‘मंडी’ भी इसी तरह का तंज़िया हस्तक्षेप है।
फ़िल्मकार अनुराग कश्यप मज़ाकिया लहजे में एक साक्षात्कार में कहते हैं अगर बेनेगल जैसे फ़िल्मकार न होते तो बंबई की कमर्शियल हिन्दी इंडस्ट्री के पास ही नेशनल अवार्ड भी दिखाने के लिए होते। पाँच दशकों की यात्रा में बेनेगल भारतीय सिनेमा में उस पढे-लिखे, विवेचनपूर्ण और तर्कसंगत फ़िल्मकार की तरह नज़र आते हैं जिन्हें कलाकार का दायित्व बोध है। बेनेगल का फ़िल्मकार अपने दर्शक से अपेक्षा रखता है कि वह भी अपने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और मानवीय बोध को हासिल करे। उन्होंने अपने सिनेमा में इस देश की आबो-हवा और मिट्टी की महक बनाए रखी। श्याम बेनेगल अब नहीं हैं लेकिन उनके सिनेमा को देख कर ऐसा अहसास होता है मानो हम समय की गोद में बैठे हुए है और स्मृतियों का घेरा बनाते हुए दादी-नानियाँ कथाएँ हमें सुना रही हैं। अपने देश में जहाँ धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, रहन-सहन आदि के मामले में एक राय नहीं बन पाती; ऐसे में हिंदुस्तान का प्रतिनिधि सिनेमा क्या हो? इस सवाल का जवाब बेनेगल का सिनेमा है। ऐसी फ़िल्मों या साहित्य या नाटक देखकर हमेशा मुझे लगता है कि अपने देश की कोई सच्ची तस्वीर उसके आधुनिक वर्तमान में नहीं बल्कि उसके लोक में ही है। लोक कथाओं जैसा परिवेश अपने सिनेमा में ‘अचीव’ कर लेना निर्देशक के रूप में श्याम बेनेगल का ही कमाल है।

