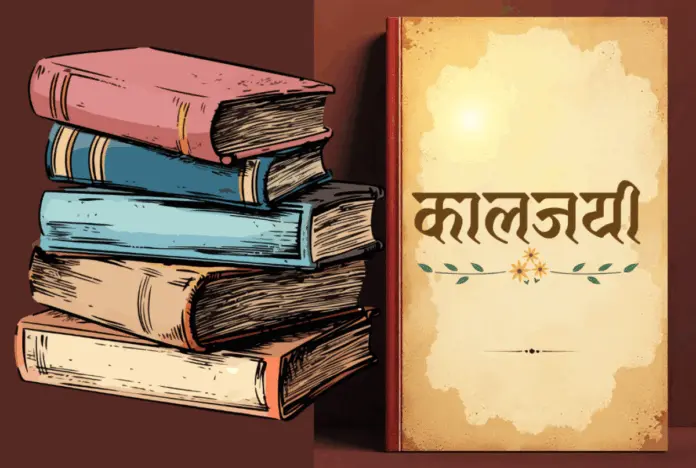जोसेफ कॉनरड, ई.एम. फाॅर्स्टर या आर्थर कॉनन डॉयल जैसे कथाकारों ने ‘व्यंग्य’ से ‘भोंडेपन’ तक ( सेटायर टू ग्रोटेस्क) तक का सफर तय किया है। पर उनका ‘सेटायर’ इतनी गहरी खुदाई नही करता, जितना श्रीलाल शुक्ल के ‘राग दरबारी’ में सामने आता है। इस उपन्यास का महाकाव्यात्मक व्यंग्य एक तरह के साहसिक अभियान की तरह आगे बढ़ता है। वह हमारी सांस्कृतिक जीवन-शैली को हास्यास्पद बनाकर, उसके पाखंडपूर्ण हो जाने की हकीकत से पर्दा उठाता है। फिर हमें वहां सभी मर्यादाएं एक अर्थहीन कर्मकांड में बदलती दिखाई देने लगती हैं। इस तरह यह परोक्ष रूप में आत्म-विखण्डन कर सकने की हद तक चला जाता है।
पर यहां व्यंग्य, भाषा-विधान के स्तर पर उतना मुखर नहीं, जितना कि वह कृति के समग्र-पाठ की व्यंजना के रूप में दिखाई देता है।
पश्चिम में व्यंग्य का ‘भोंडा’ पहलू, ‘स्व’ की बजाय, अमूमन ‘अन्य’ के प्रति मुखातिब रहता है। उसके हो सकने के लिये, किसी प्रति-स्थिति या समान्तर-स्थिति को आधार बनाया जाता है। जबकि वह जो केन्द्रीय पात्र या स्थिति का हिस्सा होकर, ‘कथ्य’ बनता है, वह अमूमन एक तरह के आत्म-व्यंग्य जैसा होता है। वह वहां किसी मार्मिक भाव-बोध की तरह ‘तरल’ या ‘अमूर्त’ होकर, पूरी कृति में फैल जाता है। ऐसा ही व्यंग्य इतना समर्थ होता है कि पाठक की यथार्थ की विसंगत दुनिया से ऊपर उठने में मदद कर सके। जैसे श्रीलाल शुक्ल का ‘राग दरबारी’।
कॉनरड, फाॅस्टर या डॉयल की कथाओं में बहुत दफा, वह जो व्यंग्य है, वह साम्राज्यवादी दर्प से युक्त होने की वजह से, ‘निष्पाप’ दिखाई नहीं देता। इसलिये यहां अब हम उसके ‘साहित्यिक मूल्य’ को लेकर सवाल उठा सकते हैं। वहां भोंडेपन को उभारने के लिए, अनेक दफा, अन्य उपनिवेशितों की तरह, भारतीय पात्रों व स्थितियों का सहारा भी लिया जाता रहा है। यह उनके प्राच्यवादी दुराग्रह का एक सुबूत है। वहाँ जो भारत है, वह इन पश्चिमी कथाओं का ‘अन्य’ संसार’ है, ‘बाहर’ की दुनियां है। इसलिए वहाँ भोंडापन ही नहीं, वीभत्स और रौद्र तक की खास तरह की मौजूदगी भी भारत को हास्यास्पद बनाने के लिहाज से दिखायी दे सकती है। वहाँ इस वीभत्स भोंडेपन का आधार हमारे सांस्कृतिक प्रतीक तक हो सकते हैं। जैसे काली माता है, जो विकराल रूप में जीभ लपलपाती, कटे हुए सिर से गिरते राक्षस के रक्त को चाटती दिख सकती है। या हमारी गुफाओं के भित्ति-चित्रों में उकेरी नग्न नारी देह हो सकती है, जो उनकी निगाह में पुरुषों की बलात्कारी प्रवृत्तियों को उकसाती है। वे ऐसी प्रवृत्तियों से युक्त भारतीय पुरुषों को, यूरोप की गरिमामय गोरियों का पीछा करते दिखा सकते हैं। और या फिर वे अपनी व्यंग्य
खुद को पश्चिम की व्यंग्य-वस्तु की तरह देखने का एक नतीजा यह निकला है, कि हमारे यहां का आधुनिक-कालीन व्यंग्य, अधिकांशतः प्रतिक्रियात्मक व आत्मरक्षात्मक हो गया है। वह आत्म-व्यंग्य के तल पर अपनी खिसियाहट और हीनता को छिपाने की कोशिश करता है।
इस संदर्भ में श्रीलाल शुक्ल के ‘राग दरबारी’ को देखें। एक तुलना तो विषय-वस्तु के प्रति दृष्टिकोण और सरोकारों की भिन्नता को लेकर सोदाहरण ही की जा सकती है। जैसे ऊपर रेखांकित किया गया है कि अनेक पश्चिमी व्यंग्यकार किस तरह सपेरों और मदारियों के हास्यास्पद विवरण उभार कर भारतीय समाज के असभ्य और पिछड़ा हुआ होने की बात करते हैं। तो यहां इस उपन्यास की चरम-सीमा में अहम हो गया एक मदारी ही है, जो उस नज़रिये की आधारहीनता की पोल खोल कर रख देता है। ‘राग दरबारी’ का यह जो मदारी है, वह व्यंग्य के औपनिवेशिक संसार का जन-पक्षीय प्रतिपक्ष बनकर सामने आता है।
हम यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि रचनात्मक अभिव्यक्ति के तल पर, इस उपन्यास के व्यंग्य ने अकारण ही, ‘बहक’ जैसा रूप नहीं लिया होगा। वह नशेड़ियों की ‘विवेकपूर्ण पीनक’ की तरह आया और एक साथ प्रतिक्रियात्मक व आत्मरक्षात्मक दोनों तरह का होने में समर्थ हो गया। लेकिन उसमें वह जो आत्मालोचन का साहस है, वह उसे बहुत ऊपर उठा देता है और आत्म-रूपांतर के लिये गुंजाइश तक पैदा करता है।
फिर वह चाहे बालमुकुन्द गुप्त के ‘शिवशंभु के चिट्ठे’ का व्यंग्य हो या भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के ‘अंधेर नगरी’ का, पीनक की गहरी विवेकपूर्णता सभी जगह हैरानी में डालती है।
भारत में व्यंग्य, बुनियादी तौर, पर ‘आत्म विखण्डक’ है। वह एक तरह की रचनात्मक ‘पाखण्ड खण्डिनी पताका’ की तरह है। इसे महज़ एक अन्य तरह का व्यंग्य कहकर उड़ा देना ठीक नहीं होगा। भारत में अभी तक जितने भी सांस्कृतिक जागरण या नवजागरण हुए हैं, उनका प्रवर्तन, किसी-न-किसी सन्त, आचार्य या प्रज्ञा-पुरुष के द्वारा लहरायी गयी, पाखण्ड खण्डिनी पताकाओं के ज़रिये मुमकिन हुआ है।
श्रीलाल शुक्ल के ‘राग दरबारी’ का रचनात्मक व्यंग्य, स्वातंत्र्योत्तर जन-जागरण का जैसे कोई ‘कच्चा मसौदा’ है, जिसके निशाने पर है हमारी पाखंड-पूर्ण नैतिकता। वह भ्रष्ट आचरण को छिपाने के लिये, मर्यादा को एक पीनक की तरह निबाहती है। लेकिन पीनक में होने की वजह से बहक जाती है।
इस रूप में इस उपन्यास के अधिकांश पात्रों का बहक जाना, एक तरह का राष्ट्रीय रूपक है। वह परंपरागत ‘लीला-भाव’ का पतनशील संस्करण है। बहक, भ्रष्ट आचरण को जीने लायक बनाये रखती है। वह एक धोखा पैदा करती है कि जो हो रहा है, एक खेल है। वह सभी को नैतिक अंतर्द्वंद्व से बचाये रखती है। इस तरह वह गिरावट को, एक शाश्वत यथास्थिति-मूलक जीवन-शैली मे बदल देती है।
इस उपन्यास के कुछ पात्रों की ‘बहक’, और उसकी वजह से गहराती पतनशीलता, फैलकर, एक तरह के ‘नये भारतीय चरित्र’ का पर्याय हो गयी लगती है। मौजूदा समय में हम जब अपने कर्णधारों को लोगो से झूठे वादे करके बरगलाता देखते है, तो किसी को परेशानी नहीं होती। बहकाने वाले, हमे अपनी बहके रहने की सुविधा के, एक छोर की तरह लगते हैं। इससे हम बिना कुछ किये-धराये, बिना बदले, अपनी और बाकी की पूरी दुनिया की ‘गहन आलोचना के शगल में रात-दिन डूबे रह सकते हैं।
जैसे मध्यकाल में हरि-सुमरन में डूब कर हम पार लगने के सपने देखते ही आये हैं। भ्रम को सच मानने का हमे खूब अभ्यास है। उस दौर को हम अपने ‘मध्यकालीन जागरण’ का नाम तक देते आये हैं। उसे देखते हुए लगता है कि राष्ट्रीय बहक का यह जो आधुनिक दौर है, वह हमें सच में किसी नवजागरण तक ले ही जायेगा।
तो आइये, श्रीलाल शुक्ल के ‘राग दरबारी’ के साथ, अब सीधे, वैद्यजी की बैठक में प्रवेश करते हैं।
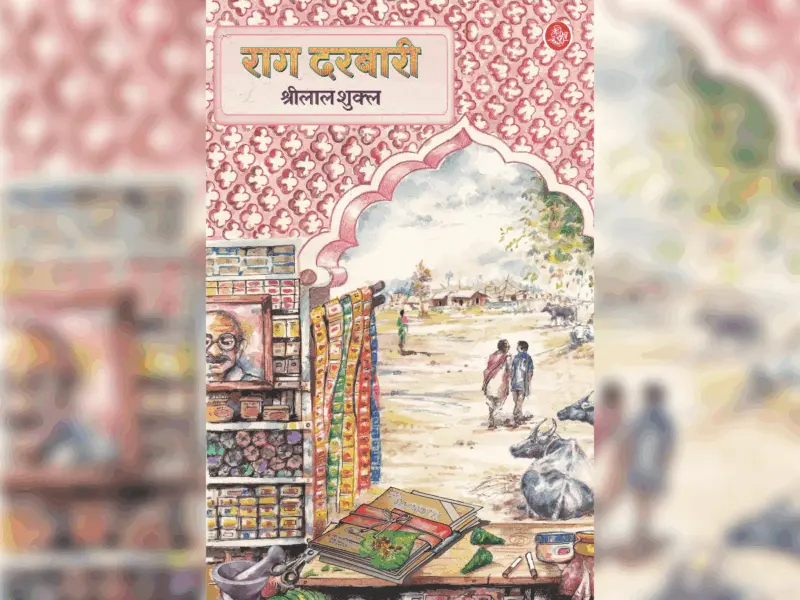
उपन्यास आरंभ में ही इस राज़ से पर्दा उठा देता है कि वहाँ, उस बैठक में, ‘भारत के गाँवों की आत्मा निवास करती है।’ तो ‘आत्म-पोषण’ के लिये वहां, रात-दिन भाँग घोटने की प्रथा का, धार्मिक कट्टरता के साथ, यों ही पालन नहीं किया जाता। इसके पीछे एक गहन-गंभीर जीवन-दृष्टि है। यह जो भांग है, वह स्वास्थ्य-वर्धक है। सब तरह की बीमारियों का ‘रामबाण ईलाज’ है। एक स्वस्थ शरीर में ही शक्तिशाली आत्मा का निवास संभव है। अपने इस जीवन-दर्शन के विस्मरण का परिणाम, बकौल वैद्य जी, यह निकला है कि हमारे शहरो ने अपनी आत्मा को खो दिया है।
तो होता यह है कि शहर में बीमार रहने वाला रंगनाथ ‘स्वस्थ होने के लिये’, गांव चला आता है। गांव, उसके लिए वैकल्पिक जीवन शैली का पैगाम है। यहां आते ही वह पाता है कि भाँग एक अचूक दवा की तरह काम करती है। वह मनुष्य के, अंतर्द्वंद्व में धकेलने वाले विवेक को, बीमार करने वाले जीवाणुओं की तरह, काबू में रखती है। वह विवेक को मारती नहीं, परन्तु उसे उतना सुलाये रखने में मदद करती है कि वह विद्रोही होकर रास्ते से भटक न जाए।
मिशेल फूको ने स्पष्ट किया है कि ‘सत्ता और ज्ञान के द्वारा समाज का जिस तरह का दमन होता है, वह ‘पागलपन’ का मूलस्रोत है। वह बात यूरोप की हकीकत को ठीक से बयां करती है। अब आइये, इस उपन्यास की मार्फत देखते हैं कि भारत जैसे मुल्को में क्या होता है? वह जो सत्ता और ज्ञान की धारा है, वह हमारे यहा वैद्य जी जैसों की बैठकों में, घोंटी जाने वाली भाँग के अजस्र प्रवाह जैसी है। यह सत्ता और ज्ञान का एकदम अलग रूप है। वैद्य जी जैसे लोगों को जैसे पहले से ही पता है कि सत्ता और ज्ञान से उपजने वाला दमन पागलपन का स्रोत होता है। तो उन जैसे लोगों ने, इस संभावित पागलपन को काबू में रखने के लिये भांग का इंतज़ाम पहले से ही कर रखा है।
यह पीनक की बहक, यहाँ एक कथास्थिति के रूप में अनेक कारणों से अहम हो गयी है। बहक, मनुष्य को सच बोल सकने का मौका देती है। सच बोलने के लिए इसके अलावा दूसरे रास्ते बंद कर दिये गये हैं। उन दूसरे रास्तों के नाकों पर, सत्ता और ज्ञान के चौधरियों ने, पहरा बिठा रखा है। परन्तु बहक को कोई आपत्तिजनक नहीं मानता। इसे हम बहक की दार्शनिक विमर्शभूमि की तरह भी देख सकते हैं।
किसी मनुष्य के ज़िंन्दा होने का एक सुबूत यह भी है कि वह बहक सकता है। इतना ही नहीं, जिन्दा बने रहकर अस्तित्व-बोध या संघर्ष-चेतना जैसे अपने मानवीय सारतत्व तक की एक झलक पाने में बहक हमारी मदद कर सकती है। जगत या समाज के सच तक अनायास पहुंचने का रास्ता है यह बहक। इस रूप में सच, मिल कर भी नहीं मिलता है। इसलिये ऐसे सच से किसी की कोई परेशानी नहीं होती। और आप झूठे हो जाने की स्थिति से भी बच जाते हैं।
भारत जैसे तीसरी दुनिया के मुल्कों में आदमी को उसकी यह अपनी ज़मीन अब, पीनक जैसी अर्ध-तन्द्रा या अवचेतन की स्थितियों में मिलती है। आत्माभिव्यक्ति के लिये पीनक, एक रचनात्मक संभावना बनकर आती है। इस तरह पीनक उसके लिये’आत्मा’ का प्रवेश-द्वार बन जाती है, और बहक उसकी अभिव्यक्ति का मार्ग। औपनिवेशिक दौर आरंभ-काल से, खुलता चला आ रहा ‘शिवशंभु का यह चिट्ठा’, हमारे व्यंग्यमय यथार्थ का पर्याय बन गया है।
यह उपन्यास गवाह है कि हमारे मौजूदा उत्तर-औपनिवेशिक हालात में भी, यह पीनक ही अब तक हमारी हमसफर बनी रह गयी है। वह जिस हद तक विकल्पहीन रूप में, हमारी सहचरी है, उस हद तक वह हमारी नियति भी है। इसे अगर ‘राग दरबारी’ जैसी कृति की मार्फत हम एक विश्वसनीय रचना-अनुभव की तरह पाते हैं, तो यह सुबूत है, इस कृति के एक बड़ी कृति होने का।
अब एक तुलना करें। मुक्तिबोध की कालजयी कविता ‘ब्रह्म-राक्षस’ के आत्म-निर्वासित बौद्धिक की ‘बड़बड़ाहट’, कैसे हमारे सामूहिक अवचेतन से बाहर निकलती है और ‘राग दरबारी’ के जोगनाथ की ‘सर्फरी बोली’ की शक्ल ले लेती है। ‘ब्रह्म-राक्षस’ और ‘अंधेरे में’ के अवचेतन में पड़ा ‘इतिहास’, बिम्बों की एक श्रृंखला की तरह टूटता है। इस तरह वह सचेतन-यथार्थ को स्वप्न-यथार्थ के रूप में विखण्डित करता है। इससे भागते हुए इन कविताओं के नायक जिस संघर्ष-संभावना को खोजते हैं, वह खुद स्वप्न-दशा जैसी वस्तु बन जाती है।
इसका अर्थ साफ है। क्रूर, अमानवीय और विसंगत यथार्थ को एक स्थिति के रूप में तभी जिया जा सकता है, जब हम किसी तरीके से अपने अवचेतन में चले जाएं। आत्म-निर्वासित होकर यथार्थ को स्वप्न की तरह, झेलने-भोगने लायक बना लें। वहां उस अवचेतन में प्रवेश करना, सीधे मुमकिन न हो, तो भांग की पीनक जैसी किसी चीज़ का सहारा ले लें। जैसे भी हो, बस खुद में गर्क हो जाएं।
यहाँ से आगे ‘डेढ़ इंच ऊपर’ का स्वप्न-लोक है। उसमें जो एक दफा धंस गया, उसका वहां से आसानी से लौटना मुमकिन नहीं होता। फिर भी आदमी लौटने का थोड़ा प्रयास ज़रूर करता है। लेकिन बार-बार असफल होकर, आखिरकार हथियार डाल देता है। फिर संघर्ष को भी, ‘यथार्थ’ के तल पर पांव टिकाने लायक जगह मिलनी, लगातार मुश्किल होती जाती है।
संघर्ष-चेतना हारती है, परन्तु यह व्यंग्य स्थिति सदाबहार बनी रहती है।
यह जो हमारी व्यंग्य-स्थिति है, वह यथार्थ की वस्तु नहीं होती, फिर भी उससे ‘परे’ नहीं कहलाती।
बेशक ‘राग दरबारी’ में भी पलायन से निजात नहीं मिलती। परन्तु यह कथा-स्थिति, मुक्तिबोध की काव्य-स्थितियीं से कुछ बेहतर मालूम पड़ती है। वजह यह है कि यह मात्र स्वप्नवत् होकर अमूर्त होने से बच जाती है।
यह भारत के औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक हालात का नतीजा है कि हमारे यहाँ यथार्थ से सीधी रचनात्मक मुलाकात या मुठभेड़ असम्भव हो गयी है। इसलिए नवजागरण के दौर में जो नववेदान्तिक रास्ता खोला गया था, उसका मकसद यथार्थ को स्वप्नवत बनाकर संघर्ष को ताकतवर बनाने की कोशिश से जुड़ा था। यहाँ मुक्तिबोध, निराला के करीब मालूम पढ़ते हैं। ‘जागो फिर एक बार’ में निराला का संघर्ष का मार्ग, यथार्थ को ‘माया है’ कहकर संबोधित होता है। उसकी दुश्वारियों को वे, ‘पदरज भर नहीं यह पूरा विश्व-भार’ कहकर झेलने के लिये प्रेरित करते है। ताकि ‘जगना’ मुमकिन हो सके। पर यथार्थ के मिथ्या हो जाने के बाद, यह जो खास तरह का जागना है, वह ‘सपने में जागने’ जैसा ही अधिक लगता है। उस अर्थ में वह जितना यथार्थ है, उतना ही अयथार्थ भी है।
ज़ाहिर है कि एक तरह से, निराला और मुक्तिबोध के स्वप्न-लोक भी, व्यंग्य स्थितियों जैसे ही है। ऐसे में पीनक और बहक की, जिस तरह की व्यंग्य-दशाएं इस उपन्यास में दिखाई देती हैं, वे ज़्यादा काम की चीज़ हो उठती हैं। वे ऐसी अनुभव-दशाएं हैं, जो यथार्थ से मुंह नहीं चुरातीं।
परन्तु जैसा नंददुलारे वाजपेयी ने लक्ष्य किया है कि यह जो व्यंग्य नाम की वस्तु है, वह ‘दुधारी तलवार की तरह’ होती है। वह ‘सामने वाले को ही नहीं, तलवार चलाने वाले हाथों को भी काटकर लहुलुहान कर देती’ है। फिर भी व्यंग्य काम की चीज़ है। वह संघर्ष-चेताओं के, अहं और दैन्य, दोनों को तार-तार करता है। और यथार्थ को उसकी वस्तुनिष्ठता में जानने-समझने के लिए तैयार करता है। इस तरह तैयार होना बहुत अहम है। वह विकल्प न होने पर भी, उसे खोजने की मानसिकता प्रदान करता है।
यह तैयारी राग दरबारी का उत्तर-राग है। या कहें कि वह कृति के व्यंग्य-रूप की व्यंजना है। व्यंजनार्थं थोड़ा मुश्किल से पकड़ में आता है। वह कई दफा कृति में होकर भी, उससे बाहर पूरे समाज की संरचना में छिपा रहता है। परन्तु इस अर्थ को पकड़े बिना हमारा काम नहीं चल सकता।
कृति के व्यंग्य-रूप की व्याख्या से यह तो बताया जा सकता है कि फलां कृति किस तरह अर्थपूर्ण है। परंतु वह इस तरह क्यों अर्थपूर्ण है, इसका विश्वसनीय जवाब, दूर कहीं और छिटका पड़ा रह गया मालूम होता रहता है। इसके लिए दृश्य से परिदृश्य में कूदना होता है। बेशक इस खतरे को उठाते हुए कि कृति पर जो ‘फोकस’ होता है, उसे परिदृश्य, पहले तो बिखेरता है, फिर एक नये कृति-पाठ की तरह पुनः रचता है।
कृति की इन दृश्य-परिदृश्य संबंधों के आधार पर व्याख्या के लिए, सबसे पहले तो कृति के शीर्षक ‘राग दरबारी’ को आधार बनाते हैं। यहां दरबारी दौर की पुराण कथा-शैली की जो ‘पैरोडी’ है, वह उस विरासत का विखण्डन करती है। इस दृष्टि से यह रूप के विद्रूप और अर्थ के अनर्थ का भाव उपजाती है।
इसका आभास हमें आरंभ में ही हो जाता है, जब कहा जाता है कि ‘वैद्य जी हैं, थे और रहेंगे’। कथन का यह अन्दाज़ पौराणिक अवतारवाद की अनुगूंज लिए है।
फिर वैद्यजी के साथ ‘राग दरबारी’ की शास्त्रीय ज़मीन, सत्ता के मौजूदा उत्तर-राग में बदलती दिखाई देने लगती है। सांस्कृतिक परम्पराओं की बड़ी भव्य, उदात्त व विराट् पृष्ठभूमि विरासत की तरह आती है और उत्तर-राग के लय-भंग का शिकार हो जाती है।
शास्त्रीय दौर की याद दिलाता हुआ वैद्यजी के पास आयुर्वेदिक स्वास्थ्य फार्मूला भी है। वह जड़ी-बूटियों के विशद ज्ञान से सराबोर है। लेकिन उसके गुण तभी उजागर होते हैं, जब उसे भाँग में रगड़ा-डुबोया जाता है।
फिर उनकी योग-मूलक मानसिकता से आया ब्रह्मचर्य भी है। वह उन्हीं के जवान और गैर-पहलवान बेटों के द्वारा व्यभिचार के खेल में बदल लिया जाता है।
फिर उनके हनुमान-अखाड़े से, एक ‘छोटा पहलवान’ और, प्रकट होता है। वह वैद्यजी के नायक हनुमान की स्वामिभक्ति के आदर्श को अपनी पितृभक्ति से चार (काले) चांद लगा देता है, और तमाम मर्यादाओं को ताक पर रखकर, अपने पिता को पीट डालने के अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन करता है।
संस्कृति के ऐसे व्यंग्य-विखण्डन के बाद किसी ‘आत्मा’ को पाने का कौन-सा मार्ग बचा रह जाता है, इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं। इससे यह प्रश्न उठता है कि यह जो सत्ता-विमर्श (राग दरबारी) है, क्या वह अपने आप में पर्याप्त है? उसका प्रयोजन क्या है? यहां जिस तरह सत्ता को साध्य बना लिया गया है, उससे सभ्यता को उसकी ज़मीन से बेदखल करने के हालात पैदा हो गये है। पर यह सवाल बचा रह जाता है कि ऐसा करनेे से आखिर हासिल ही क्या होगा?
अगर संस्कृति का विखण्डन ज़रूरी है, जैसा कि ‘राग दरबारी’ में संभव हो सका है, तो वह हमें ले कहां जाता है? संस्कृति के विखंडन का काम जैसे ही एक मुकाम पर पहुंचता है, सभ्यता के लिये भी अपनी ज़मीन पर लौटना तत्काल ज़रूरी हो जाता है। परन्तु इस विकल्प का अभाव, हमारे सामने एक गंभीर चुनौती पेश करता है।
इसका अर्थ है- आत्महीनता के खतरनाक अराजक परिदृश्य से घिर कर रह जाने के लिये तैयार होना। यह हमें किसी आत्महन्ता भविष्य की ओर धकेल सकता है। ऐसे भविष्य की ओर, जो हमे कहीं का नहीं छोड़ेगा।
यहाँ हिन्दी आलोचना के मौजूदा परिदृश्य पर एक अवांतर टिप्पणी ज़रूरी लग रही है। अपनी कृतियों की आलोचना करते हुए हमारा काम उनके विवेचन-विश्लेषण से ही चलने वाला नहीं होता। हर आलोचना हमें भविष्य के प्रति उत्तरदायी भी बनाती है। पर उस दायित्व को हम तभी निभा सकते हैं, जब आरोपित और आयातित औजारों और दृष्टियों से थोड़ा अलग हटकर सोचें। हमारा साहित्य जो है, जिस तरह का है, उसी में समाज को दिशा दिखाने के सूत्र भी होते हैं। बेशक वे परोक्ष होते हैं। इसलिये उन्हें खोजना पड़ता है।
लौटकर अब चलिए, ‘राग दरबारी’ के सांस्कृतिक विखण्डन वाले पहलू के व्यंजनार्थ की तरह मौजूद, सभ्यता के विकास वाले पक्ष को, खोजने की कोशिश करते हैं।
यहाँ रंगनाथ के रूप में ‘शहर का एक बीमार’ आदमी, गाँव की ओर मुड़ा और लौटा है। यहां सवाल ये है कि हमारे समय मे सभ्यता के नव-विकास की आधार-भूमि कहां है? नये तरीके से सभ्य होने के लक्षणों की खोज में हम अंततः भारत के ऊबड़-खाबड़ शहरी विकास की ओर ही तो देख पाते हैं।
गांव का परंपरागत परिदृश्य, जैसा कि हमने इस उपन्यास में देखा, विखंडनीय हो गया है। दूसरी तरफ शहरी परिदृश्य है। उम्मीद उसी से है। वह संस्कृति के पतनशील रूपों से थोड़ा-बहुत आज़ाद होने की प्रक्रिया में भी है। पर अभी उसके पास किसी नयी सभ्यता की कोई पुख्ता ज़मीन भी नहीं है। जैसी रंगनाथ की स्थिति है, वह अपने विकृत हालात से जूझता हुआ बीमारी से ग्रस्त हो गया है। यह वह परिवेशगत पृष्ठभूमि है, जो इस कृति की आधार स्थिति की तरह हमारे सामने है।
जहां तक आर्थिक हालात का सवाल है, विकास का पूरा ढाँचा दिशाहीन है। उसमें गाँवों जैसे एक गाँव शिवपालगंज की, ‘गंजही संस्कृति’ की भूमिका, केंद्रीय हो गयी है। जन-कल्याण को एक पाखंड में बदलती हुई वह अपने ही नशे में डूबी है। इसलिये वह कोई विकल्प नहीं बन पाती।
भारत के गाँवों का अपना ‘आत्मस्वायत्त आर्थिक ढाँचा तो औपनिवेशिक दौर में अंग्रेज़ों के द्वारा कब का नष्ट किया जा चुका है। गाँवों में आज़ादी के बाद जो नया विकास माॅडल लाया गया, उसने उन्हें शहरों पर निर्भर एक ‘परजीवी’ में ही अधिक बदला है। नयी तरह से जीने और स्वावलंबी हो सकने में मदद करने के लिये नव-पंचायत, को-ऑपरेटिव, स्कूल-काॅलेज और पुलिस थाने जैसी भी संस्थाएँ सक्रिय हुईं, उन्होंने वहाँ भी शहरी सभ्यताकरण का अधूरा और विकृत विस्तार भर किया। सारा सत्ता-विमर्श इन्हीं ‘लाभदायक संस्थाओं’ के आसपास केन्द्रित होकर रह गया। यह पूरा एजेंडा आरोपित है। वह हमारे अपने ग्रामीण यथार्थ से उपजी वस्तु नहीं है। यह लखनऊ जैसे महानगर का, आसपा के गाँवों तक फैलता शहरी सभ्यता का आधुनिक अभिशाप अधिक है।
शहर के आदमी’ के रूप में रंगनाथ की, एक गांव के ऐसे ‘शहर-परजीवी’ सत्ता-पाखंड से, सन्तुष्टि नहीं हो सकती। इससे तो बेहतर है- ‘शहर के बीमार’ की तरह रहना और जीने के हालात खोजना।
परन्तु रंगनाथ की शहर वापसी कृति का व्यंग्यार्थ नहीं है। हालांकि इस कृति के एक नाट्य रूपान्तर में इसी ओर ज्यादा तवज्जो दी गयी है। कृति के अन्त में जो मदारी आता है, वह इस कृति के बाहर छलांग लगाने के लिए एक खिड़की का काम करता है।
मदारी कृति के पूरे सत्ता-विमर्श के ताने-बाने के बाहर का आदमी है, परन्तु उसका खेल कृति के व्यंग्यार्थ को, रंगनाथ के अन्तर्विवेक के रूप में प्रकट करने के लिए एक बहाना बन जाता है।
मदारी, कृति का जनपक्ष है। वह ठीक से न शहर का है, न गाँव का। एक तरह से वह शहर व गाँव दोनों का ‘अन्य पक्ष’ है। उसके साथ दूसरे सामान्य-जन वहाँ कहीं पीछे खड़े दिखायी दे सकते हैं। वे अपनी ज़मीनी अर्थवत्ता और सभ्यता की उपज हैं। वे अभी विनष्ट नहीं हुए हैं। उनकी मानसिकता अभी तक किसी गहरी ‘प्राकृतिक न्याय’ की मौजूदगी में यकीन से बंधी है।
कहीं- कहीं यह प्राकृतिक न्याय, कृति के विरूपित सत्ता-विमर्श के भीतर भी, एक अलग तरह की संघर्षशीलता की तरह प्रवेश करता है। जैसे ‘लंगड़’ का भ्रष्ट न्यायपालिका से न्याय पाने की उम्मीद से भरा संघर्ष है। कोई सामान्य-जन इस तरह का संघर्ष नहीं करता है। उसे सभ्यता के विकास की प्रतीक इन शहरी संस्थाओं पर कुछ खास भरोसा नहीं है। परन्तु अपने भीतर अन्तर्भूत प्राकृतिक न्याय को लेकर वह कभी नाउम्मीद भी नहीं होता है।
यह भारत का ‘जनपक्षीय अन्य’ है, जिसे पश्चिम ने अपने सभ्यतामूलक विकास की झोंक में अपने समाजों में नष्ट कर दिया है।
इस आलेख के आरम्भ में भी इस संभावना की बाबत संकेत किया गया है। उसे दोहराते हुए पुनः कहा जा सकता है कि पश्चिम, भारत व अन्य तीसरी दुनियां के यथार्थ को ‘विद्रूप भोंडेपन’ वाले व्यंग्य-बोध में बदल कर खारिज करता है। परंतु भारत की इस तरह की औपन्यासिक कृतियों में अभिव्यक्त होने वाले, रचनात्मक व्यंग्य का स्वरूप वैसा नहीं है।
‘राग दरबारी’ का मदारी इस ‘अन्य पक्ष’ को खारिज नहीं करता। उल्टे उसे ही समेट और सहेज कर, कृति के सभ्यता-मूलक व्यंजनार्थ की ज़मीन बना लेता है। यहां हम भारतीय व्यंग्य के अलग तरह की सम्भावना वाले अन्तर्विकास को देखते हैं।
समाज की मुख्यधारा से बाहर, हाशिये पर होने के बावजूद, मदारी जैसे आम आदमी का यह ‘अन्य-पक्ष’ या जन-पक्ष, किसी विकल्प के मौजूद होने की ओर इशारा करता है।
उसे ‘फोकस’ में लाने वाला यह विकल्प, ‘खालिस भारतीय व्यंग्य-बोध का पर्याय है। वह पश्चिमी व्यंग्य की तरह ‘अन्य-हन्ता’ नहीं है। वह एक तरह से पश्चिमी व्यंग्य-बोध का ‘पोलेमिक्स खड़ा करता है। वह, उसकी तुलना मे, कहीं ज्यादा मानवीय है। और, इतना ही नहीं, वह एक खास तरह के सभ्यता-मूलक नव-विकास का हेतु भी लगता है।