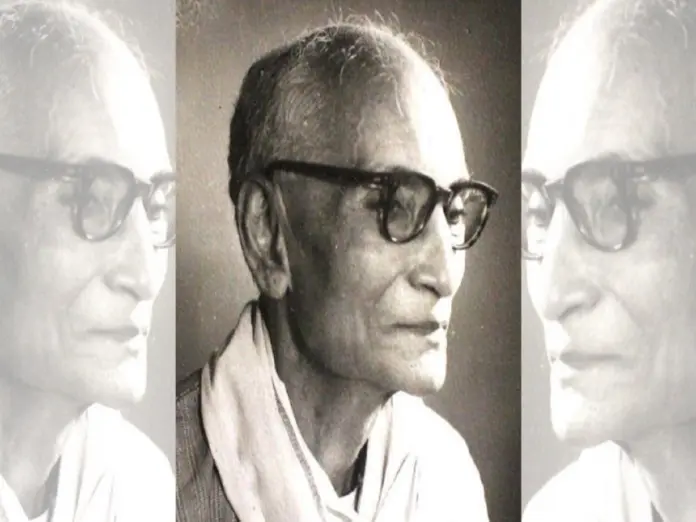आखिर राजा राधिकारमण प्रसाद जैसे लेखक हिंदी आलोचकों की दृष्टि से क्यों ओझल हो गए और हाशिये पर चले गए, जबकि उनकी 8 खंडों में रचनावली वर्षों पहले छप चुकी है और उनकी कहानी प्रेमचन्द और गुलेरी जी से पहली आ चुकी थी औऱ उनक़ा उपन्यास भी 1936 में ही आ गया था। उनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियाँ भी आज़ादी से पूर्व आ गयी थीं। यही नहीं 1962 में ही उन्हें पद्मभूषण भी मिल चुका है। फिर क्या कारण कि उनका कोई मूल्यांकन नहीं हुआ और अकादमिक जगत के विमर्शों में कोई उनक़ा नाम लेवा नहीं रहा।
मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी “सौत” 1915 में छपी थी जबकि उससे चार वर्ष पूर्व राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की उल्लेखनीय कहांनी “कानों में कंगना “छपी थी। जयशंकर प्रसाद ने 1913 में अपनी पत्रिका” इंदु” में उसे छापा था और उससे भी पहले वो आगरा के कॉलेज की पत्रिका में छप चुकी थी।
हिंदी साहित्य में अक्सर हिंदी की आरंभिक कहानियों में माधव राव सप्रे की ‘टोकरी भर मिट्टी’ , रामचन्द्र शुक्ल की कहानी ‘ग्यारह वर्ष का समय’ राजबाला घोष की ‘दुलाइबाई’, प्रेमचन्द की ‘सौत’, प्रसाद की ‘ग्राम’ और गुलेरी की ‘उसने कहा था’ की चर्चा होती है लेकिन लोग ‘कानों में कंगना’ की चर्चा नहीं करते या कम करते हैं और आज की नई पीढ़ी तो उस कहानी से वाकिफ भी नहीं होगी। क्योंकि हिंदी आलोचना की मुख्य धारा में राजा जी का जिक्र कम हुआ,.उनकी चर्चा नहीं हुई, उनक़ा मूल्यांकन भी नहीं हुआ। जबकि ‘उसने कहा था’ की चर्चा अधिक हुई और वह कालजयी कहानी मानी गई। जबकि सच्चाई यह है कि राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह की यह कहानी किसी मायने में ‘उसने कहा था” से कम नहीं है, बल्कि अपने कथा विन्यास में उससे अधिक कसी हुई और गहरी मार्मिकता लिए हुए है।
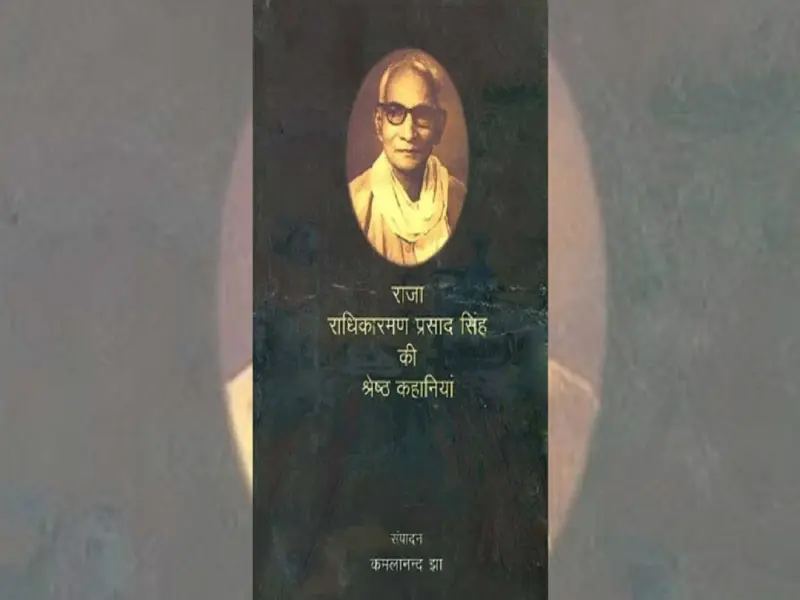
1911 में पहली बार कालेज पत्रिका में छपी ‘कानों में कंगना’ के शिल्प और विषय वस्तु को देखें तो वह बहुत ही अनूठा और नवाचार लिए हुए है। दरअसल वह अपने ट्रीटमेंट में एक विश्व स्तरीय कहानी है।
अगर आप उस कहानी को गौर से पढ़े तो वह एक बहुत ही क्रिस्प कहानी है, उसमें कहीं से कोई अनावश्यक विस्तार नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों इस कहानी की तरफ आलोचकों का ध्यान नहीं गया, या उतना नहीं जाता है जितना जाना चाहिए था और उसे भी एक कालजयी कहानी माना जाना चाहिए था।
‘कानों में कंगना’ एक ढहते सामंतवाद की कहानी है। इसमें एक अय्याश किस्म का जमींदार अपनी बीमार पत्नी की उपेक्षा करते हुए उसके अस्तित्व को नजर अंदाज करते हुए एक कोठे पर तवायफ के पास जाता रहता है और अपनी यौन पिपासा मिटाता है। और बदले में अपनी पत्नी के आभूषण उस वेश्या को दिया करता है। इसी तरह उसकी पत्नी के गहने खत्म होते जाते है और अंत में जब वह जमींदार पत्नी के ‘कानों के कंगना’ को उस तवायफ़ को देने के लिए कान से निकालता है तो उसकी पत्नी उसकी बाहों में ही दम तोड़ देती है। तब उसे अपनी गलतियों का अहसास और पछतावा होता है।
यह अत्यंत मार्मिक और मानवीय विडंबना की कहानी है, जिसमें जमींदार का ‘कन्फेशन’ ही इस कहानी को उत्कर्ष पर ले जाता है। यह लेखक के मानवीय सोच को रेखांकित करता है। लेखक एक जमींदार के भीतर भी दबी-बची उसकी संवेदनशीलता को रेखांकित करता है। पत्नी के मरने के बाद उसे अपने दुष्कर्म का अहसास होता है कि वह अब तक अपने जीवन में वह कैसा पाप करता रहा और पत्नी को छलता रहा, लेकिन पत्नी अपने पति की इस दैहिक भूख को मिटाने के लिए अपने आभूषण सहर्ष देती रही। नैतिकता और अनैतिकता के बीच के द्वंद्व और पश्चाताप के स्वीकार ने इस कहानी को एक ऊंचाई प्रदान की है।
हालांकि आज के स्त्री विमर्श की दृष्टि से यह कोई प्रगतिशील कहानी नहीं है। इसमें स्त्री का मौन ही दिखाया गया है और उसके द्वारा शोषण का प्रतिकार नहीं किया गया। बल्कि उसे एक त्यागमयी, लाचार, बेबस महिला के रूप में दिखाया गया है।
लेकिन क्लासिकल साहित्य और कहानी कला की दृष्टि से विचार करें तो 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में जब हिंदी कहानी का विकास हो रहा था, तब ऐसी उच्च स्तरीय कहानी लिखना कम आश्चर्यजनक नहीं। जबकि राजा की उम्र तब महज 21 वर्ष की थी। इस उम्र में हिंदी के शायद ही किसी लेखक ने इतनी स्तरीय कहानी लिखी हो जो सौ साल बाद भी जिंदा है। इस कहांनी को पढ़कर लगता है राजा जी बहुत तैयारी के साथ साहित्य-जगत में आये थे।
दस सितंबर 1890 में बिहार के विक्रमगंज इलाके में सूर्यपुरा स्टेट में जन्मे राजा जी हिंदी के उन तीन प्रमुख शैलीकारों में से एक थे, जिन्होंने बीसवीं सदी के आरम्भ में हिंदी गद्य का विकास किया था औऱ उसकी छटा विखरने का काम भी किया था।
उतर प्रदेश के लेखकों में गद्य की वह शैली नहीं दिखती जो शिवपूजन सहाय, रामबृक्ष बेनीपुरी और राजा जी मे दिखाई देती है। तीनों की अलग अलग खुशबू और अलग रंग हैं। तीनों गहरे मित्र और जनता के लेखक। तीनों गांधीवाद से प्रभावित और गरीब गुरबों की चिंता करनेवाले सेक्युलर लेखक। राजा जी इन तीनों में सबसे बड़े थे पर वे सबसे मित्रवत थे तथा समकालीन भी।
शिवपूजन बाबू से तो उनक़ा परिचय आरा से ही था और आजीवन रहा। अलबत्ता शिवपूजन बाबू की नजरों और संपादन में ही राजा जी का समस्त साहित्य छपा। यह बात राजा जी के पुत्र ने भी अपने संस्मरण में स्वीकार किया है। दोनों का स्कूली जीवन आरा में बीता। शिवपूजन जी की नजर में राजा जी हिंदी उर्दू बंगला ब्रजभाषा के गहरे विद्वान भी थे। राजा जी के पिता और पितामह दोनों कवि थे। इस तरह राजा जी को साहित्य विरासत में मिली थी लेकिन उनके लिए राजपाट से अधिक साहित्य महत्वपूर्ण था और वे जीवन भर साहित्य की सेवा करते रहे।
आरा में ही राजा राधिकारमण प्रसाद जी की शादी हुई। यह बहुत कम लोग जानते हैं कि जब गांधी जी आरा आये थे तो उनकी जन्मसभा के आयोजन की जिम्मेदारी राजा जी ने ही निभाई थी। वे डिस्ट्रिक बोर्ड के चेयरमैन थे।
अंग्रेजों ने राजा जी को गांधी जी का साथ देने पर नौकरी से हटा दिया था। लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की।
बाद में गांधी जी ने उन्हें हरिजन सेवक संघ का प्रमुख बना दिया था।
राजा जी को राजेन्द्र बाबू व्यक्तिगत रूप से जानते थे। उनसे उनकी मित्रता थी। उनकी हस्ती का अंदाज़ इस बात से पता चलता है कि जब 1950 में आरा नागरी प्रचारिणी सभा की ओर से राजेन्द्र बाबू को राजेन्द्र अभिनंदन ग्रन्थ भेंट किया गया तो उस समारोह के अध्यक्ष राजा जी ही थे। और उस अभिनंदन ग्रंथ के संपादक शिवपूजन बाबू थे। जब 1950 में मार्च में ‘नई धारा’ का शुभारंभ हुआ तो संपादक बेनीपुरी जी थे और सहायक सम्पादक वीरेंद्र नारायण थे जो शिवपूजन जी के दामाद थे। वे 1942 के आंदोलन में रेणु के साथ जेल गए थे। 1955 में बेनीपुरी और वीरेंद्र नारायण ने अपनी व्यस्तताओं से नई धारा छोड़ दिया।नई धारा के लोकार्पण समारोह का उद्घटान बाबू श्रीकृष्ण सिंह ने किया था।

अपने समय के कांग्रेस के बड़े बड़े राज नेताओं से मित्रता के बावजूद वे राजनीति में नहीं गए। चाहते तो राज्यसभा में जा सकते थे जैसे दिनकर गए। अलबत्ता राजा जी के एक बेटे जरूर कांग्रेस से राज्य सभा के सदस्य रहे पर राजा जी का मन साहित्य सेवा में ही लगता था। इसलिए उन्होंने अशोक प्रेस स्थापित किया और नई धारा वहीं से निकलती रही।
राजा जी कहानीकार या उपन्यासकार ही नहीं नाटककार भी थे। कोलकत्ता में उनके पिता टैगोर के पड़ोसी थे। जब 13 साल की उम्र में राजा जी के पिता नहीं रहे तो कोर्ट ऑफ वॉर्ड हो गया था।
राजा जी हिंदी-उर्दू की एकता के हिमायती थे और उनके गद्य में उर्दू की खुशबू प्रेमचन्द से भी अधिक थी। उनकी बारे में कहा जाता है कि वे फ्लॉवरी भषा लिखते थे। वे भाषा को गुलदस्ता के रूप में पेश करते थे।
यह दुर्भाग्य है कि बिहार के पुराने आलोचकों नागेश्वर, खगेन्द्र ठाकुर, नंदकिशोर नवल, सुरेंद्र चौधरी, चंद्रभूषण तिवारी आदि ने भी उनक़ा मूल्यांकन नहीं किया। इतना ही नहीं बाद में रविभूषण और रेवती रमण आदि ने भी नहीं लिखा।
तीस साल पहले वीरेंद्र नारायण ने राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह की जन्मशती के मौके पर साहित्य अकादमी के लिए एक मोनोग्राफ लिखा और कुछ साल पहले डॉक्टर मंगलमूर्ति जी ने उनक़ा एक संचयन साहित्य अकादमी के लिए सम्पादित किया एवम कमलानंद झा ने राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के लिए उनकी कहानियों का एक चयन संपादित किया और एक महत्वपूर्ण भूमिका लिखी। अन्यथा अबतक उनकी सुध किसी ने नहीं ली थी।
राजा जी की पत्रिका से विजय मोहन सिंह भी जुड़े थे। कमलेश्वर ने भी इसका एक अंक संपादित किया था लेकिन पत्रिका को इसके बाद कोई योग्य संपादक नहीं मिला।
अगर उनकी रचनावली नए सिरे से संपादित होकर निकले और उनके महत्व को रेखाँकित करते हुए कोई योग्य व्यक्ति संपादित करें तो राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह पर लोगों का, शोधार्थियों का ध्यान जाए। ठीक उसी तरह जिस तरह नलिन विलोचन शर्मा का अबकाम लोगों के ध्यान में आया है।
राम-रहीम के लेखक राजा जी ने प्रेमचन्द युग और उसके बाद तक अपना साहित्य लिखा लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी आलोचना के केंद्र में प्रेमचन्द प्रसाद और निराला ही थे और वही रहें। इसलिए उस दौर के अन्य लेखकों के योगदान पर लोगों की निगाह नहीं जा सकी। राजा जी ही नहीं कौशिक जी, उग्र, शिवपूजन सहाय और बेनीपुरी का सम्यक मूल्यांकन आजतक नहीं हुआ है। साहित्य की दुनिया मे इस तरह के हादसे होते रहते हैं। उम्मीद है राजा जी का मूल्यांकन अब जल्द ही होगा।