“यह फर्क न पड़ने वाला समय है जिसमें चकाचौंध और क्षण में जीने के भाव भरे हैं। जहां-जहां चमक नहीं है या चमक की संभावना नहीं वे सब अर्थहीन हो चुके हैं और यह रुकने का नाम नहीं ले रहा है।”
उपर्युक्त पंक्तियाँ हंस मार्च 2025 में प्रकाशित युवा कहानीकार आलोक रंजन की कहानी ‘तलईकूत्तल’ के लगभग मध्य से उद्धृत हैं। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष जिन दो कहानियों को राजेन्द्र यादव हंस कथा सम्मान प्राप्त हुआ है, यह कहानी उनमें से एक है। हर भाषा और काल की कहानियों में समय के विवरण मिलते रहे हैं। पर उदय प्रकाश के बाद की हिन्दी काहानियों में समय को संबोधित ऐसे विवरण बहुतायत में दिखाई पड़ते हैं। कई बार कहानियों से सीधा संबंध नहीं होने के बावजूद, कुछ कहानीकार इसे कहन की आधुनिक तकनीक (पढ़ें फैशन) की तरह पेश करते रहे हैं। यह सुखद है कि आलोक रंजन इस कहानी में ऐसा नहीं करते और समय का यह विवरण कहानी का अभिन्न हिस्सा बनकर सामने आता है। विगत पच्चीस-तीस वर्षों का कालखंड, जिसे मैं भूमंडलोत्तर समय कहता हूँ, की तीन प्रमुख विशेषताओं- गति, फ्यूजन और संकुचन को मैंने बार-बार रेखांकित किया है। इस संदर्भ में यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि गति के समानान्तर ठहराव की मौजूदगी इस समय को दो परस्पर विपरीत अभिलक्षणों के बीच सांस लेते कालखंड की तरह भी रेखांकित करती है। ‘तलईकूत्तल’ से उद्धृत उपर्युक्त पंक्तियों में गति और ठहराव की दुहरी मौजूदगी, जो लगभग आद्योपांत इस कहानी में भी उपस्थित है, को समझा जाना चाहिए।
तमिलनाडु के कुछ इलाकों में अशक्त और अवांछित बुजुर्गों की हत्या की एक पुरानी कुप्रथा प्रचलित है, जिसे ‘तलईकूत्तल’ कहा जाता है। एलीकुट्टी, जिसका जीवन इस कहानी के केंद्र में है, इसी अनैतिक और बर्बर परंपरा का शिकार होती है। यूं तो शीर्षक और परिणति दोनों ही इस कहानी को इस कुप्रथा को उद्घाटित करनेवाली कहानी की तरह ही रेखांकित करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में वर्ग और जेंडर की दोहरी मार झेलती स्त्री का जीवन तथा पूंजी और धर्म की गठजोड़ के बीच पानी के सूखते स्रोतों की चिंताएँ कथानक का स्वाभाविक हिस्सा बनकर पाठकों के समक्ष उपस्थित होती हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा हिन्दी कहानी के कथानक का भौगोलिक विस्तार करने के लिए इस कहानी को रेखांकित किया जाना चाहिए। द्रष्टा और भोक्ता के मध्य स्थित अनुभूति-अंतरालों के कारण उत्पन्न किंचित रचनात्मक सीमाओं के बावजूद, मेरी सीमित पढ़त में संभवतः पहली बार हिन्दी कहानी ने संपूर्णता में दक्षिण भारत की रुख की है। हालांकि आलोक रंजन की दो-एक अन्य कहानियों में भी दक्षिण का आस्वाद मिलता है, पर यह कहानी उन कहानियों की सीमाओं का भी कुछ हद तक विस्तार करती है। किसी उपन्यास या कहानी में यदा कदा प्रसंगवश उपस्थित होते रहे कुछेक दक्षिण भारतीय संदर्भों की सीमा का अतिक्रमण करते हुये हिन्दी कहानी के परिसर का यह विस्तार निश्चय ही स्वागत योग्य है।
एलीकुट्टी के जीवन संघर्ष किसी भी आम स्त्री के जीवन संघर्षों से अलग नहीं हैं, पर उसकी जिजीविषा, उसका अनथक श्रम और सतत संघर्ष का जज्बा उसे आम स्त्रियों से अलग भी करते हैँ। एलीकुट्टी के दैनंदिन जद्दोजहद से शुरू होकर उसकी आनुष्ठानिक हत्या तक फैली इस कहानी को, जिसे लेखक ने उसके माध्यम से ही फ्लैशबैक की तकनीक के सहारे पाठकों तक पहुंचाया है, मोटे तौर पर तीन हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। पहला हिस्सा वह, जिसमें त्वचा को झुलसाने वाली गर्मी के दिनों में घर के कामकाज निबटाकर एलीकुट्टी साइकिल पर टोकरी लादकर फूल बेचने के लिये शहर (मदुरै) जाती-आती है। दूसरा हिस्सा वह, जहाँ गाँव में बारिश के लिए हो रहे यज्ञ में उसके मुहल्ले के हिस्से के पानी के टैंकर भेज दिए गए हैं। अपने हिस्से का पानी लेने वह कुछ अन्य स्त्रियों के साथ यज्ञ स्थल तक जाती है और वहीं हुए आक्रमण और भगदड़ के बीच फिसलकर कमर में गंभीर चोट का शिकार हो जाती है। तीसरा और अंतिम हिस्सा वह, जिसमें नेताजी से मुआवजा मिलने के बाद अस्पताल से उसका पति उसे घर ले जाता है और कुछ ही दिनों बाद बढ़िया इलाज के बहाने किसी और गाँव ले जाकर कुटुम्बों के साथ मिलकर उसकी अनुष्ठानिक हत्या कर देता है।
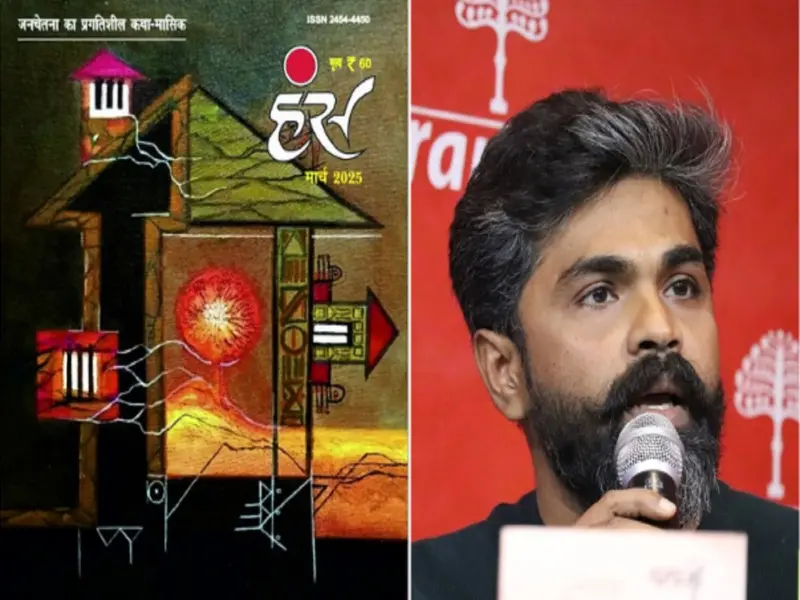
यूं तो घटनाओं की दृष्टि से देखें तो कहानी बहुत सामान्य मालूम होती है, लेकिन इन सामान्य सी घटनाओं को उनकी परिणति तक पहुंचाने में कहानी जिन बाह्यांतरिक प्रक्रियाओं से गुजरती है, उसकी सघन वर्णनात्मकता से ही इस कहानी ने अपने लिए प्राण वायु अर्जित किया है। इस क्रम में आलोक रंजन पानी की कमी या किल्लत का जो प्रतीकात्मक इस्तेमाल करते हैं, वह काबिले तारीफ है। मदुरै शहर के बीचोंबीच स्थित वैगई नदी का सूखना हो कि पानी के अभाव और प्यास से सूखता एलीकुट्टी का कंठ कहानी में एकाधिक बार आते हैं और हर बार दोनों कब और कैसे एक हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। पर्यावरण संकट और सूख कर कांटा हुई नदी की बात करते-करते स्त्री जीवन पर आरोपित शुष्कता की ओर संकेत कर जाना और स्त्री जीवन में व्याप्त रिक्तियों पर बात करते-करते प्राकृतिक आपदाओं की पड़ताल कर जाने की पारस्परिकता जिस सहजता से यहाँ घटित होती है, प्राणी और पर्यावरण की अन्योन्याश्रयिता को समझने के कई सूत्र उसमें सन्निहित हैं। हाँफती साँसों के साथ साइकिल खींचती एलीकुट्टी के पसीने का जैसा मारक और अचूक इस्तेमाल इस कहानी में हुआ है, उसे सीधे कहानी की भाषा में ही देखा जाना चाहिए-
“एली को अपनी साइकिल स्वयं घसीटनी है। पता नहीं शरीर में इतना पानी कहाँ से आ जाता है कि पुल पर चढ़ते-चढ़ते उसकी पीठ और चेहरे पर पसीना दिखाई देने लगता है। उम्र के इस पड़ाव पर दर्द का झलक जाना तो उसे समझ आता है, लेकिन इस सूखे में उसके चेहरे पर पानी का आ जाना पानी की बर्बादी है।”
सत्ता धर्म की हो या राजनीति की या फिर पूंजी की हो या पितृसत्ता की, कुछ बाहरी अंतरों के बावजूद, इन सबके हाथ एक ही दस्ताने में होते हैं। विभिन्न सत्ताओं के गुपचुप गठजोड़ और शोषितों पर उसके समवेत प्रभाव को यह कहानी बहुत बारीकी से अभिव्यंजित करती है। शोषित यदि स्त्री हुई तो सत्ता की मार और ज्यादा गहरी और परतदार हो जाती है-
’अम्मा गर्मी तो सच में बहुत ज्यादा है। इस बार तो पानी बरसने का नाम ही नहीं ले रहा है। मदुरै के सारे पेड़ सूख जाएंगे इस बार।’
‘तुम्हें पेड़ों की पड़ी है, मेरे घर में आज पानी नहीं आया तो इडली बनाने के लिए भी पानी नहीं है।’
‘पर अम्मा तुम्हारे उधर तो सुना है पानी के लिए यज्ञ हो रहा है। देवता खुश होकर वर्षा से खेत खलिहान भर देंगे।’
‘बेटी जिनके खेत है देवता अभी उन्हीं के हैं। उनके देवता उनकी बात सुनकर उनके लिए पानी बरसाएंगे, यज्ञ से हमें क्या फायदा!’
उपर्युक्त प्रसंग में एलीकुट्टी के शब्द ‘उनके देवता उनकी बात सुनकर उनके लिए पानी बरसाएंगे’ सुनते हुए प्रजातन्त्र की सर्वमान्य परिभाषा ‘जनता का, जनता के लिये, जनता के द्वारा,’ की याद हो आना सहज है। दरअसल इन दोनों शब्दावलियों के इसी सहज वैषम्य में इस कहानी और लोकतंत्र दोनों की विडंबना के सूत्र छिपे हुए हैं।
ऊपर की पंक्तियों में जिन खासियतों का जिक्र मैंने किया है, वही इस कहानी और ऊपर वर्णित इसके दो हिस्सों की ताकत है। लेकिन जैसे-जैसे कहानी तीसरे हिस्से, खासकर अपने अंत की तरफ बढ़ती है, उसकी बहुपरतीयता किंचित छीजने लगती है। वैगई नदी पर बने पुल की ढाल से बिना पैडल मारे नीचे उतरना भले एलीकुट्टी के जीवन का सबसे खूबसूरत पल हो, पर तीसरे हिस्से के उत्तरार्द्ध में कहानी जिस तेजी से अपने अंत यानी एलीकुट्टी के ‘तलईकूत्तल’ की तरफ बढ़ती है, वह बहुत हद तक कहानी को एकरैखिक ढलान की तरफ ले जाता है। भोक्ता की संवेदनभेदी दृष्टि को पीछे कर, पर्यटकीय प्राप्ति में ही यथार्थ के उद्घाटन को सीमित कर देना, मेरी दृष्टि में इसका एक बड़ा कारण है।
यह कहानी तमिल समाज की इस कुप्रथा के हवाले से हिन्दी के पाठकों का परिचय एक नितांत नए यथार्थ से कराती है, जो निःसंदेह बहुत त्रासद है। लेकिन हिंदीतर समाज, खास कर तमिल और मराठी भाषा साहित्य व चलचित्र से सम्बद्ध पाठक और दर्शक इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि विगत कुछ सालों में इस विषय पर कई फिल्में बनी हैं। नाटक भी मंचित हुए हैं। तमिलनाडु के पिछड़े इलाकों में घटित होनेवाली ऐसी कई घटनाओं और उसके प्रति लोगों के प्रतिरोध की खबरें भी पत्र-पत्रिकाओं में साया हुई हैं।
यह भी दिलचस्प है कि प्रख्यात तमिल फ़िल्मकार जयप्रकाश राधाकृष्णन ने 2023 में ‘तलईकूत्तल’ नाम से ही एक फिल्म बनाई थी जो खासा चर्चित भी हुई। इस फिल्म में शुरुआती प्रतिरोध के बावजूद ससुराल वालों के भारी दबाव में बेटा अपने बीमार और असहाय पिता की अनुष्ठानिक हत्या को अंजाम तो दे देता है, लेकिन फिल्म के अंतिम दृश्य में पिता की अस्थियों पर लगाए गए बरगद के पास अपनी बेटी के साथ जिस सुकून और बेचैनी के दुकूल में वह दिखाई पड़ता है, उसमें उसका अपराधबोध और पश्चाताप दोनों शामिल है।
सुपरिचित मराठी नाटककार रवीन्द्र इंगले नावरेकर द्वारा इसी शीर्षक से रचित नाटक की कई प्रस्तुतियाँ लगभग तीन वर्ष पूर्व महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में हुई थीं। उस नाटक में जिस तरह ट्रांस जेंडर और समलैंगिक समुदायों से जोड़कर इस पुरानी प्रथा का एक आधुनिक पाठ तैयार किया गया है, उसने इस प्रथा के प्रभाव क्षेत्र का रचनात्मक विस्तार किया है।
प्रसंगवश यहाँ 2019 में प्रदर्शित दो अन्य तमिल फिल्मों ‘केडी एंगिरा करुप्पुदुरई’ (निर्देशक – मधुमिता) और ‘बाराम’ (निर्देशक- प्रिया कृष्णस्वामी) का उल्लेख भी जरूर किया जाना चाहिए, जो समाज में बुजुर्गों की असहाय और उपेक्षित जीवन दशा, ‘तलईकूत्तल’ के लिए पारिवारिक दबाव और कुटुम्बों की बेरुखी के बीच इसके सामाजिक प्रतिरोध की भूमिका भी तैयार करती हैं। ‘केडी एंगिरा…’ फिल्म के अंत में परिवारवालों की बदनीयत को भाँप कर करुप्पुदुरई का घर छोड़कर भाग जाना हो या कि बाराम फिल्म में करुप्पासामी के अंतिम संस्कार के वक्त एक बूढ़ी औरत का यह दावा कि उसकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं, बल्कि एक सुनियोजिय हत्या थी, को इन्हीं संदर्भों से जोड़कर देखा जाना चाहिए।
यह भी गौरतलब है कि उपर्युक्त तीनों तमिल फिल्मों के बुजुर्ग पात्र मुथु (तलईकूत्तल), करुप्पुदुरई (केडी एंगिरा करुप्पुदुरई) और करुप्पासामी (बाराम) एकाकी पुरुष हैं और उनके बेटों पर उनकी अनुष्ठानिक हत्या करने का पारिवारिक-सामाजिक दबाव है। इन फिल्मों से अलग, आलोक रंजन की कहानी में एक स्त्री इस अनुष्ठानिक हत्या यानी ‘तलईकूत्तल’ का शिकार होती है। एलीकुट्टी निःसन्तान है और हत्या की साजिश उसका पति रचता है, वह पति जो शराबी, नकारा और गैरजिम्मेदार है। मुथु (तलईकूत्तल), करुप्पुदुरई (केडी एंगिरा करुप्पुदुरई) और करुप्पासामी (बाराम) की तुलना में एलीकुट्टी की चुनौतियाँ दोहरी हैं। परस्पर स्वीकार और अस्वीकार के शुष्क जीवन के बीच एक दूसरे के प्रति अक्रिय रहते हुए भी वह पति की उपेक्षा और जिम्मेवारी दोनों का संयुक्त बोझ ढोने को विवश है। कहानी के केन्द्रीय बुजुर्ग पात्र के रूप में पुरुष की जगह एक स्त्री को रखने का लेखकीय निर्णय इस कहानी को इन फिल्मों की तुलना में ज्यादा चुनौतीपूर्ण तो बनाता है, लेकिन आलोक रंजन की सीमा यह है कि अंत तक आते-आते वे अपनी कहानी को स्थूल यथार्थ के प्रकटीकरण का माध्यम भर बनाकर छोड़ देते हैं। कहानी के अंत में लगभग मृत्यु के दरवाजे पर खड़ी एलीकुट्टी अपने पति को देखकर थूकना चाहती है। थूकने की इस अंतिम चाह को लेखक ने उसके प्रतिरोध की तरह दर्ज करने की कोशिश की है, लेकिन संवेदना के बृहत्तर फलक पर प्रतिरोध दर्ज करने के लिए यथार्थ की प्रस्तुति से दो कदम आगे उसकी पुनर्रचना की जरूरत थी। यथार्थ की पुनर्रचना के लिए स्थूल यथार्थ का अतिक्रमण करना होता है, जिसका किंचित अभाव इस कहानी में दिखाई पड़ता है।
विवेच्य कहानी की एलीकुट्टी और ‘बाराम’ की करुप्पासामी की अनुष्ठानिक हत्याओं के घटनाक्रम में एक खास तरह का साम्य है। अपने हिस्से का पानी हासिल करने के लिए संघर्ष करते हुए एलीकुट्टी की कमर में चोट लगी थी, वहीं करुप्पासामी जो पेशे से एक नाइट वाचमैन है, की एक सुबह, ड्यूटी से लौटते हुए सड़क हादसे में कूल्हे की हड्डी टूट जाती है। घायल होने के बाद एलीकुट्टी एक अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन उसका पति उसे पहले घर और फिर किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराने के बहाने गाँव ले जाकर उसकी हत्या को अंजाम देता है। दिलचस्प है कि करुप्पासामी का भतीजा उसका ऑपरेशन शहर के अस्पताल में कराना चाहता था, लेकिन उसका बेटा पुश्तैनी वैद्य से इलाज कराने के नाम पर उसे गाँव ले जाता है और कुछ दिन बाद वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। घटनाक्रमों की ऊपरी एकरूपता बावजूद इन दोनों कृतियों के बीच एक लंबा फासला है। जैसा कि पहले भी कहा गया है, विवेच्य कहानी के अंत में जहाँ एलीकुट्टी अपने पति के प्रति घृणा से भर उठती है, वहीं ‘बाराम’ फिल्म में करुप्पासामी के अंतिम संस्कार के वक्त एक बूढ़ी औरत सार्वजनिक तौर पर यह दावा करती है कि उसकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि हत्या की गई है। निजी घृणा और सार्वजनिक प्रतिकार का यह अंतर दरअसल दो रचनात्मक दृष्टियों का अंतर है। यथार्थ के अंकन और उसकी पुनर्रचना के अंतर को समझने के लिए भी इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती कथा अपनी परिणति तक आते-आते ‘बाराम’ में एक बृहत्तर सामाजिक चिंता से उत्पन्न प्रश्न और बेचैनी के रूप में प्रकट होती है, जबकि शुरुआत में बृहत्तर स्त्री समाज की चिंता करती कहानी ‘तलईकूत्तल’ अपने अंत तक पहुंचकर पति के प्रति एलीकुट्टी की घृणा में परिसीमित हो जाती है।
स्थूल यथार्थ के अनुभव-भूगोल का द्रष्टा भर होकर रह जाने की लेखकीय नियति एलीकुट्टी की चाहत को एक प्रभावी सामाजिक बेचैनी में तब्दील होने से रोकती है। परिणामतः हिन्दी पाठकों को यह कहानी एक अनजानी प्रथा से परिचित तो करवा देती है, लेकिन, इस अनुभव-यथार्थ की उन परतों तक भी नहीं पहुँच पाती, जिसका उत्खनन ऊपर वर्णित तमिल फिल्मों ने कुछ वर्ष पहले ही कर रखा है। बावजूद इस सीमा के, ‘तलईकूत्तल’ की भयावहता को स्त्री संवेदी दृष्टि से देख्नने की कोशिश इसे महत्त्वपूर्ण तो बनाती ही है। तलईकूत्तल को सिर्फ दक्षिण भारत या तमिलनाडु की समस्या की तरह देखना इस कहानी की प्रभाव-परिधि को परिसीमित करना होगा। अपने विस्तृत अर्थों में यह कहानी पूरे देश में बुज़ुर्गों की उपेक्षा और असुरक्षा की स्थिति और उसकी भयावहता की तरफ भी संकेत करती है। इसे समझे जाने की जरूरत है।


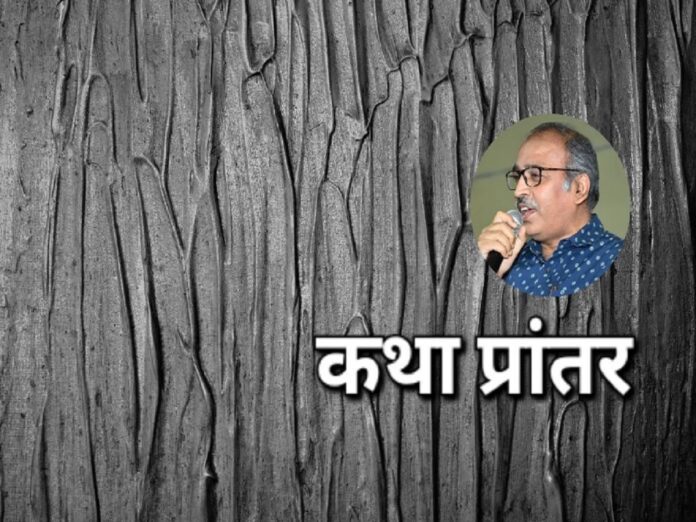
सम्यक विश्लेषण कहानी का
यह आलेख केवल आलोक रंजन की कहानी ‘तलईकूत्तल’ का मूल्यांकन नहीं करता, बल्कि हिंदी कहानी के बदलते परिदृश्य, स्त्री जीवन के संघर्षों और हमारे समय की त्रासदियों को गहरी संवेदनात्मकता और आलोचनात्मक दृष्टि से उद्घाटित करता है।
एलीकुट्टी यहाँ महज़ पात्र नहीं, बल्कि भारतीय स्त्री जीवन की सामूहिक छवि बन जाती है—उसका श्रम, संघर्ष और अंततः हत्या पितृसत्ता व पूंजी की अमानवीय संरचना को उजागर करते हैं। आलेख में पानी, प्यास और नदी की छवियाँ उसके जीवन से इस तरह जुड़ती हैं कि स्त्री और प्रकृति दोनों की सूखती नमी का बिंब एक साथ उभरता है।
समीक्षक कहानी की तुलना तमिल फिल्मों व नाटकों से करते हुए दिखाते हैं कि जहाँ फिल्में सामूहिक प्रतिरोध तक पहुँचती हैं, वहीं यह कहानी व्यक्तिगत घृणा तक सिमट जाती है। इसी से यह प्रश्न उठता है कि क्या साहित्य केवल यथार्थ का चित्रण करे या उसकी पुनर्रचना कर सामाजिक परिवर्तन में हस्तक्षेप भी करे।
भावनात्मक गहराई और बौद्धिक पैठ का यह संगम इस आलेख को हिंदी आलोचना की गंभीर परंपरा में एक महत्त्वपूर्ण और यादगार हस्तक्षेप बनाता है।
शुक्रिया उर्वशी जी!
मैंने यह कहानी नहीं पढ़ पायी थी लेकिन समीक्षा पढ़ने के बाद अब पढ़ूंगा। कथ्य एकदम अलग है।