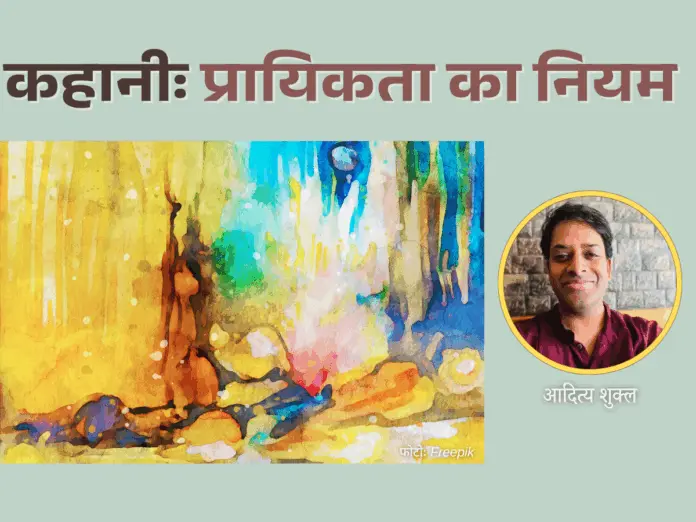वे सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे सूखे में बारिश की, भूख में रोटी की, विरह संतप्त प्रेमी अपने प्रेम की और जैसे ना जाने कैसे कैसे! उनकी आँखों की कोरों पर लदी हुई है एक अधूरी नींद। मानो सदियों से उन्हें नींद नहीं मिली है और आँगन भर में पसरी है उदासी, दुआर है उजाड़।
हरिहर भाई लकड़ी की एक पुरातन कुर्सी पर कई चादरों की परतें लपेटकर बैठे हुए हैं। वे थोड़ा भी हिलते हैं तो कुर्सी से चर्र चर्र की आवाज़ निकलती है.. फिर वे कुर्सी में ख़ुद को समेटकर ऐसे ख़ामोश हो जाते हैं मानो उन्हें कुर्सी में ख़ामोश बैठने की सजा मिली हो।उनका छोटा साँवला मुँह एक मटमैले ऊनी टोपे से ढँका हुआ है। पास में पुराने पलंग पर उनकी दोनों बेटियाँ असहाय बैठी हैं। पलंग के सिरहाने पर नीले रंग की कारीगरी है जो किसी बीत चुके युग से अब तक संरक्षित चले आए थे। उनकी पत्नी एक कमरे से दूसरे कमरे में बेचैनी से आ-जा रही थीं।
फ़ोन की घंटी बजी – ‘भुला देंगे तुमको सनम धीरे-धीरे..’
हरिहर भाई ने अपनी बेटी के फ़ोन की ओर एक तरेरती नज़र दौड़ायी। छुटकी ने जल्दी से फ़ोन उठा लिया।
‘कहाँ पहुँचे?
‘मुसैले के पेट्रोल पंप से भागलपुर वाला बायपास ले लेना।’ हरिहर भाई ने बताया।
बात ख़त्म होने के बाद हरिहर भाई ने बेटी से रिंगटोन बदलने के लिए कहा और वो अपने फ़ोन सेटिंग में हेरा गई।
बगल वाले कमरे से जोर से किसी के कराहने की आवाज़ आई। एक पल के लिए पूरी सृष्टि स्तब्ध हो गयी। घर में जो जहाँ था वहीं पर ठहर गया। विचार, बेचैनियाँ, सपने, डर सब कुछ। एक पल के लिए स्तब्ध! जनजीवन सिनेमा की रील अटक गई।अगले ही पल खट से फिर चल निकली और सब अपने-अपने काम में व्यस्त हो गए।
घर के मालिक रामभरोसे बरामदे में एक चौकी पर बैठकर कुछ कागज़ पत्तर देख रहे थे। काले रंग का एक कुत्ता चौकी के पाये के पास बैठा हर छोटी मोटी अनजान हरकत पर भौंक लगा रहा था। पास के कमरे में बैठा नीलेश परीक्षा की तैयारी में गणित के सवाल हल कर रहा था। गणित के सवाल हल करते हुए नीलेश ने अपनी अंजुरी में भरे हुए पासों अच्छे से हिलाकर बिस्तर पर गिरा दिया। ये रहा क्रमचय-संचय! फिर उसने किताब से ट्रैफिक लाइट के नियम को जोर-जोर से पढ़ना शुरू किया। उसके दोनों छोटे भाई बाहर नीम के पेड़ तले जाने कौन सा खेल खेल रहे थे। भैया क्रमचय-संचय पढ़ रहा है क्या – हीही! छोटू ने मझले से बोला कि नीलेश की क्लास के बच्चे कहते हैं कि वह गणित में कमजोर है और उसे आजतक क्रमचय संचय नहीं समझ आया।
जीवन अगर अपनी गति से चल रहा था तो चल रहा था मगर पृष्ठभूमि में एक प्रतीक्षा जारी थी।
रामभरोसे ने आवाज़ लगायी – ‘ऐ नीलेश, माई के पेंशनवा कैसे निकली ए महीना?’
‘बुझाते नईखे हो।’ एक उदासी दोनों के चेहरे पर उतर आयी थी। काला कुत्ता भौंक लगाते हुए सामने एक गड़हे की ओर दौड़ा। कुछ देर तक उस ओर भौंकता रहा। लौटकर धूल में पेट के बल लेट गया अपने चारों पैर ऊपर उठाकर।
छोटू ने मझलू से हिंदी में कहा – ‘भैया देखिए, कालू फिर से अपने पैर पर आसमान रोक रहा है!’
‘अगर वह आसमान ना रोके तो घर पर दुखों का आसमान फूट पड़ेगा’
‘हम कभी-कभी हिंदी क्यों बोलते हैं भैया?’
‘इस्कूल में सिखाया जाता है इसलिए।’
‘अगर हम अंग्रेजी सीखते तो खेलने के लिए धूल मिट्टी की जगह प्लास्टिक के सुंदर और महंगे खिलौने मिलते।’
‘नीलेश भैया बोल रहा था हम सभी किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं।’
‘मुझे नहीं मालूम मगर इतना मालूम है कि रजनीश भैया मोटरसाइकिल से आ रहे हैं। मुसैले से भागलपुर वाला बायपास लिए होंगे।’
‘चाचा, पापा से बात क्यों नहीं करते?’
‘चाचा ने पापा का कोई सामान चुरा लिया होगा।’
‘तुम मेरा कोई सामान चुरा लोगे तो मैं भी कभी तुमसे बात नहीं करूँगा।’
‘मैं भी नहीं करूँगा।’
‘गणित इतना मुश्किल क्यों होता है?’
‘क्योंकि हम लोग बुद्धू हैं।’
‘लेकिन इस्कूल का गणित मुश्किल होता है तो पैसा गिनना तो हम जानते हैं।’
‘मामा कहते हैं कि इस्कूल के गणित की हमारी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं।’
रजनीश ने आकर गेट के बाहर अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। रामभरोसे को प्रणाम करके घर के अंदर चला गया। रामभरोसे ने छुटकू मझलू को आवाज़ लगायी। दोनों दौड़कर घर में अंदर गए और चाचा के कमरे में झाँक आए। छुटकी, उसकी माँ और उसकी बहन छोटू मझलू की ताका झांकी से चिढ़ते थे।
हरिहर भाई कुर्सी पर बैठे-बैठे खंखार रहे थे। जनवरी का महीना। ठंडी का महीना तो है ही, ठंडी तासीर का महीना भी है। मानो महीने के ऊपर बर्फ जम गई हो। धूप निकलती नहीं, बर्फ पिघलती नहीं। बिना बर्फ के बर्फ से ढँका पहाड़ है जीवन इस महीने। हरिहर भाई जनवरी की गिनती कर रहे थे। लगता था साल जनवरी से शुरू होकर जनवरी पर ख़त्म होता और जनवरी है कि ख़त्म नहीं होती। रजनीश घर में सबसे मिलकर आ गया। सामने पड़े स्टूल को थोड़ा साफ़ करके बैठ गया। हरिहर भाई ने उसे देखा और बस सिर हिलाया। वे किसी भी विडंबना के सामने हमेशा सिर हिलाते थे। रजनीश समझ गया था। वह अपना फ़ोन निकाल कर उसमें कुछ देखने लगा। दो लोग थे और उनके बीच ख़ामोश बातचीत जारी थी। हरिहर भाई आजकल तब तक मुँह नहीं खोलते जब तक ख़ामोशी भाँय-भाँय करके ख़ाली जगह में बजने नहीं लगती थी। रजनीश के पास कहने के लिए कुछ होता नहीं था। रामभरोसे किसी काम के नहीं थे। घर कैसे चलेगा यही सवाल सब अपने मन ही मन करते थे। इस बार जवाब में जनवरी का पहाड़ उतर आया था। इस पहाड़ की दुर्गम वादियों में सब एक-एक करके बिलाते जा रहे थे। हरिहर की बेटियों के स्कूल नागा हो रहे थे। उन्हें अपने स्कूलों की याद आती थी। वहीं उनका समानांतर जीवन था। घर में तो कोई जीवन नहीं था। घर में सिर्फ़ खाना-पीना, पढ़ना, सोना, थोड़ा बहुत फ़ोन चलाना और डाँट खाना। मगर इस महीने वे सब गाँव में थे। यहाँ वे सब प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा के ऊपर कुंडली मारके हरिहर भाई बैठे थे। वे चुपचाप बैठे इशारे करते और उस हिसाब से घर को चलना पड़ता। रामभरोसे को भी क्योंकि उनसे कुछ होता नहीं था। मगर यह उन्हें मन ही मन नागवार गुजरता। हरिहर भाई की खंखार सुनकर रामभरोसे का खून जलने लगता। मगर वे भी अपना सिंहासन सम्भाल कर बैठे रहते। वे घर में राष्ट्रपति की तरह थे। कभी कभी वे बिलों को पारित होने से रोक लेते। हठी उनमें भी कम नहीं थी। हरिहर भाई प्रधानमंत्री थे। कैबिनेट उनकी थी। इस तरह यह रगड़-झगड़ चलती रहती थी जिसमें बच्चों का अपना स्वतंत्र पक्ष था। हरिहर भाई अवसाद की प्रतिमूर्ति थे। वे अपने भीतर के अँधेरे और बाहर के संघर्षों में उलझे रहते थे। उनकी जेब में पैसे तो रहते नहीं थे। अगर कोई ऐसी जेब होती जिससे जब चाहें जितना पैसा निकाल सकते तो शायद उनके अवसाद में कमी आती। पिताजी जब तक थे जीवन बेहतर था। पेंशन आती थी। अब माताजी को आती है मगर पहले से आधी। खर्चा पहले से कई गुना अधिक और दोनों भाइयों में हमेशा रहने वाली रगड़ ऊपर से। इन सबमें माताजी के पैसे कब किधर सुलट जाते हैं पता तो चलता नहीं। किसी महाकाव्य के पात्रों की तरह फैला हुआ लंबा परिवार था।
रजनीश ने नोटों की एक गड्डी निकाल कर टेबल पर रख दी थी।
नोटों की गड्डी देखने के लिए सब लोग एक-एक करके जमा होने लगे। बाहर के कमरे से दौड़कर सबसे पहले नीलेश आया मानो नोटों की गड्डी टेबल पर रखते ही उसे ख़बर हो गई हो। रामभरोसे धीमी चाल से आकर हरिहर भाई के कमरे के सामने एक पीढ़े पर बैठ गए। हरिहर की पत्नी, बेटियाँ, छोटू मझलू, रामभरोसे की पत्नी आकर उनकी बगल में बैठ गई और उनसे इधर उधर की बातें करने लगीं। हरिहर की बहन शर्मीली मटकते हुए आके रजनीश के पास खड़ी हो गईं। किसी ने कुछ नहीं कहा। किसी से नहीं। सब ख़ुद से बातें कर रहे थे। एक बार फिर से ख़ामोशी का पर्दा गिर गया। इस पर्दे से सब ढँक चुके थे और कोई किसी को नहीं देख पा रहा था। सबके अपने-अपने पर्दे थे। सब अपनी हाथों से पर्दे चढ़ाते गिराते। सब चाहते थे सबसे पहले हरिहर भाई अपने पर्दे का शटर उठाएँ। वे रह रह कर सिर्फ़ खँखार देते। गड्डी देखकर लगता था इसमें कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी। कुछ कामचलाऊ रकम थी। जिससे नीलेश और हरिहर भाई सबसे अधिक निराश थे। उन्हें अधिक रकम की जरूरत थी। हरिहर भाई ने आख़िरकार खामोशी तोड़ते हुए नीलेश को पैसे गिनने का इशारा कर दिया। नीलेश ने गड्डी उठाई और उसे ताश के पत्तों की तरह फेंटने लगा। छोटू ने मझलू को फेंटते देख हरिहर भाई नाराज़ हुए और नीलेश ने पैसों की गंभीरता से गिनती कर दी। पाँच सौ के उन्यासी नोट, सौ के तैंतीस, पचास के पचपन और दस के पिचहत्तर। कुल जमा छियालीस जमा तीन हज़ार रुपये। बस? इतना ही! सब सोचने लगे और सब उसमें से कितना उसके हिस्से आयेगा इसका गणित लगाने लगे। एक बटा छियालीस हज़ार तीन सौ। नहीं सौ बटा छियालीस हज़ार तीन सौ, नहीं हज़ार बटा छियालीस हज़ार तीन सौ। कुल जमा पचास हज़ार भी नहीं थे गड्डी में। इतने में क्या होगा। इतने सवाल रजनीश की दिशा में बढ़ने लगे थे। वह पलंग पर थोड़ा सिकुड़ कर बैठ गया।
इतना ही पैसा अकाउंट में बचा था मामा। अब ना मेरे पास और ना मम्मी के पास एक साबुत रुपया बचा है।
इतने में क्या होगा? रामभरोसे ने कहा।
दीदी ने तो इतना भी दे दिया, तुमसे कुछ होगा कि नहीं होगा? हरिहर ने चिढ़ते हुए कहा।
घर तो मैं ही चला रहा हूँ कि तुम वहाँ क़स्बे में बैठकर यहाँ चलाते हो।
लड़ो मत, शर्मीली ने कहा।
लड़ो मत, रजनीश ने कहा।
ठीक है हम नहीं लड़ेंगे, छोटू मझलू ने कहा। छियालीस हज़ार में क्या होगा यह नीलेश और हरिहर की चिंता थी। दोनों भाइयों में कहीं फिर से बहुत लड़ाई ना हो जाये ये दोनों बहुओं की चिंता थी। पास के कमरे से किसी के पुकारने की आवाज़ आई। एक ऐसी पुकार जिसमें शारीरिक दर्द की अभिव्यक्ति थी। बहुएँ उस कमरे की ओर चली गईं। बस छियालीस हज़ार है यह किसी ने किसी को किसी से कहते हुए सुना।
छियालीस हज़ार में नीलेश एक सेकंड हैंड स्कूटी ले सकता था। उसने देख रखा था। स्कूटी का मालिक पचास हज़ार माँग रहा है लेकिन थोड़ी बहुत जद्दोजहद करके पैंतालीस पर राज़ी किया जा सकता है। अगर पैंतालीस में एक स्कूटी मिल जाये फिर भी एक हज़ार बच जाएगा। जिसमें वह अपनी पसंद का एक जीन्स या एक जूता तो ले सकता था। छियालीस हज़ार उसकी अपनी जरूरतों के लिए पर्याप्त थे। लेकिन जिस मद में खर्च के लिए यह बहुप्रतीक्षित नगद आज कमरे की टेबल पर नज़र आ रहा है उसके लिए छियालीस हज़ार कुछ नहीं है। हरिहर भाई की जितनी भी समस्याएँ थीं उनके लिए छियालीस हज़ार को छियालीस से गुणा करके अगर कुछ पैसे मिल जाते तो भी शायद कम पड़ते। नीलेश ने गणना की – इक्कीस लाख रुपये। चाचा, चाचा इक्कीस लाख में तो अपना सारा काम हो सकता है। नहीं हो पाएगा, रामभरोसे ने कहा। बच्चों के गणित की सीमा होती है हरिहर ने सोचा।
सबने सबसे पहले अपने-अपने हिस्से में छियालीस हज़ार का गणित किया। सबके मन थोड़ी देर के लिए प्रफुल्लित हुए। फिर उन्हें याद आया कि ये छियालीस हज़ार किस मद में लगेंगे। फिर झुंझलाहट हुई। धीरे-धीरे झुंझलाहट बदल गई उदासी में। नोट की गड्डी टेबल पर आराम फ़रमा रही थी। नीलेश एक नॉयलॉन के बैग में पैसे को भरने लगा। उसने सोचा अगर इसमें से वह पचास रुपये निकाल ले तो? तीन सौ में से पचास गए तो कितने? इससे बाक़ी खर्चे पर क्या ही प्रभाव पड़ेगा। मगर उसने नोट नहीं निकाली। बैग की चेन लगते ही रामभरोसे उठकर बाहर की ओर चल दिए। उनकी पत्नी रसोई की ओर। हरिहर भाई के कमरे में लगा मजमा बिखरने लगा। रजनीश भी उठकर बाहर चला गया। अपनी पुरातन कुर्सी पर रजनीश भाई अकेले बच गए। अँधेरा घिरने लगा था। सूरज तो निकलता नहीं था इस पहाड़ जैसे महीने में। दिन रात के बीच बदलाए उजाले का एक छोटा चक्र रोज पूरा होता था और लोग अपनी-अपनी रजाई कंबल पकड़ लेते थे। ठंडे अँधेरे की चादर ओढ़े इस छोटे से हलचल भरे घर में चुप्पी पसर जाती थी। अवसाद का शैतान आँगन में भाँय-भाँय करके चिग्घाड़ने लगता था। उससे लड़ने के लिए हरिहर भाई बीच-बीच में खँखार देते।
छियालीस हज़ार रुपये तितली अम्मा के इलाज के लिए कम थे, कम नहीं बहुत कम थे।
उनका नाम ही तितली पड़ गया था। जब उन्हें पहली बार पता चला चला कि तितलियाँ भी कीट-पतंग होती हैं, कई दिन तक खाना नहीं खाया। दिन-दिन भर चुपचाप खिड़की से बाहर की ओर देखती रहतीं। खेत खलिहानों में, फूलों पौधों पर, टेम्पुओं के पीछे, कोहड़े के फूलों पर, किसी दिवाली के बच्चे हुए दीयों में इकट्ठे बारिश के पानी पर, हर जगह तितलियाँ मंडराती थीं। और तबसे पहली बार जब उन्होंने तितली का नाम सुनकर कई दिन के लिए खाना नहीं खाया, उन्हें बार-बार खाना छोड़ देने की आदत विकसित कर ली थी। वे आए दिन किसी बात पर नाराज़ होकर भूख हड़ताल पर बैठ जातीं। घर के आधे से अधिक व्यंजन उन्हें नापसंद थे। फल फूल दूध जूस जैसी चीजें उन्हें नापसंद थीं।
वे तितली नाम से पली-बढ़ीं और ज़िंदगी पर लार्वा रह गईं।
और अब बुढ़ापा। ज़िंदगी भर की नासमझियाँ और लापरवाहियाँ। शारीरिक कष्ट का कुल जोड़ जमा। वे अब एक कमरे में लेटी लेटी थोड़ी-थोड़ी देर पर कराहती रहती हैं। खाना वे अब भी नहीं खाना चाहतीं। सेब देने पर उसे मुँह में रख लेतीं और मौका मिलते ही मुँह में उँगली डालकर उसे निकाल फेंकतीं। दूध पीना नहीं, दही खाना नहीं। पौष्टिक खाद्य क्या होता है? इन्होंने ना कभी जाना और ना ही उन्हें वो कभी मिला।
लोग कहने लगे थे कि वे अब मृत्यु शैया पर हैं।
गांव में सब कहने लगे थे कि जिस दिन से वे गिरी हैं और अपना कूल्हा तोड़कर बिस्तर पकड़ा है, उनके बेटे अब बस बैठकर उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें अस्पताल ना ले जाना पड़े। वे अस्पताल जाना भी नहीं चाहतीं। जब उनके मोतियाबिंद की सर्जरी हुई थी, वे ठीक होने के दस दिन बाद तक रोती रहीं कि उन्हें अस्पताल क्यों ले जाया गया। नर्स ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया। अस्पताल से घर आते समय गाड़ी में बैठे-बैठे चक्कर आया, उल्टी आई। मैं अस्पताल नहीं जाऊँगी, वे कहतीं। वे अस्पताल नहीं जातीं। पेट में हमेशा कोई ना कोई दिक्कत रहती थी। उल्टियाँ, कब्ज़ आम बात थी। मैं अस्पताल नहीं जाऊँगी, वे कहतीं। और भला उन्हें अस्पताल ले कौन जाता! उनके दोनों बेटे ठन ठन गोपाल थे। उन्हीं के नाम मात्र पेंशन से पूरा घर जैसे-तैसे चल रहा था। पेंशन आते ही महीने भर का राशन पानी गल्ला उधारी और किसकी जेब में कितने पैसे बचते? कभी कभी लगता कहीं वे इसलिए भी तो अस्पताल जाने से मना करती कि वे जानती थीं, मन ही मन, अस्पताल के तो पैसे किसी के पास हैं नहीं।
संभव है वे लार्वा से तितली बन गई हों, कभी किसी को जताया नहीं और अपनी ज़िंदगी एक बेतकल्लुफ़ी में गुजार दी।
लेकिन गांव वाले कहते हैं कि बेटे बीमार माँ का इलाज नहीं कराते। रामभरोसे तो सबके ताने सुन लेते हैं। घर आके चादर तान कर सो जाते। रेडियो और मोबाइल पर दिन भर समाचार बजता रहता। उनके मन में क्या चलता रहता, कभी किसी को शायद ही पता चले। बातें वे देश दुनिया के बदलाव और हिंदू समाज के उद्धार की तो करते मगर अपने घर का कोई भी उद्धार उनसे हो सकने से रहा। लोग अचंभित होते उनकी स्थितप्रज्ञता पर। घर में आने वाले हर भूचाल को किसी पुराने जटिल बरगद की तरह झेलते थे। उनके चेहरे पर कभी कहीं एक शिकन नहीं दिखाई देता था। वे छोटे-से जीवन में मगन थे। उन्हें किसी चीज की कोई परवाह नहीं थे। वे सुबह उठते, गाय बछड़े को सानी पानी करते, लोटा लेकर खेत जाते। घर आकर चाय पीते, भूजा खाते और तैयार होकर मोटर लेकर तहसील निकल जाते। दिन भर उनके तहसील में गुजरते। वहाँ वे किसी वकील को पकड़कर उसके कागज़ी लिखा पढ़ी में कुछ मदद करते और जो मेहनताना मिल जाता लेकर देर रात तक घर आ जाते। खाते पीते और समाचार सुनते कब नींद के आग़ोश में गिर जाते, पता नहीं चलता। उन्हें हिंदुओं के उद्धार के अलावे किसी अन्य चीज की कभी कोई चिंता नहीं हुई। चाहे जब पिताजी बीमार हुए। वे उन
गांव भर में सब कहते थे वे सिर्फ़ इंतज़ार कर रहे हैं।
हरिहर भाई का केस अलग था। लापरवाह तो वे भी थे। मगर अलग कोटि के। गांव कस्बे के हर कोने में उन्होंने लोगों से उधारी कर छोड़ी थी। बच्चों की फ़ीस से लेकर बीवी के साड़ी-लत्ते गहने गुरिया सब उधारी पर निकल रहे थे। इसलिए अम्मा तितली के बीमार पड़ने और रामभरोसे के रामभरोसे होने के बाद उन्होंने जब इधर उधर लोगों से मदद के लिए फ़ोन मिलाना शुरू किया तो कहीं से एक चवन्नी नसीब नहीं हुई। हर संभव जगह उन्होंने सिर फोड़ लिया।
अम्मा तितली की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। खाना पीना तो पहले से उन्होंने छोड़ रखा था, फिर चलना फिरना बंद हुआ, फिर आवाज़ बंद हुई और फिर एक समय बाद वे सिर्फ़ दिन रात सोती रहती। और जब तक नींद से उठकर दहाड़े मारकर रोतीं। अब नहीं जियूँगी! उनकी भयावह चीख से घर वाले ही नहीं पड़ोस तक में अपशगुन का आतंक फैला हुआ था। पहली बार रामभरोसे को चिंता हुई थी और वे एक दिन तहसील नहीं गए। लेकिन फिर जब अम्मा की दहाड़ों की पुनरावृत्ति होने लगी और पूरा परिवार धीरे-धीरे करके इस नए यथार्थ का आदी हो चला। मगर गाँव में अब और जोर-शोर से बातें चलने लगीं। कट पिटकर, बढ़ चढ़कर ये बातें हरिहर, रामभरोसे से लेकर नीलेश तक भी पहुँचती थीं।
और थक हार कर हरिहर भाई ने अपनी बड़ी बहन से फ़ोन पर अपना दुखड़ा रोया और उसने अपने बेटे रजनीश को छियालीस हज़ार तीन सौ रुपयों के साथ गांव भेजा था।
पाँच हज़ार तो एम्बुलेंस का किराया था। फिर ये अस्पताल वो अस्पताल ये टेस्ट वो टेस्ट। अस्पताल में भर्ती। सामने छियालीस हज़ार रुपये रखे होने पर भी दोनों भाइयों के अंदर थोड़ी भी हिम्मत नहीं आई कि अब उठकर एम्बुलेंस को फ़ोन मिलाते।
नीलेश ने कहा, ‘कहीं से शुरू तो करो!’ रजनीश ने एम्बुलेंस को फ़ोन मिला दिया।
हरिहर भाई की कल्पनाओं में एम्बुलेंस की भयावह आवाज़ गूँजने लगी थी। जिला मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी प्रांगण से निकल कर एक एम्बुलेंस राजीव नगर की ओर चल पड़ी। देवरिया बाईपास से निकलते-निकलते घंटा भर लगना तय था। विधायक सूर्य नारायण के गोदाम के पास एक भयानक जाम रोज़ हर समय लगा रहता था। हरिहर भाई को एम्बुलेंस आते दिख रही थी, दिख रही थीं वे सड़कें, जाम, बेबस आदमी औरतों से लदे-फदे विक्रम टेम्पू, खटारे बस, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटी, गाय-बैल-बकरी, कुत्ते.. जान पड़ता मानो सब एक-दूसरे के ऊपर चढ़कर बाहर निकलने को आतुर हैं। इन सबके बीच एक एम्बुलेंस भयानक विलाप करते हुए आगे बढ़ने की चेष्टा कर रही थी। कहीं ना कहीं किसी ना किसी जाम में कोई ना कोई एम्बुलेंस फँसी हुई थी।
हरिहर भाई ने देखा कि नॉयलॉन बैग में रखें नोटों से बना हुआ एक छोटा सा दैत्य धीरे-धीरे बैग से बाहर निकल रहा है। उसके बाहर आते ही चारों ओर अँधेरा छा गया। बर्फ जैसी ठंडी जनवरी के ऊपर बारिश के काले बादल छाने लगे थे। कुछ देर में ऐसा लगने लगा जैसे वो कोई घर नहीं एक काली कोठरी हो जिसमें हरिहर भाई अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। नोटों से बने हुए दैत्य का आकार बढ़ने लगा। उसके आकर में बढ़ने से आस-पास की वस्तुएँ विकृत होने लगीं। सबसे पहले पलंग के पुर्जे चरचराने लगे। फिर दरवाजा जिसके कोरों को पहले ही कीड़ों ने खा रखा था। छत पर झूलता हुआ पंखा टेढ़ा-मेढ़ा होने लगा। अब उसका सिर छत से टकराया। छत इतनी कमजोर ना थी। लेकिन उसने अपना सिर नीचे झुकाया और हरिहर भाई की नाक पर अपनी एक उंगली रख दी। हरिहर भाई उसे एकटक देखे जा रहे थे। नोट से बने दैत्य ने कराहा और पास रखे जग से पानी पीने लगा। पानी पीकर वो कमरे से बाहर निकल आया। छज्जे से सिर बचाते हुए। आँगन में कोई छत नहीं थी। यहाँ अब वो बेहिसाब बढ़ सकता था। उसने अपना सिर झटका और छत पर रखे बोरों को उठाकर फेंकने लगा। नोटों का इतना बड़ा दैत्य अगर टूटकर बिखर जाता तो घर में पैसे ही पैसे होते,
विलाप करता हुआ एक एम्बुलेंस दरवाज़े पर आ खड़ा हुआ।
दो नर्सों ने गाड़ी से उतरकर स्ट्रेचर तैयार कर दिया। स्ट्रेचर लेकर घर में गए और तितली अम्मा को उठाकर स्ट्रेचर पर रखने लगे। और तितली अम्मा के नखरे शुरू। छूते ही हाथ पैर पटकने लगीं। चिल्ला चिल्लाकर गले फाड़ना शुरू। ‘अरे दादा रे दादा, ई सब मिलके हमके मुआ देहल चाहत बान सन रे! अब ना जियब दादा रे दादा, माई रे माई!’ पैर पटकने से एक तलवे पर उन्हें थोड़ी चोट भी आई। अब उन्हें रोने का एक और बहाना मिल गया था। वे और बुक्का फाड़ कर रोने लगीं। किसी ने उनके हाथ पकड़े, किसी ने पैर तो किसी ने पीठ से सहारा देकर उठाया और स्ट्रेचर पर लिटाया। उनकी दहाड़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी।
काला कुत्ता भी स्ट्रेचर तक आ गया था। उसकी भी भूँक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उछल उछल कर भौंक रहा था। नर्स स्ट्रेचर को धक्का देकर बाहर ले चले और उनके साथ साथ दौड़ा काला कुत्ता, जिसकी जिम्मेदारी थी आसमान को अपने चार टाँगों पर थाम कर रखने की। अब वह आसमान पर दौड़ रहा था। उसकी मालकिन को कोई कहाँ ले जा रहा है! वह उसके साथ तक हर जगह जाएगा। जैसे उनके सोकर उठने से लेकर उनके बिस्तर पर जाने के समय तक वह उनके साथ रहता है। उनकी खाट के नीचे सोता। उनके उठकर टॉयलेट जाने पर उनके बाहर आने तक बाहर दरवाजे पर बैठा रहता। फिर पूंछ हिलाते उनके साथ हो लिया। वे सोतीं तो वह भी खाट के नीचे फैलकर सो जाता। ओ काले कुत्ते, तेरे हिस्से का आसमान रात में कौन उठाता था? या रात में तेरे साथ साथ आसमान सो जाता था। तितली अम्मा सोती थी एक बेतकल्लुफ़ नींद और काला कुत्ता सोता था श्वान की नींद और आसमान रात में काला हो जाता था। कुत्ते के रंग का काला जिसमें टिमटिमाते थे तारे। जिन तारों में बसते थे तितली अम्मा के पूर्वज। इस काले आसमान में थी कितनी ही सभ्यताओं की कॉलोनी। जब तितली अम्मा अस्पताल में होगी तब काला कुत्ता कहाँ सोएगा? अस्पताल जाने पर लोग उसपर चप्पल जूते मारेंगे।
तितली अम्मा को एम्बुलेंस में चढ़ाकर दरवाजा बंद कर दिया गया। साथ में नीलेश, रजनीश, छुटकी, हरिहर भाई और उनकी पत्नी बैठ गए। रामभरोसे लौटकर अपनी चौकी पर बैठ गए। उन्होंने बरामदे की दीवार पर टँगी घड़ी और कैलेण्डर पर नज़र डाली।
उनके लिए एक अजीब हफ़्ता था वह। वे भूलते जा रहे थे कि उस हफ़्ते में कितने दिन थे और कौन कौन सी तारीखें थीं। तारीखें कैलेंडर से निकलकर इधर-उधर भटक गयीं थीं। संख्याओं का क्रम गड़बड़ हो गया था। किसी को नहीं याद कौन-सी संख्या पहली थी तो फिर आगे की कौन पूछे। इतिहास गड्डमड्ड हो गया था। हो चुके युद्ध भविष्य की ओर खिसक गए थे। भविष्य की घटनाएँ अतीत में घटित हो गयीं थीं। घड़ी 23.59 पर रुकी थी। लगता था अब एक मिनट बीता कि तब। जैसे ही एक मिनट बीतता 23.59 से 00.00 हो जाता। नया दिन शुरू हो जाता। घर के बाहर पेड़ पर पक्षी चहचहाने लगते। पर यह मुआ एक मिनट नहीं बीतता। घड़ी के सभी अंक कैलेंडर के अंकों की तरह घड़ी के गोल में इधर उधर गिरे पड़े हैं।